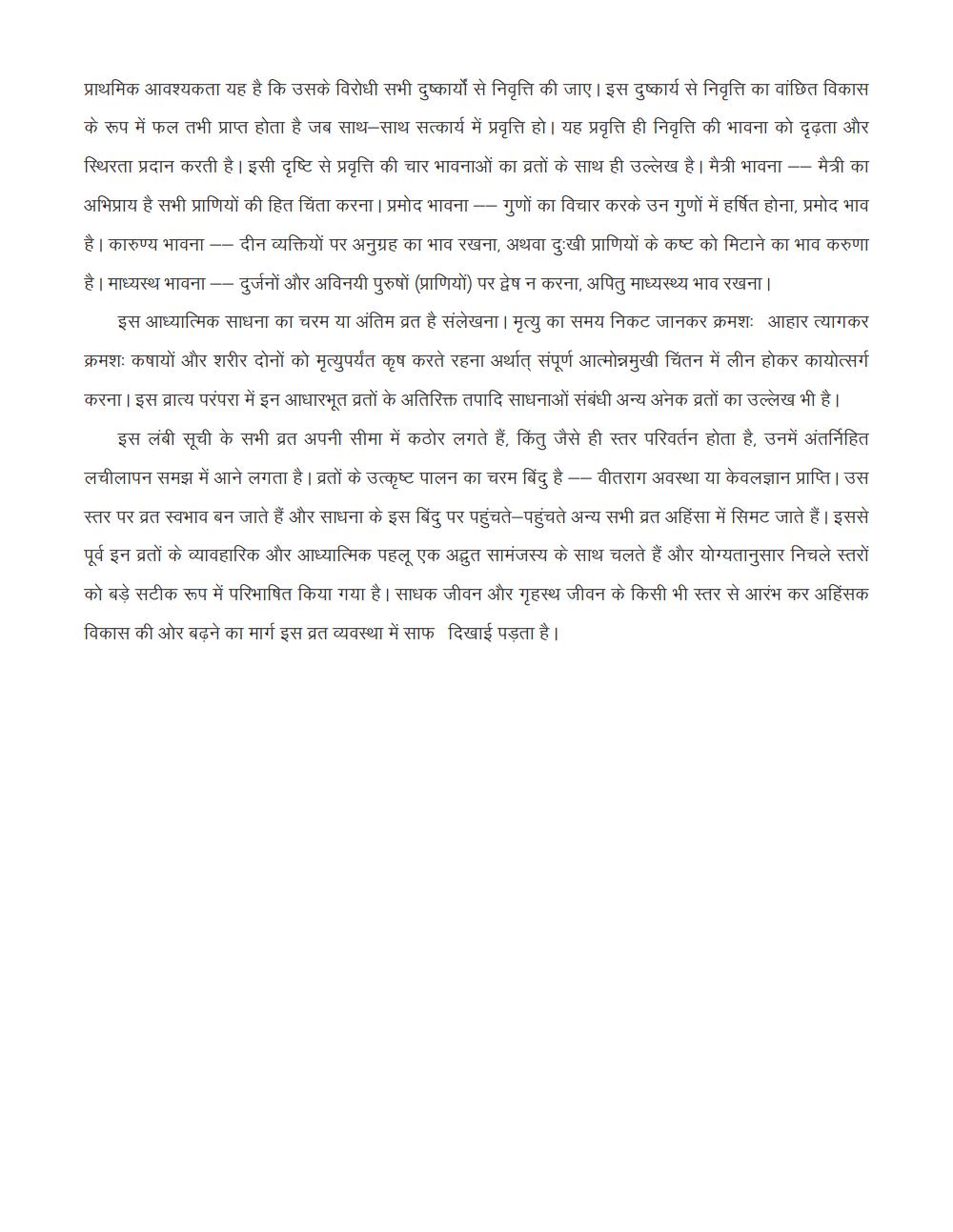Book Title: Jain Vrat Author(s): Surendra Bothra Publisher: Surendra Bothra View full book textPage 4
________________ प्राथमिक आवश्यकता यह है कि उसके विरोधी सभी दुष्कार्यों से निवृत्ति की जाए। इस दुष्कार्य से निवृत्ति का वांछित विकास के रूप में फल तभी प्राप्त होता है जब साथ-साथ सत्कार्य में प्रवृत्ति हो। यह प्रवृत्ति ही निवृत्ति की भावना को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करती है। इसी दृष्टि से प्रवृत्ति की चार भावनाओं का व्रतों के साथ ही उल्लेख है। मैत्री भावना -- मैत्री का अभिप्राय है सभी प्राणियों की हित चिंता करना। प्रमोद भावना -- गुणों का विचार करके उन गुणों में हर्षित होना, प्रमोद भाव है। कारुण्य भावना -- दीन व्यक्तियों पर अनुग्रह का भाव रखना, अथवा दुःखी प्राणियों के कष्ट को मिटाने का भाव करुणा है। माध्यस्थ भावना -- दुर्जनों और अविनयी पुरुषों (प्राणियों) पर द्वेष न करना, अपितु माध्यस्थ्य भाव रखना। इस आध्यात्मिक साधना का चरम या अंतिम व्रत है संलेखना। मृत्यु का समय निकट जानकर क्रमशः आहार त्यागकर क्रमशः कषायों और शरीर दोनों को मृत्युपर्यंत कृष करते रहना अर्थात् संपूर्ण आत्मोन्नमुखी चिंतन में लीन होकर कायोत्सर्ग करना। इस व्रात्य परंपरा में इन आधारभूत व्रतों के अतिरिक्त तपादि साधनाओं संबंधी अन्य अनेक व्रतों का उल्लेख भी है। इस लंबी सूची के सभी व्रत अपनी सीमा में कठोर लगते हैं, किंतु जैसे ही स्तर परिवर्तन होता है, उनमें अंतर्निहित लचीलापन समझ में आने लगता है। व्रतों के उत्कृष्ट पालन का चरम बिंदु है -- वीतराग अवस्था या केवलज्ञान प्राप्ति / उस स्तर पर व्रत स्वभाव बन जाते हैं और साधना के इस बिंदु पर पहुंचते-पहुंचते अन्य सभी व्रत अहिंसा में सिमट जाते हैं। इससे पूर्व इन व्रतों के व्यावहारिक और आध्यात्मिक पहलू एक अद्भुत सामंजस्य के साथ चलते हैं और योग्यतानुसार निचले स्तरों को बड़े सटीक रूप में परिभाषित किया गया है। साधक जीवन और गृहस्थ जीवन के किसी भी स्तर से आरंभ कर अहिंसक विकास की ओर बढ़ने का मार्ग इस व्रत व्यवस्था में साफ दिखाई पड़ता है।Page Navigation
1 2 3 4