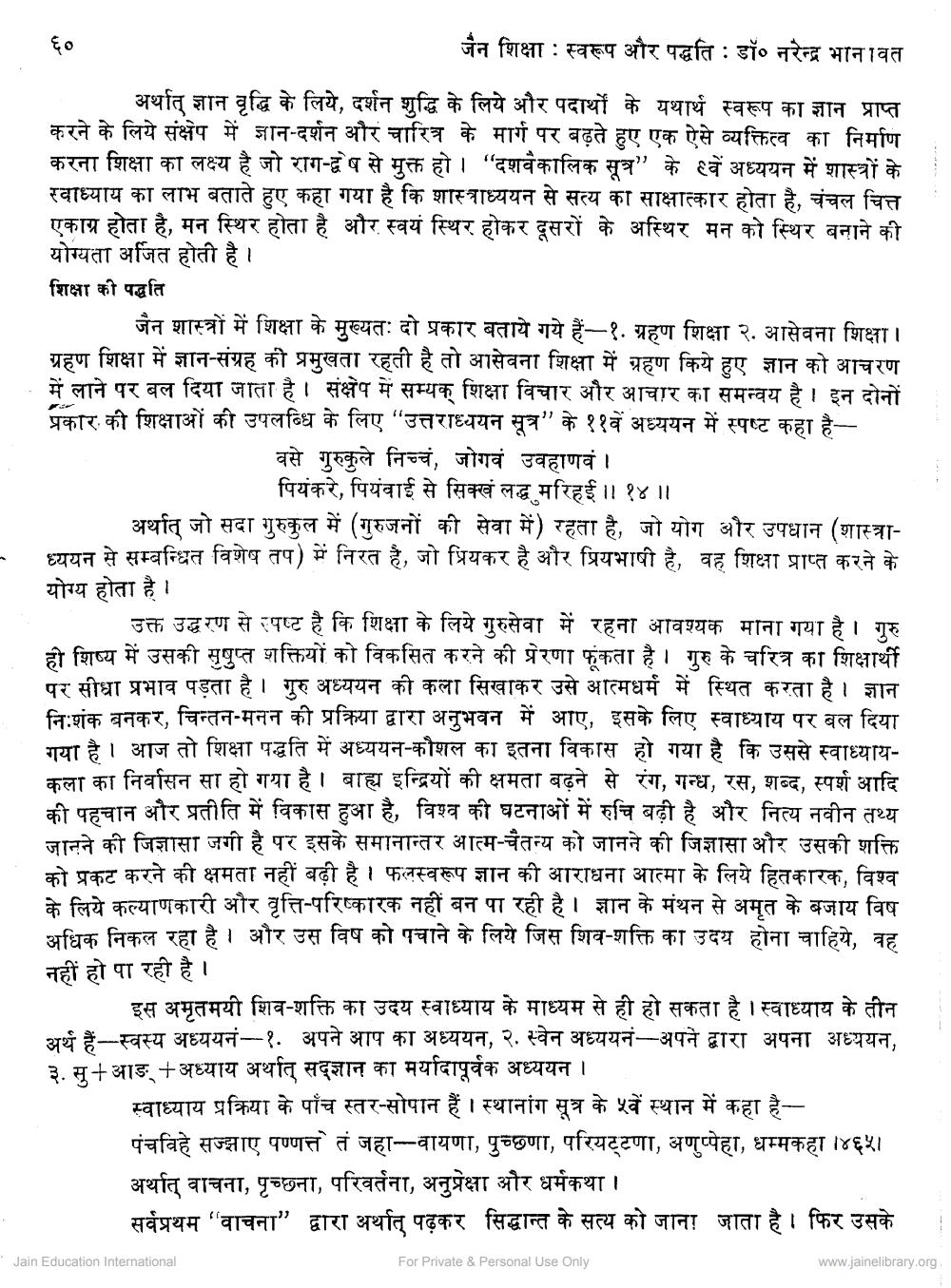Book Title: Jain Shiksha swarup aur Paddhati Author(s): Narendra Bhanavat Publisher: Z_Sajjanshreeji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012028.pdf View full book textPage 3
________________ जैन शिक्षा : स्वरूप और पद्धति : डॉ० नरेन्द्र भानावत अर्थात् ज्ञान वृद्धि के लिये, दर्शन शुद्धि के लिये और पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये संक्षेप में ज्ञान दर्शन और चारित्र के मार्ग पर बढ़ते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना शिक्षा का लक्ष्य है जो राग-द्व ेष से मुक्त हो । "दशवैकालिक सूत्र" के हवें अध्ययन में शास्त्रों के स्वाध्याय का लाभ बताते हुए कहा गया है कि शास्त्राध्ययन से सत्य का साक्षात्कार होता है, चंचल चित्त एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है और स्वयं स्थिर होकर दूसरों के अस्थिर मन को स्थिर बनाने की योग्यता अर्जित होती है । शिक्षा की पद्धति जैन शास्त्रों में शिक्षा के मुख्यतः दो प्रकार बताये गये हैं - १. ग्रहण शिक्षा २. आसेवना शिक्षा | ग्रहण शिक्षा में ज्ञान -संग्रह की प्रमुखता रहती है तो आसेवना शिक्षा में ग्रहण किये हुए ज्ञान को आचरण में लाने पर बल दिया जाता है । संक्षेप में सम्यक् शिक्षा विचार और आचार का समन्वय है । इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं की उपलब्धि के लिए "उत्तराध्ययन सूत्र" के ११ वें अध्ययन में स्पष्ट कहा हैवसे गुरुकुले निच्चं, जोगवं उवहाणवं । पियंकरे, पियंवाई से सिक्ख लद्ध मरिहई ॥ १४ ॥ ६० अर्थात् जो सदा गुरुकुल में (गुरुजनों की सेवा में ) रहता है, जो योग और उपधान (शास्त्राध्ययन से सम्बन्धित विशेष तप ) में निरत है, जो प्रियकर है और प्रियभाषी है, वह शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता है । उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि शिक्षा के लिये गुरुसेवा में रहना आवश्यक माना गया है। गुरु ही शिष्य में उसकी सुषुप्त शक्तियों को विकसित करने की प्रेरणा फूंकता है। गुरु के चरित्र का शिक्षार्थी पर सीधा प्रभाव पड़ता है । गुरु अध्ययन की कला सिखाकर उसे आत्मधर्म में स्थित करता है । ज्ञ निःशंक बनकर, चिन्तन-मनन की प्रक्रिया द्वारा अनुभवन में आए, इसके लिए स्वाध्याय पर बल दिया गया है । आज तो शिक्षा पद्धति में अध्ययन - कौशल का इतना विकास हो गया है कि उससे स्वाध्यायकला का निर्वासन सा हो गया है । बाह्य इन्द्रियों की क्षमता बढ़ने से रंग, गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श आदि की पहचान और प्रतीति में विकास हुआ है, विश्व की घटनाओं में रुचि बढ़ी है और नित्य नवीन तथ्य जानने की जिज्ञासा जगी है पर इसके समानान्तर आत्म- चैतन्य को जानने की जिज्ञासा और उसकी शक्ति को प्रकट करने की क्षमता नहीं बढ़ी है । फलस्वरूप ज्ञान की आराधना आत्मा के लिये हितकारक, विश्व के लिये कल्याणकारी और वृत्ति - परिष्कारक नहीं बन पा रही है। ज्ञान के मंथन से अमृत के बजाय विष अधिक निकल रहा है । और उस विष को पचाने के लिये जिस शिव-शक्ति का उदय होना चाहिये, वह नहीं हो पा रही है । इस अमृतमयी शिव-शक्ति का उदय स्वाध्याय 'माध्यम से ही हो सकता है । स्वाध्याय के तीन अर्थ हैं—स्वस्य अध्ययनं - १. अपने आप का अध्ययन, २. स्वेन अध्ययनं - अपने द्वारा अपना अध्ययन, ३. सु + आ + अध्याय अर्थात् सद्ज्ञान का मर्यादापूर्वक अध्ययन | स्वाध्याय प्रक्रिया के पाँच स्तर-सोपान हैं । स्थानांग सूत्र के ५वें स्थान में कहा है पंचविहे सज्झाए पण्णत्त े तं जहा - वायणा, पुच्छणा, परियट्टणा, अणुप्पेहा, धम्मका । ४६५ । अर्थात् वाचना, पृच्छ्ना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा । सर्वप्रथम “वाचना” द्वारा अर्थात् पढ़कर सिद्धान्त के सत्य को जाना जाता है । फिर उसके For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org. Jain Education InternationalPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7