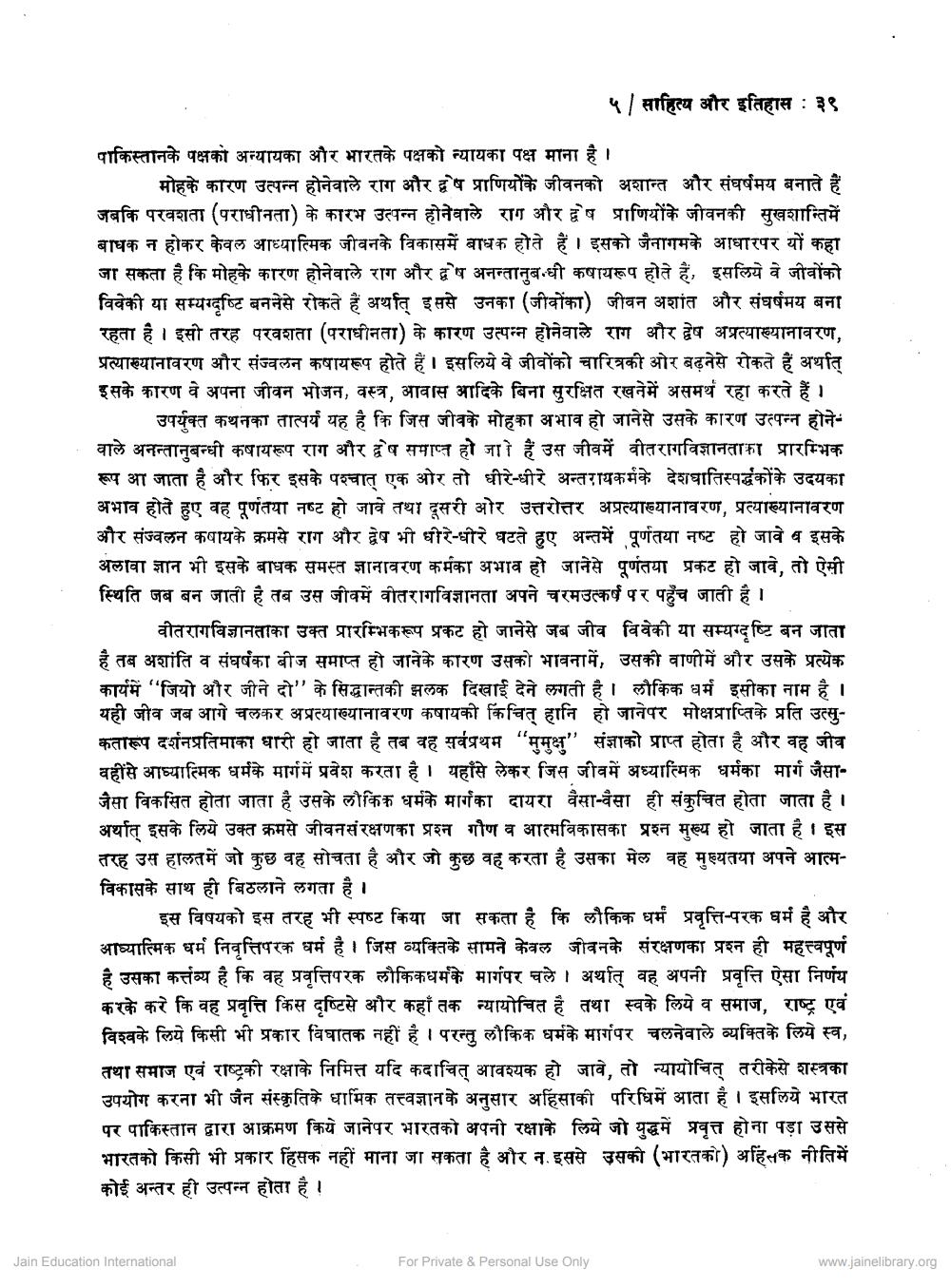Book Title: Jain Sanskruti aur Tattvagyan Author(s): Bansidhar Pandit Publisher: Z_Bansidhar_Pandit_Abhinandan_Granth_012047.pdf View full book textPage 6
________________ ५/साहित्य और इतिहास : ३९ पाकिस्तानके पक्षको अन्यायका और भारतके पक्षको न्यायका पक्ष माना है। मोहके कारण उत्पन्न होनेवाले राग और द्वष प्राणियोंके जीवनको अशान्त और संघर्षमय बनाते हैं जबकि परवशता (पराधीनता) के कारभ उत्पन्न होनेवाले राग और द्वेष प्राणियोंके जीवनकी सुखशान्तिमें बाधक न होकर केवल आध्यात्मिक जीवनके विकासमें बाधक होते हैं। इसको जैनागमके आधारपर यों कहा जा सकता है कि मोहके कारण होनेवाले राग और द्वष अनन्तानुबन्धी कषायरूप होते हैं, इसलिये वे जीवोंको विवेकी या सम्यग्दृष्टि बननेसे रोकते हैं अर्थात् इससे उनका (जीवोंका) जीवन अशांत और संघर्षमय बना रहता है । इसी तरह परवशता (पराधीनता) के कारण उत्पन्न होनेवाले राग और द्वेष अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायरूप होते हैं। इसलिये वे जीवोंको चारित्रकी ओर बढ़नेसे रोकते हैं अर्थात् इसके कारण वे अपना जीवन भोजन, वस्त्र, आवास आदिके बिना सुरक्षित रखने में असमर्थ रहा करते हैं। उपर्युक्त कथनका तात्पर्य यह है कि जिस जीवके मोहका अभाव हो जानेसे उसके कारण उत्पन्न होनेवाले अनन्तानुबन्धी कषायरूप राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं उस जीवमें वीतरागविज्ञानताका प्रारम्भिक रूप आ जाता है और फिर इसके पश्चात् एक ओर तो धीरे-धीरे अन्तरायकर्मके देशघातिस्पर्द्धकोंके उदयका अभाव होते हुए वह पूर्णतया नष्ट हो जावे तथा दूसरी ओर उत्तरोत्तर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायके क्रमसे राग और द्वेष भी धीरे-धीरे घटते हए अन्तमें पूर्णतया नष्ट हो जावे व इसके अलावा ज्ञान भी इसके बाधक समस्त ज्ञानावरण कर्मका अभाव हो जानेसे पूर्णतया प्रकट हो जावे, तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तब उस जीवमें वीतरागविज्ञानता अपने चरमउत्कर्ष पर पहुँच जाती है। वीतरागविज्ञानताका उक्त प्रारम्भिकरूप प्रकट हो जानेसे जब जीव विवेकी या सम्यग्दष्टि बन जाता है तब अशांति व संघर्षका बीज समाप्त हो जानेके कारण उसको भावनामें, उसकी वाणीमें और उसके प्रत्येक कार्यमें "जियो और जीने दो" के सिद्धान्तकी झलक दिखाई देने लगती है। लौकिक धर्म इसीका नाम है । यही जीव जब आगे चलकर अप्रत्याख्यानावरण कषायको किंचित् हानि हो जानेपर मोक्षप्राप्तिके प्रति उत्सुकतारूप दर्शनप्रतिमाका धारी हो जाता है तब वह सर्वप्रथम “मुमुक्षु" संज्ञाको प्राप्त होता है और वह जीव वहींसे आध्यात्मिक धर्मके मार्ग में प्रवेश करता है। यहाँसे लेकर जिस जीवमें अध्यात्मिक धर्मका मार्ग जैसाजैसा विकसित होता जाता है उसके लौकिक धर्मके मार्गका दायरा वैसा-वैसा ही संकुचित होता जाता है। अर्थात् इसके लिये उक्त क्रमसे जीवनसंरक्षणका प्रश्न गौण व आत्मविकासका प्रश्न मुख्य हो जाता है । इस तरह उस हालतमें जो कुछ वह सोचता है और जो कुछ वह करता है उसका मेल वह मुख्यतया अपने आत्मविकासके साथ ही बिठलाने लगता है। इस विषयको इस तरह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि लौकिक धर्म प्रवृत्ति-परक धर्म है और आध्यात्मिक धर्म निवृत्तिपरक धर्म है। जिस व्यक्तिके सामने केवल जीवनके संरक्षणका प्रश्न ही महत्त्वपूर्ण है उसका कर्तव्य है कि वह प्रवृत्तिपरक लौकिकधर्मके मार्गपर चले । अर्थात् वह अपनी प्रवृत्ति ऐसा निर्णय करके करे कि वह प्रवृत्ति किस दृष्टिसे और कहाँ तक न्यायोचित है तथा स्वके लिये व समाज, राष्ट्र एवं विश्वके लिये किसी भी प्रकार विघातक नहीं है । परन्तु लौकिक धर्मके मार्गपर चलनेवाले व्यक्तिके लिये स्व, तथा समाज एवं राष्ट्रको रक्षाके निमित्त यदि कदाचित आवश्यक हो जावे, तो न्यायोचित तरीकेसे शस्त्रका उपयोग करना भी जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्त्वज्ञान के अनुसार अहिंसाकी परिधिमें आता है । इसलिये भारत पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किये जानेपर भारतको अपनी रक्षाके लिये जो युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा उससे भारतको किसी भी प्रकार हिंसक नहीं माना जा सकता है और न. इससे उसको (भारतको) अहिंसक नीतिमें कोई अन्तर ही उत्पन्न होता है । Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10