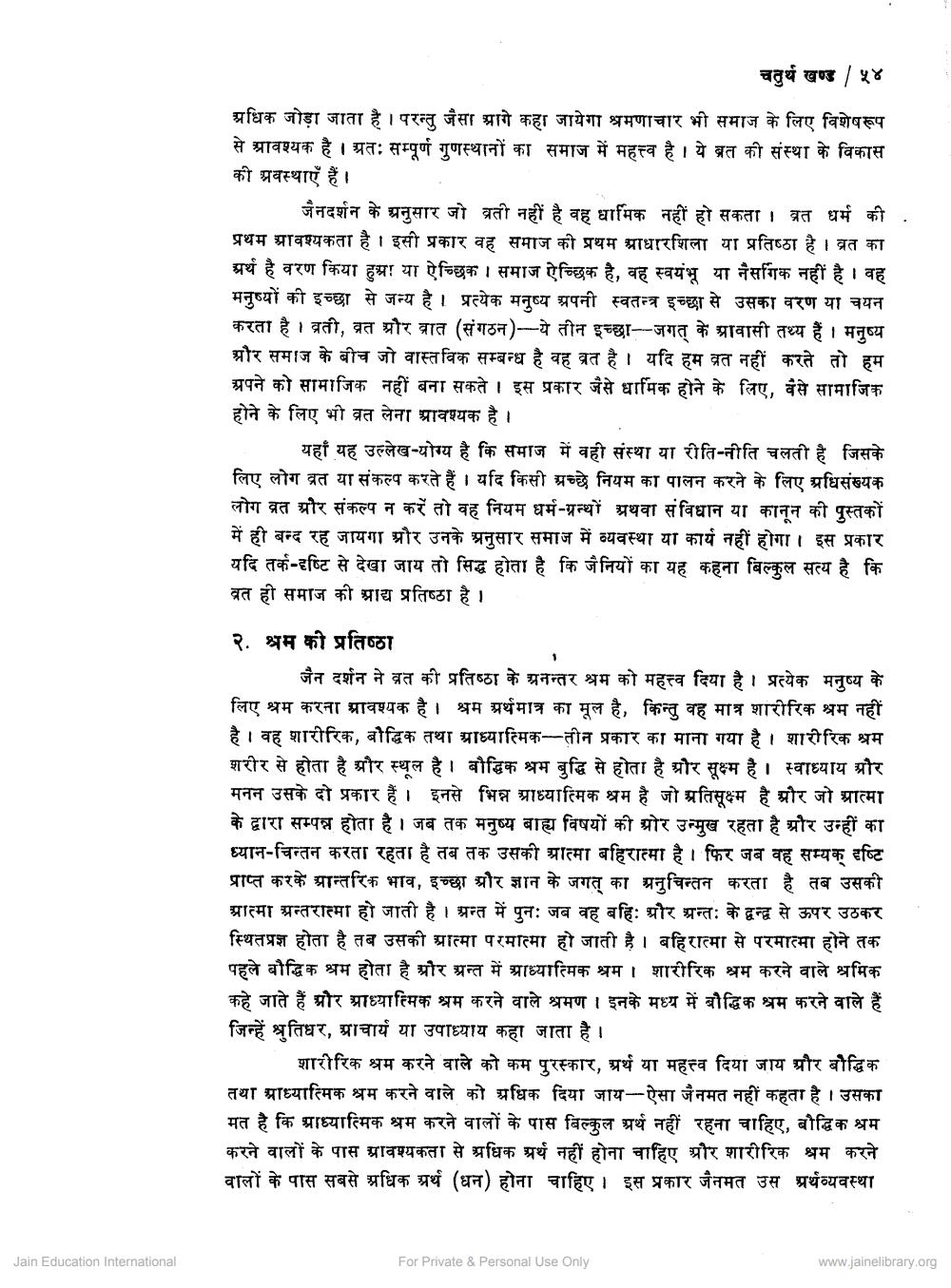Book Title: Jain Samaj Darshan Author(s): Sangamlal Pandey Publisher: Z_Umravkunvarji_Diksha_Swarna_Jayanti_Smruti_Granth_012035.pdf View full book textPage 2
________________ चतुर्थ खण्ड/५४ अधिक जोड़ा जाता है । परन्तु जैसा आगे कहा जायेगा श्रमणाचार भी समाज के लिए विशेषरूप से आवश्यक है । अतः सम्पूर्ण गुणस्थानों का समाज में महत्त्व है। ये ब्रत की संस्था के विकास की अवस्थाएँ हैं। जैनदर्शन के अनुसार जो व्रती नहीं है वह धार्मिक नहीं हो सकता। व्रत धर्म की . प्रथम आवश्यकता है। इसी प्रकार वह समाज की प्रथम प्राधारशिला या प्रतिष्ठा है । व्रत का अर्थ है वरण किया हुआ या ऐच्छिक । समाज ऐच्छिक है, वह स्वयंभू या नैसर्गिक नहीं है । वह मनुष्यों की इच्छा से जन्य है। प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा से उसका वरण या चयन करता है। व्रती, व्रत और वात (संगठन)-ये तीन इच्छा-जगत् के आवासी तथ्य हैं । मनुष्य और समाज के बीच जो वास्तविक सम्बन्ध है वह व्रत है। यदि हम व्रत नहीं करते तो हम अपने को सामाजिक नहीं बना सकते । इस प्रकार जैसे धार्मिक होने के लिए, वैसे सामाजिक होने के लिए भी व्रत लेना आवश्यक है। यहाँ यह उल्लेख-योग्य है कि समाज में वही संस्था या रीति-नीति चलती है जिसके लिए लोग व्रत या संकल्प करते हैं। यदि किसी अच्छे नियम का पालन करने के लिए अधिसंख्यक लोग व्रत और संकल्प न करें तो वह नियम धर्म-ग्रन्थों अथवा संविधान या कानून की पुस्तकों में ही बन्द रह जायगा और उनके अनुसार समाज में व्यवस्था या कार्य नहीं होगा। इस प्रकार यदि तर्क-दृष्टि से देखा जाय तो सिद्ध होता है कि जैनियों का यह कहना बिल्कुल सत्य है कि व्रत ही समाज की प्राद्य प्रतिष्ठा है। २. श्रम की प्रतिष्ठा जैन दर्शन ने व्रत की प्रतिष्ठा के अनन्तर श्रम को महत्त्व दिया है। प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रम करना आवश्यक है। श्रम अर्थमात्र का मूल है, किन्तु वह मात्र शारीरिक श्रम नहीं है। वह शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक-तीन प्रकार का माना गया है। शारीरिक श्रम शरीर से होता है और स्थल है। बौद्धिक श्रम बुद्धि से होता है और सूक्ष्म है। स्वाध्याय और मनन उसके दो प्रकार हैं। इनसे भिन्न प्राध्यात्मिक श्रम है जो प्रतिसूक्ष्म है और जो आत्मा के द्वारा सम्पन्न होता है। जब तक मनुष्य बाह्य विषयों की ओर उन्मुख रहता है और उन्हीं का ध्यान-चिन्तन करता रहता है तब तक उसकी आत्मा बहिरात्मा है। फिर जब वह सम्यक् दृष्टि प्राप्त करके आन्तरिक भाव, इच्छा और ज्ञान के जगत् का अनुचिन्तन करता है तब उसकी आत्मा अन्तरात्मा हो जाती है । अन्त में पुनः जब वह बहिः और अन्तः के द्वन्द्व से ऊपर उठकर स्थितप्रज्ञ होता है तब उसकी आत्मा परमात्मा हो जाती है। बहिरात्मा से परमात्मा होने तक पहले बौद्धिक श्रम होता है और अन्त में आध्यात्मिक श्रम । शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक कहे जाते हैं और आध्यात्मिक श्रम करने वाले श्रमण । इनके मध्य में बौद्धिक श्रम करने वाले हैं जिन्हें श्रुतिधर, प्राचार्य या उपाध्याय कहा जाता है । शारीरिक श्रम करने वाले को कम पुरस्कार, अर्थ या महत्त्व दिया जाय और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक श्रम करने वाले को अधिक दिया जाय-ऐसा जैनमत नहीं कहता है । उसका मत है कि प्राध्यात्मिक श्रम करने वालों के पास बिल्कुल अर्थ नहीं रहना चाहिए, बौद्धिक श्रम करने वालों के पास आवश्यकता से अधिक अर्थ नहीं होना चाहिए और शारीरिक श्रम करने वालों के पास सबसे अधिक अर्थ (धन) होना चाहिए। इस प्रकार जैनमत उस अर्थव्यवस्था Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6