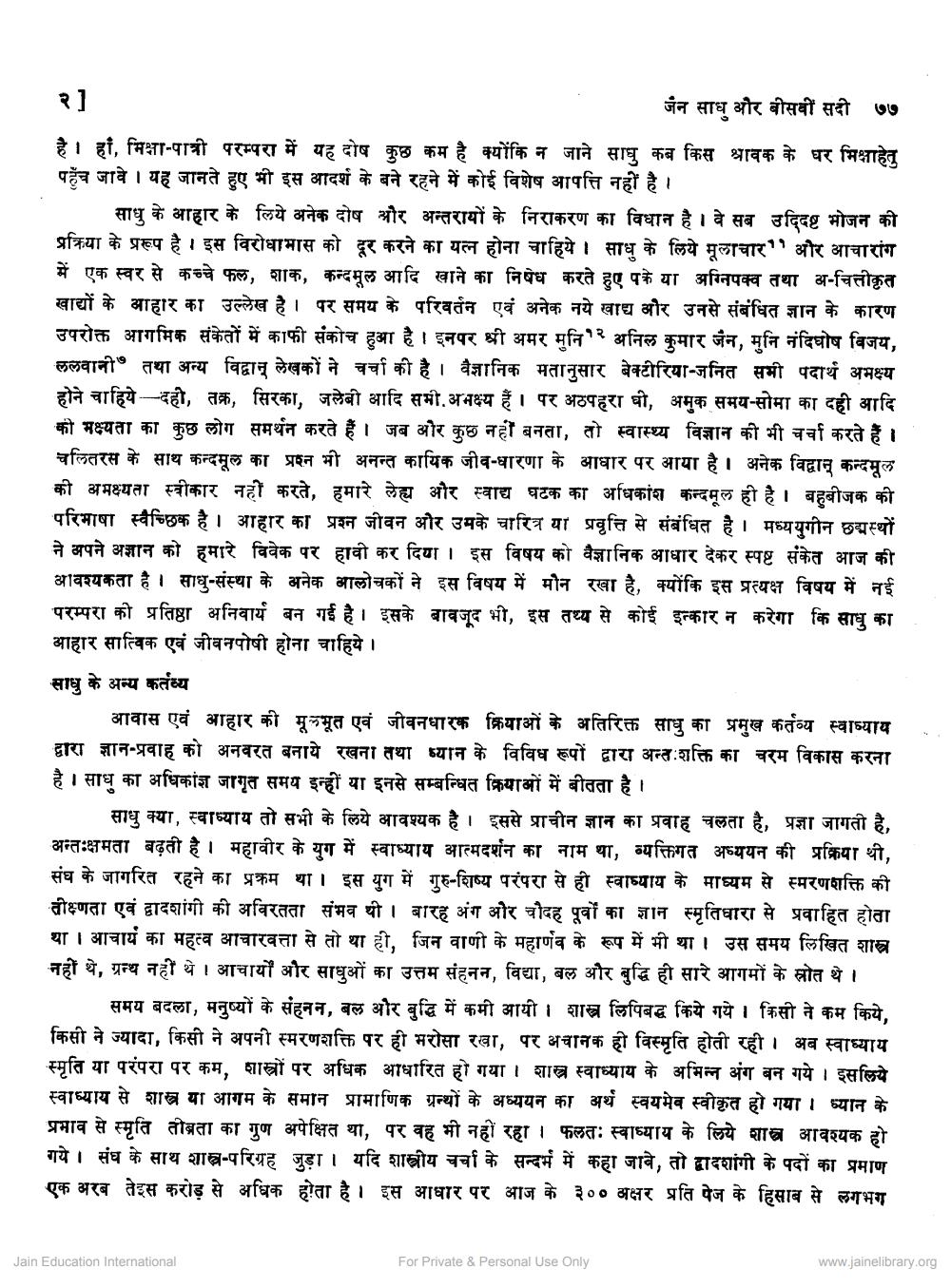Book Title: Jain Sadhu aur Biswi Sadi Author(s): Nirmal Azad Publisher: Z_Jaganmohanlal_Pandit_Sadhuwad_Granth_012026.pdf View full book textPage 7
________________ २] जैन साधु और बीसवीं सदी ७७ है। हां, मिक्षा-पात्री परम्परा में यह दोष कुछ कम है क्योंकि न जाने साधु कब किस श्रावक के घर भिक्षाहेतु पहुँच जावे । यह जानते हुए भी इस आदर्श के बने रहने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है। साधु के आहार के लिये अनेक दोष और अन्तरायों के निराकरण का विधान है। वे सब उद्दिष्ट भोजन की प्रक्रिया के प्ररूप है। इस विरोधाभास को दूर करने का यत्न होना चाहिये। साध के लिये मूलाचार" और आचारांग में एक स्वर से कच्चे फल, शाक, कन्दमूल आदि खाने का निषेध करते हुए पके या अग्निपक्व तथा अ-चित्तीकृत खाद्यों के आहार का उल्लेख है । पर समय के परिवर्तन एवं अनेक नये खाद्य और उनसे संबंधित ज्ञान के कारण उपरोक्त आगमिक संकेतों में काफी संकोच हुआ है। इनपर श्री अमर मुनि'२ अनिल कुमार जैन, मुनि नंदिघोष विजय, ललवानी तथा अन्य विद्वान् लेखकों ने चर्चा की है। वैज्ञानिक मतानुसार बेक्टीरिया-जनित सभी पदार्थ अभक्ष्य होने चाहिये-दही, तक, सिरका, जलेबी आदि सभी.अमक्ष्य हैं । पर अठपहरा घी, अमुक समय-सोमा का दही आदि की भक्ष्यता का कुछ लोग समर्थन करते हैं। जब और कुछ नहीं बनता, तो स्वास्थ्य विज्ञान की भी चर्चा करते हैं । चलितरस के साथ कन्दमूल का प्रश्न भी अनन्त कायिक जीव-धारणा के आधार पर आया है। अनेक विद्वान् कन्दमूल की अमक्ष्यता स्वीकार नहीं करते, हमारे लेह्य और स्वाद्य घटक का अधिकांश कन्दमूल ही है । बहुबीजक की परिभाषा स्वैच्छिक है। आहार का प्रश्न जीवन और उसके चारित्र या प्रवृत्ति से संबंधित है। मध्ययुगीन छद्मस्थों ने अपने अज्ञान को हमारे विवेक पर हावी कर दिया। इस विषय को वैज्ञानिक आधार देकर स्पष्ट संकेत आज की आवश्यकता है। साधु-संस्था के अनेक आलोचकों ने इस विषय में मौन रखा है, क्योंकि इस प्रत्यक्ष विषय में नई परम्परा को प्रतिष्ठा अनिवार्य बन गई है। इसके बावजूद भी, इस तथ्य से कोई इन्कार न करेगा कि साधु का आहार सात्विक एवं जीवनपोषी होना चाहिये । साधु के अन्य कर्तव्य आवास एवं आहार की मूलभूत एवं जीवनधारक क्रियाओं के अतिरिक्त साधु का प्रमुख कर्तव्य स्वाध्याय द्वारा ज्ञान-प्रवाह को अनवरत बनाये रखना तथा ध्यान के विविध रूपों द्वारा अन्तःशक्ति का चरम विकास करना है । साधु का अधिकांश जागृत समय इन्हीं या इनसे सम्बन्धित क्रियाओं में बीतता है। साधु क्या, स्वाध्याय तो सभी के लिये आवश्यक है। इससे प्राचीन ज्ञान का प्रवाह चलता है, प्रज्ञा जागती है, अन्तःक्षमता बढ़ती है। महावीर के युग में स्वाध्याय आत्मदर्शन का नाम था, व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया थी, संघ के जागरित रहने का प्रक्रम था। इस युग में गुरु-शिष्य परंपरा से ही स्वाध्याय के माध्यम से स्मरणशक्ति की तीक्ष्णता एवं द्वादशांगी की अविरतता संभव थी। बारह अंग और चौदह पूर्वो का ज्ञान स्मृतिधारा से प्रवाहित होता था । आचार्य का महत्व आचारवत्ता से तो था ही, जिन वाणी के महार्णव के रूप में भी था। उस समय लिखित शास्त्र नहीं थे, ग्रन्थ नहीं थे । आचार्यों और साधुओं का उत्तम संहनन, विद्या, बल और बुद्धि ही सारे आगमों के स्रोत थे । __ समय बदला, मनुष्यों के संहनन, बल और बुद्धि में कमी आयी। शास्त्र लिपिबद्ध किये गये । किसी ने कम किये, किसी ने ज्यादा, किसी ने अपनी स्मरणशक्ति पर ही भरोसा रखा, पर अचानक ही विस्मृति होती रही। अब स्वाध्याय स्मृति या परंपरा पर कम, शास्त्रों पर अधिक आधारित हो गया। शास्त्र स्वाध्याय के अभिन्न अंग बन गये । इसलिये स्वाध्याय से शास्त्र या आगम के समान प्रामाणिक ग्रन्थों के अध्ययन का अर्थ स्वयमेव स्वीकृत हो गया। ध्यान के प्रभाव से स्मृति तीब्रता का गुण अपेक्षित था, पर वह भी नहीं रहा। फलतः स्वाध्याय के लिये शास्त्र आवश्यक हो गये। संघ के साथ शास्त्र-परिग्रह जुड़ा। यदि शास्त्रीय चर्चा के सन्दर्भ में कहा जावे, तो द्वादशांगी के पदों का प्रमाण एक अरब तेइस करोड़ से अधिक होता है। इस आधार पर आज के ३०० अक्षर प्रति पेज के हिसाब से लगभग Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10