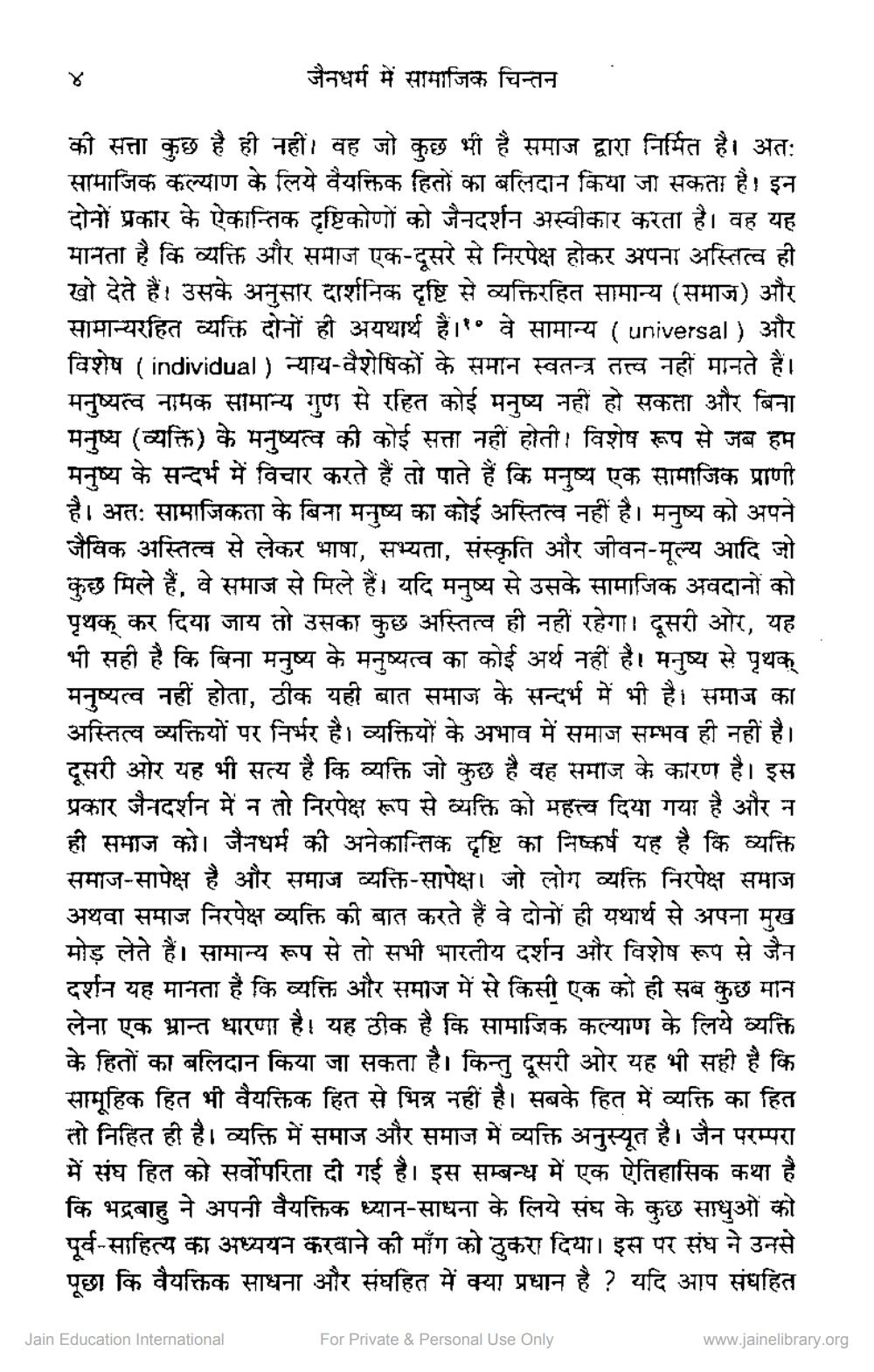Book Title: Jain Dharm me Samajik Chintan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Sagar_Jain_Vidya_Bharti_Part_3_001686.pdf View full book textPage 4
________________ जैनधर्म में सामाजिक चिन्तन की सत्ता कुछ है ही नहीं। वह जो कुछ भी है समाज द्वारा निर्मित है। अत: सामाजिक कल्याण के लिये वैयक्तिक हितों का बलिदान किया जा सकता है। इन दोनों प्रकार के ऐकान्तिक दृष्टिकोणों को जैनदर्शन अस्वीकार करता है। वह यह मानता है कि व्यक्ति और समाज एक-दूसरे से निरपेक्ष होकर अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। उसके अनुसार दार्शनिक दृष्टि से व्यक्तिरहित सामान्य (समाज) और सामान्यरहित व्यक्ति दोनों ही अयथार्थ हैं। वे सामान्य ( universal) और विशेष ( individual ) न्याय-वैशेषिकों के समान स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानते हैं। मनुष्यत्व नामक सामान्य गुण से रहित कोई मनुष्य नहीं हो सकता और बिना मनुष्य (व्यक्ति) के मनुष्यत्व की कोई सत्ता नहीं होती। विशेष रूप से जब हम मनुष्य के सन्दर्भ में विचार करते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अत: सामाजिकता के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य को अपने जैविक अस्तित्व से लेकर भाषा, सभ्यता, संस्कृति और जीवन-मूल्य आदि जो कुछ मिले हैं, वे समाज से मिले हैं। यदि मनुष्य से उसके सामाजिक अवदानों को पृथक कर दिया जाय तो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दूसरी ओर, यह भी सही है कि बिना मनुष्य के मनुष्यत्व का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य से पृथक मनुष्यत्व नहीं होता, ठीक यही बात समाज के सन्दर्भ में भी है। समाज का अस्तित्व व्यक्तियों पर निर्भर है। व्यक्तियों के अभाव में समाज सम्भव ही नहीं है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि व्यक्ति जो कुछ है वह समाज के कारण है। इस प्रकार जैनदर्शन में न तो निरपेक्ष रूप से व्यक्ति को महत्त्व दिया गया है और न ही समाज को। जैनधर्म की अनेकान्तिक दृष्टि का निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति समाज-सापेक्ष है और समाज व्यक्ति-सापेक्ष। जो लोग व्यक्ति निरपेक्ष समाज अथवा समाज निरपेक्ष व्यक्ति की बात करते हैं वे दोनों ही यथार्थ से अपना मुख मोड़ लेते हैं। सामान्य रूप से तो सभी भारतीय दर्शन और विशेष रूप से जैन दर्शन यह मानता है कि व्यक्ति और समाज में से किसी एक को ही सब कुछ मान लेना एक भ्रान्त धारणा है। यह ठीक है कि सामाजिक कल्याण के लिये व्यक्ति के हितों का बलिदान किया जा सकता है। किन्तु दूसरी ओर यह भी सही है कि सामूहिक हित भी वैयक्तिक हित से भिन्न नहीं है। सबके हित में व्यक्ति का हित तो निहित ही है। व्यक्ति में समाज और समाज में व्यक्ति अनुस्यूत है। जैन परम्परा में संघ हित को सर्वोपरिता दी गई है। इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक कथा है कि भद्रबाहु ने अपनी वैयक्तिक ध्यान-साधना के लिये संघ के कुछ साधुओं को पूर्व-साहित्य का अध्ययन करवाने की माँग को ठुकरा दिया। इस पर संघ ने उनसे पूछा कि वैयक्तिक साधना और संघहित में क्या प्रधान है ? यदि आप संघहित Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19