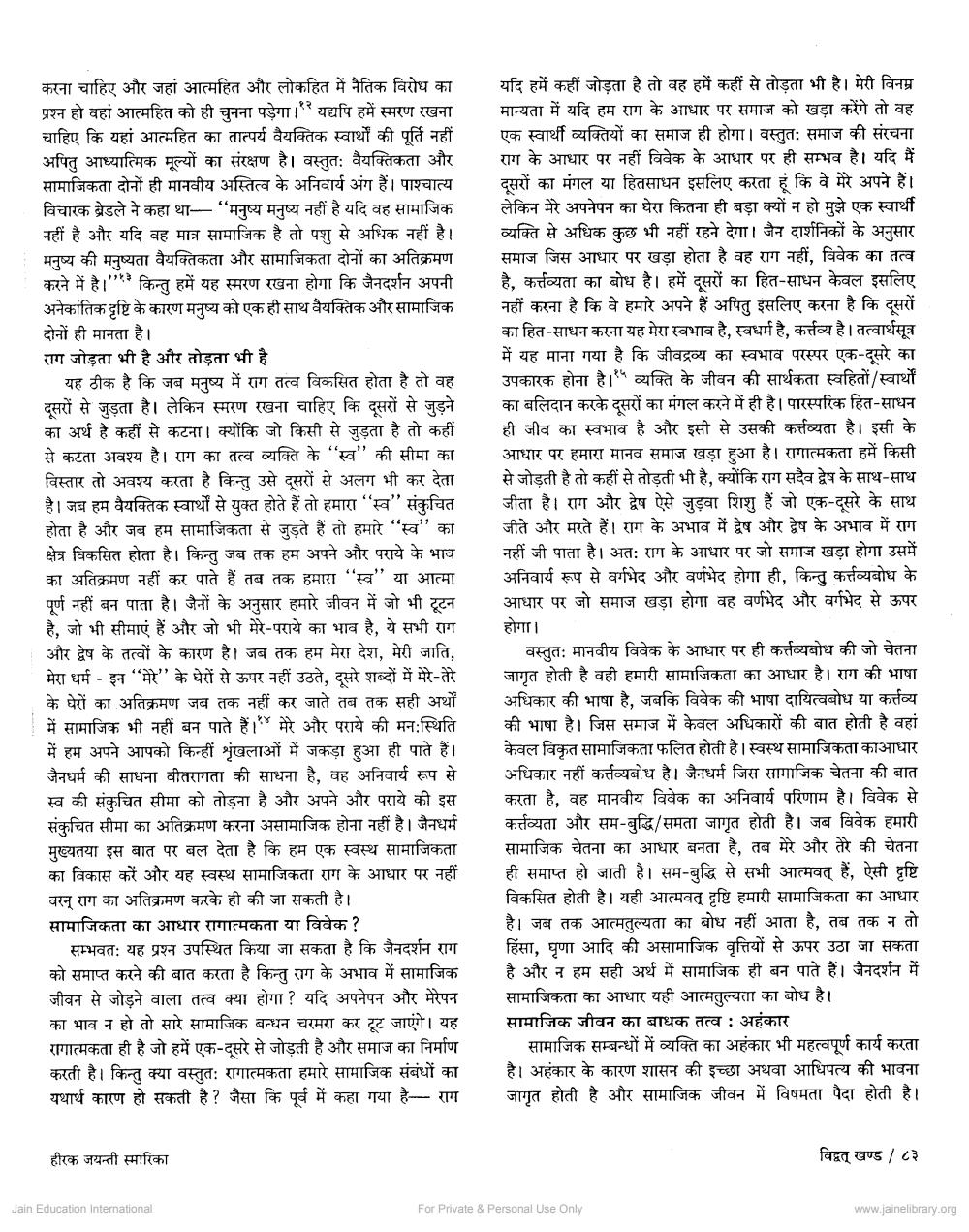Book Title: Jain Dharm me Samajik Chintan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Jain_Vidyalay_Hirak_Jayanti_Granth_012029.pdf View full book textPage 3
________________ करना चाहिए और जहां आत्महित और लोकहित में नैतिक विरोध का प्रश्न हो वहां आत्महित को ही चुनना पड़ेगा। यद्यपि हमें स्मरण रखना चाहिए कि यहां आत्महित का तात्पर्य वैयक्तिक स्वार्थों की पूर्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण है। वस्तुत: वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों ही मानवीय अस्तित्व के अनिवार्य अंग हैं। पाश्चात्य विचारक ब्रेडले ने कहा था- "मनुष्य मनुष्य नहीं है यदि वह सामाजिक नहीं है और यदि वह मात्र सामाजिक है तो पशु से अधिक नहीं है। मनुष्य की मनुष्यता वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों का अतिक्रमण करने में है।"५३ किन्तु हमें यह स्मरण रखना होगा कि जैनदर्शन अपनी अनेकांतिक दृष्टि के कारण मनुष्य को एक ही साथ वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही मानता है। राग जोड़ता भी है और तोड़ता भी है __ यह ठीक है कि जब मनुष्य में राग तत्व विकसित होता है तो वह दूसरों से जुड़ता है। लेकिन स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों से जुड़ने का अर्थ है कहीं से कटना। क्योंकि जो किसी से जुड़ता है तो कहीं से कटता अवश्य है। राग का तत्व व्यक्ति के "स्व" की सीमा का विस्तार तो अवश्य करता है किन्तु उसे दूसरों से अलग भी कर देता है। जब हम वैयक्तिक स्वार्थों से युक्त होते हैं तो हमारा “स्व” संकुचित होता है और जब हम सामाजिकता से जुड़ते हैं तो हमारे "स्व" का क्षेत्र विकसित होता है। किन्तु जब तक हम अपने और पराये के भाव का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं तब तक हमारा "स्व" या आत्मा पूर्ण नहीं बन पाता है। जैनों के अनुसार हमारे जीवन में जो भी टूटन है, जो भी सीमाएं हैं और जो भी मेरे-पराये का भाव है, ये सभी राग और द्वेष के तत्वों के कारण है। जब तक हम मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म - इन “मेरे" के घेरों से ऊपर नहीं उठते, दूसरे शब्दों में मेरे-तेरे के घेरों का अतिक्रमण जब तक नहीं कर जाते तब तक सही अर्थों में सामाजिक भी नहीं बन पाते हैं। मेरे और पराये की मन:स्थिति में हम अपने आपको किन्हीं शृंखलाओं में जकड़ा हुआ ही पाते हैं। जैनधर्म की साधना वीतरागता की साधना है, वह अनिवार्य रूप से स्व की संकुचित सीमा को तोड़ना है और अपने और पराये की इस संकुचित सीमा का अतिक्रमण करना असामाजिक होना नहीं है। जैनधर्म मुख्यतया इस बात पर बल देता है कि हम एक स्वस्थ सामाजिकता का विकास करें और यह स्वस्थ सामाजिकता राग के आधार पर नहीं वरन् राग का अतिक्रमण करके ही की जा सकती है। सामाजिकता का आधार रागात्मकता या विवेक ? सम्भवत: यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि जैनदर्शन राग को समाप्त करने की बात करता है किन्तु राग के अभाव में सामाजिक जीवन से जोड़ने वाला तत्व क्या होगा? यदि अपनेपन और मेरेपन का भाव न हो तो सारे सामाजिक बन्धन चरमरा कर टूट जाएंगे। यह रागात्मकता ही है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है और समाज का निर्माण करती है। किन्तु क्या वस्तुत: रागात्मकता हमारे सामाजिक संबंधों का यथार्थ कारण हो सकती है? जैसा कि पूर्व में कहा गया है- राग यदि हमें कहीं जोड़ता है तो वह हमें कहीं से तोड़ता भी है। मेरी विनम्र मान्यता में यदि हम राग के आधार पर समाज को खड़ा करेंगे तो वह एक स्वार्थी व्यक्तियों का समाज ही होगा। वस्तुत: समाज की संरचना राग के आधार पर नहीं विवेक के आधार पर ही सम्भव है। यदि मैं दूसरों का मंगल या हितसाधन इसलिए करता हूं कि वे मेरे अपने हैं। लेकिन मेरे अपनेपन का घेरा कितना ही बड़ा क्यों न हो मुझे एक स्वार्थी व्यक्ति से अधिक कुछ भी नहीं रहने देगा। जैन दार्शनिकों के अनुसार समाज जिस आधार पर खड़ा होता है वह राग नहीं, विवेक का तत्व है, कर्त्तव्यता का बोध है। हमें दूसरों का हित-साधन केवल इसलिए नहीं करना है कि वे हमारे अपने हैं अपितु इसलिए करना है कि दूसरों का हित-साधन करना यह मेरा स्वभाव है, स्वधर्म है, कर्तव्य है। तत्वार्थसूत्र में यह माना गया है कि जीवद्रव्य का स्वभाव परस्पर एक-दूसरे का उपकारक होना है। व्यक्ति के जीवन की सार्थकता स्वहितों/स्वार्थों का बलिदान करके दूसरों का मंगल करने में ही है। पारस्परिक हित-साधन ही जीव का स्वभाव है और इसी से उसकी कर्त्तव्यता है। इसी के आधार पर हमारा मानव समाज खड़ा हुआ है। रागात्मकता हमें किसी से जोड़ती है तो कहीं से तोड़ती भी है, क्योंकि राग सदैव द्वेष के साथ-साथ जीता है। राग और द्वेष ऐसे जुड़वा शिशु हैं जो एक-दूसरे के साथ जीते और मरते हैं। राग के अभाव में द्वेष और द्वेष के अभाव में राग नहीं जी पाता है। अत: राग के आधार पर जो समाज खड़ा होगा उसमें अनिवार्य रूप से वर्गभेद और वर्णभेद होगा ही, किन्तु कर्त्तव्यबोध के आधार पर जो समाज खड़ा होगा वह वर्णभेद और वर्गभेद से ऊपर होगा। वस्तुत: मानवीय विवेक के आधार पर ही कर्त्तव्यबोध की जो चेतना जागृत होती है वही हमारी सामाजिकता का आधार है। राग की भाषा अधिकार की भाषा है, जबकि विवेक की भाषा दायित्वबोध या कर्त्तव्य की भाषा है। जिस समाज में केवल अधिकारों की बात होती है वहां केवल विकृत सामाजिकता फलित होती है। स्वस्थ सामाजिकता काआधार अधिकार नहीं कर्त्तव्यबध है। जैनधर्म जिस सामाजिक चेतना की बात करता है, वह मानवीय विवेक का अनिवार्य परिणाम है। विवेक से कर्त्तव्यता और सम-बुद्धि/समता जागृत होती है। जब विवेक हमारी सामाजिक चेतना का आधार बनता है, तब मेरे और तेरे की चेतना ही समाप्त हो जाती है। सम-बुद्धि से सभी आत्मवत् हैं, ऐसी दृष्टि विकसित होती है। यही आत्मवत् दृष्टि हमारी सामाजिकता का आधार है। जब तक आत्मतुल्यता का बोध नहीं आता है, तब तक न तो हिंसा, घृणा आदि की असामाजिक वृत्तियों से ऊपर उठा जा सकता है और न हम सही अर्थ में सामाजिक ही बन पाते हैं। जैनदर्शन में सामाजिकता का आधार यही आत्मतुल्यता का बोध है। सामाजिक जीवन का बाधक तत्व : अहंकार ___सामाजिक सम्बन्धों में व्यक्ति का अहंकार भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। अहंकार के कारण शासन की इच्छा अथवा आधिपत्य की भावना जागृत होती है और सामाजिक जीवन में विषमता पैदा होती है। हीरक जयन्ती स्मारिका विद्वत् खण्ड/८३ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8