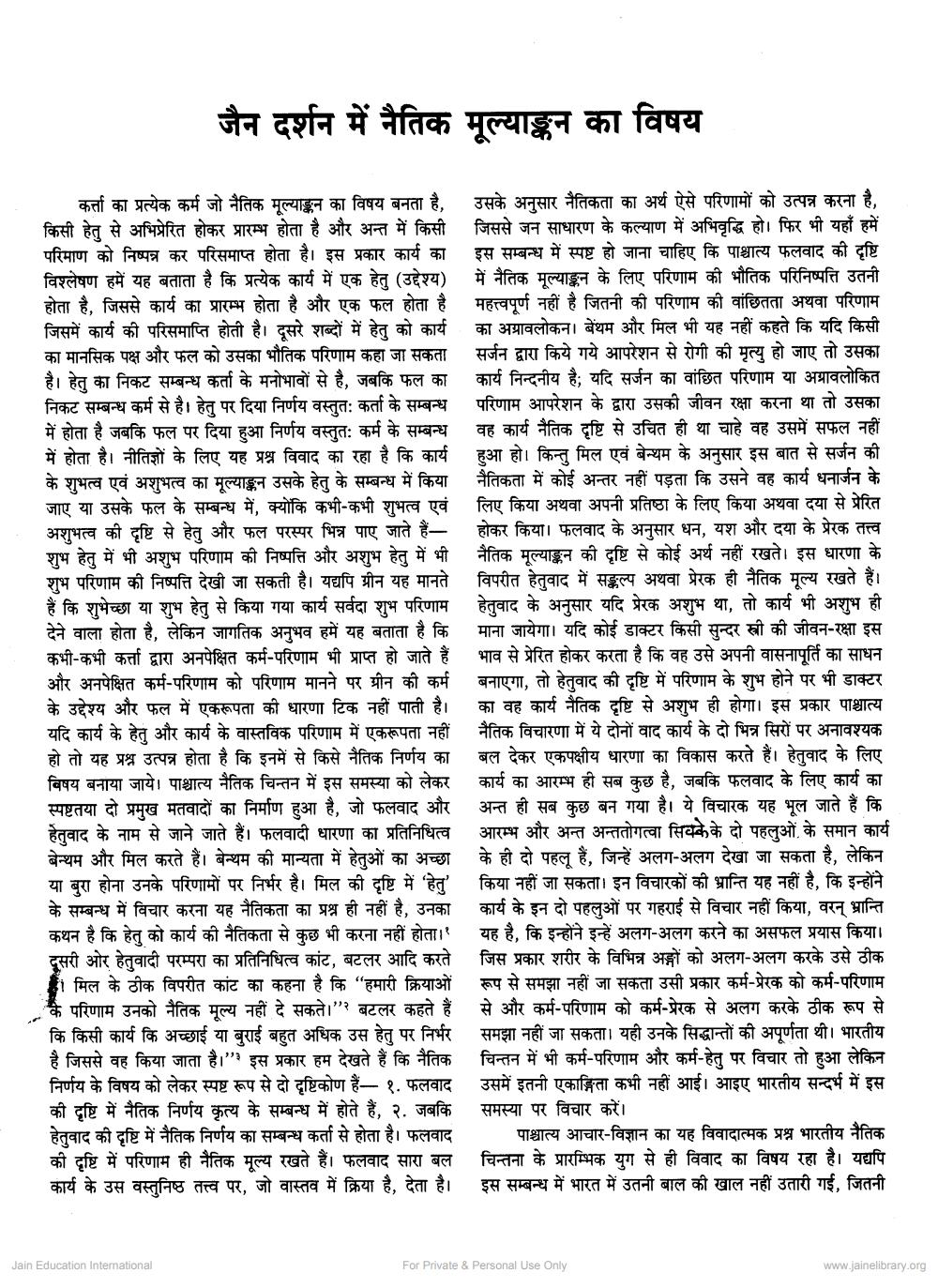Book Title: Jain Darshan me Naitik Mulyankan ka Vishay Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 1
________________ जैन दर्शन में नैतिक मूल्याङ्कन का विषय कर्ता का प्रत्येक कर्म जो नैतिक मूल्याङ्कन का विषय बनता है, किसी हेतु से अभिप्रेरित होकर प्रारम्भ होता है और अन्त में किसी परिमाण को निष्पन्न कर परिसमाप्त होता है। इस प्रकार कार्य का विश्लेषण हमें यह बताता है कि प्रत्येक कार्य में एक हेतु (उद्देश्य) होता है, जिससे कार्य का प्रारम्भ होता है और एक फल होता है जिसमें कार्य की परिसमाप्ति होती है। दूसरे शब्दों में हेतु को कार्य का मानसिक पक्ष और फल को उसका भौतिक परिणाम कहा जा सकता है हेतु का निकट सम्बन्ध कर्ता के मनोभावों से है, जबकि फल का निकट सम्बन्ध कर्म से है हेतु पर दिया निर्णय वस्तुतः कर्ता के सम्बन्ध में होता है जबकि फल पर दिया हुआ निर्णय वस्तुतः कर्म के सम्बन्ध में होता है। नीतिज्ञों के लिए यह प्रश्न विवाद का रहा है कि कार्य के शुभत्व एवं अशुभत्व का मूल्याङ्कन उसके हेतु के सम्बन्ध में किया जाए या उसके फल के सम्बन्ध में, क्योंकि कभी-कभी शुभत्व एवं अशुभत्व की दृष्टि से हेतु और फल परस्पर भिन्न पाए जाते हैं— शुभ हेतु में भी अशुभ परिणाम की निष्पत्ति और अशुभ हेतु में भी शुभ परिणाम की निष्पत्ति देखी जा सकती है। यद्यपि प्रीन यह मानते हैं कि शुभेच्छा या शुभ हेतु से किया गया कार्य सर्वदा शुभ परिणाम देने वाला होता है, लेकिन जागतिक अनुभव हमें यह बताता है कि कभी-कभी कर्ता द्वारा अनपेक्षित कर्म परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं और अनपेक्षित कर्म-परिणाम को परिणाम मानने पर ग्रीन की कर्म के उद्देश्य और फल में एकरूपता की धारणा टिक नहीं पाती है। यदि कार्य के हेतु और कार्य के वास्तविक परिणाम में एकरूपता नहीं हो तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इनमें से किसे नैतिक निर्णय का विषय बनाया जाये। पाश्चात्य नैतिक चिन्तन में इस समस्या को लेकर स्पष्टतया दो प्रमुख मतवादों का निर्माण हुआ है, जो फलबाद और हेतुवाद के नाम से जाने जाते हैं । फलवादी धारणा का प्रतिनिधित्व बेन्थम और मिल करते हैं। बेन्थम की मान्यता में हेतुओं का अच्छा या बुरा होना उनके परिणामों पर निर्भर है। मिल की दृष्टि में 'हेतु' के सम्बन्ध में विचार करना यह नैतिकता का प्रश्न ही नहीं है, उनका कथन है कि हेतु को कार्य की नैतिकता से कुछ भी करना नहीं होता । " दूसरी ओर हेतुवादी परम्परा का प्रतिनिधित्व कांट, बटलर आदि करते है। मिल के ठीक विपरीत कांट का कहना है कि "हमारी क्रियाओं के परिणाम उनको नैतिक मूल्य नहीं दे सकते।"२ बटलर कहते हैं कि किसी कार्य कि अच्छाई या बुराई बहुत अधिक उस हेतु पर निर्भर है जिससे वह किया जाता है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय के विषय को लेकर स्पष्ट रूप से दो दृष्टिकोण हैं— १. फलवाद की दृष्टि में नैतिक निर्णय कृत्य के सम्बन्ध में होते हैं, २. जबकि हेतुवाद की दृष्टि में नैतिक निर्णय का सम्बन्ध कर्ता से होता है । फलवाद की दृष्टि में परिणाम हो नैतिक मूल्य रखते हैं। फलवाद सारा बल कार्य के उस वस्तुनिष्ठ तत्त्व पर, जो वास्तव में क्रिया है, देता है। Jain Education International उसके अनुसार नैतिकता का अर्थ ऐसे परिणामों को उत्पन्न करना है, जिससे जन साधारण के कल्याण में अभिवृद्धि हो । फिर भी यहाँ हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाश्चात्य फलवाद की दृष्टि में नैतिक मूल्याङ्कन के लिए परिणाम की भौतिक परिनिष्पत्ति उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितनी की परिणाम की वांछितता अथवा परिणाम का अग्रावलोकन बेंथम और मिल भी यह नहीं कहते कि यदि किसी सर्जन द्वारा किये गये आपरेशन से रोगी की मृत्यु हो जाए तो उसका कार्य निन्दनीय है; यदि सर्जन का वांछित परिणाम या अग्रावलोकित परिणाम आपरेशन के द्वारा उसकी जीवन रक्षा करना था तो उसका वह कार्य नैतिक दृष्टि से उचित ही था चाहे वह उसमें सफल नहीं हुआ हो । किन्तु मिल एवं बेन्थम के अनुसार इस बात से सर्जन की नैतिकता में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसने वह कार्य धनार्जन के लिए किया अथवा अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया अथवा दया से प्रेरित होकर किया । फलवाद के अनुसार धन, यश और दया के प्रेरक तत्त्व नैतिक मूल्याङ्कन की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं रखते। इस धारणा के विपरीत हेतुवाद में सङ्कल्प अथवा प्रेरक ही नैतिक मूल्य रखते हैं। हेतुवाद के अनुसार यदि प्रेरक अशुभ था, तो कार्य भी अशुभ ही माना जायेगा। यदि कोई डाक्टर किसी सुन्दर स्त्री की जीवन रक्षा इस भाव से प्रेरित होकर करता है कि वह उसे अपनी वासनापूर्ति का साधन बनाएगा, तो हेतुवाद की दृष्टि में परिणाम के शुभ होने पर भी डाक्टर का वह कार्य नैतिक दृष्टि से अशुभ ही होगा। इस प्रकार पाश्चात्य नैतिक विचारणा में ये दोनों वाद कार्य के दो भिन्न सिरों पर अनावश्यक बल देकर एकपक्षीय धारणा का विकास करते हैं। हेतुवाद के लिए कार्य का आरम्भ ही सब कुछ है, जबकि फलवाद के लिए कार्य का अन्त ही सब कुछ बन गया है। ये विचारक यह भूल जाते हैं कि आरम्भ और अन्त अन्ततोगत्वा सिक्के के दो पहलुओं के समान कार्य के ही दो पहलू हैं, जिन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है, लेकिन किया नहीं जा सकता। इन विचारकों की भ्रान्ति यह नहीं है, कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वरन् भ्रान्ति यह है, कि इन्होंने इन्हें अलग-अलग करने का असफल प्रयास किया। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अङ्गों को अलग-अलग करके उसे ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता उसी प्रकार कर्म-प्रेरक को कर्म-परिणाम से और कर्म - परिणाम को कर्म-प्रेरक से अलग करके ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता यही उनके सिद्धान्तों की अपूर्णता थी। भारतीय चिन्तन में भी कर्म-परिणाम और कर्म- हेतु पर विचार तो हुआ लेकिन उसमें इतनी एकाङ्गिता कभी नहीं आई। आइए भारतीय सन्दर्भ में इस समस्या पर विचार करें। पाश्चात्य आचार-विज्ञान का यह विवादात्मक प्रश्न भारतीय नैतिक चिन्तना के प्रारम्भिक युग से ही विवाद का विषय रहा है। यद्यपि इस सम्बन्ध में भारत में उतनी बाल की खाल नहीं उतारी गई. जितनी For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8