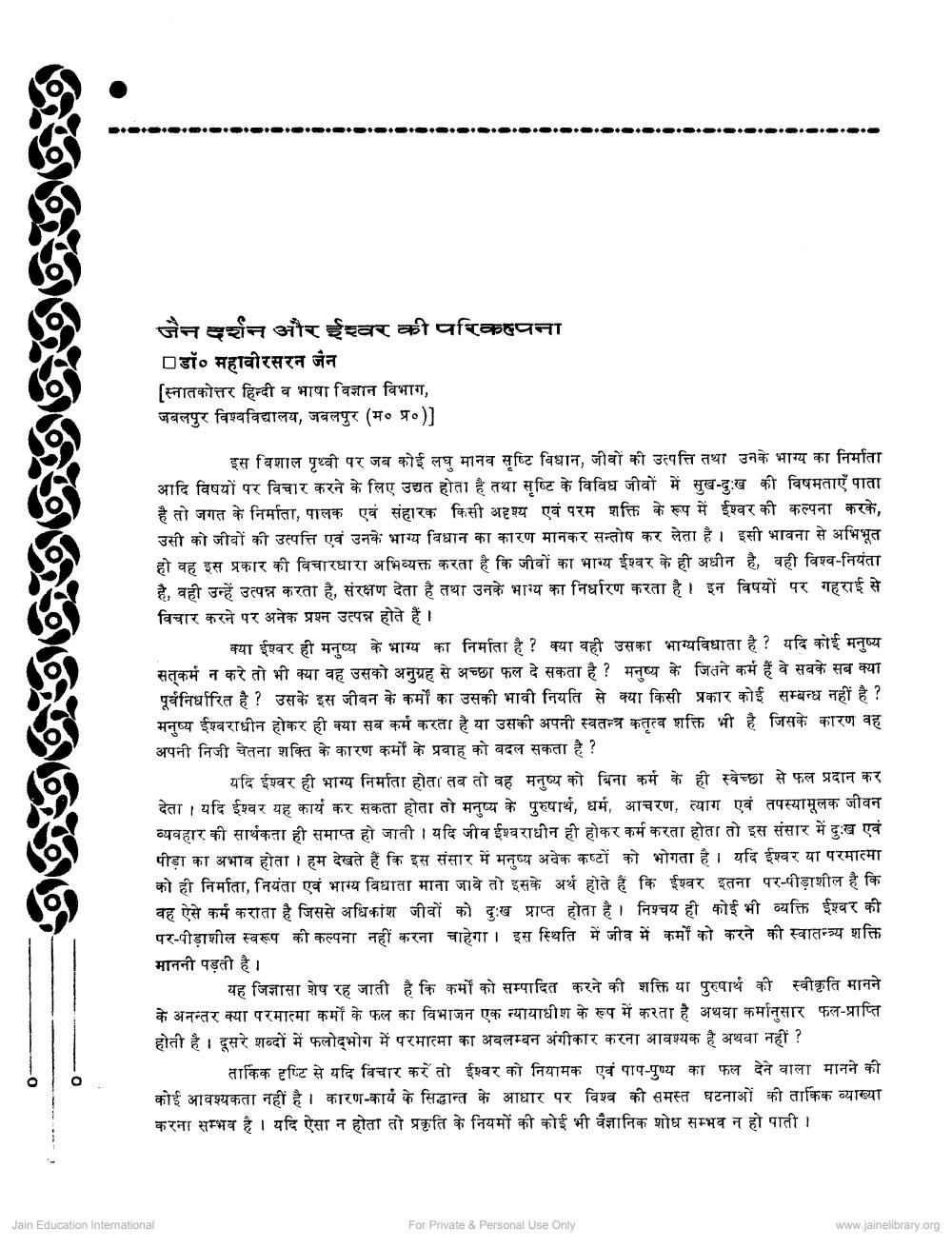Book Title: Jain Darshan aur Ishwar ki Parikalpana Author(s): Mahaveer Saran Jain Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 1
________________ to o too to o जैन दर्शन और ईश्वर की परिकल्पना डॉ० महावीर सरन जैन [स्नातकोत्तर हिन्दी व भाषा विज्ञान विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)] इस विशाल पृथ्वी पर जब कोई लघु मानव सृष्टि विधान, जीवों की उत्पत्ति तथा उनके भाग्य का निर्माता आदि विषयों पर विचार करने के लिए उद्यत होता है तथा सृष्टि के विविध जीवों में सुख-दुःख की विषमताएँ पाता है तो जगत के निर्माता, पालक एवं संहारक किसी अदृश्य एवं परम शक्ति के रूप में ईश्वर की कल्पना करके, उसी को जीवों की उत्पत्ति एवं उनके भाग्य विधान का कारण मानकर सन्तोष कर लेता है। इसी भावना से अभिभूत हो वह इस प्रकार की विचारधारा अभिव्यक्त करता है कि जीवों का भाग्य ईश्वर के ही अधीन है, वही विश्व-नियंता है, वही उन्हें उत्पन्न करता है, संरक्षण देता है तथा उनके भाग्य का निर्धारण करता है। इन विषयों पर गहराई से विचार करने पर अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं । क्या ईश्वर ही मनुष्य के भाग्य का निर्माता है ? क्या वही उसका भाग्यविधाता है ? यदि कोई मनुष्य सत्कर्म न करे तो भी क्या वह उसको अनुग्रह से अच्छा फल दे सकता है ? मनुष्य के जितने कर्म हैं वे सबके सब क्या पूर्वनिर्धारित है? उसके इस जीवन के कर्मों का उसकी भावी नियति से क्या किसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं है ? मनुष्य ईश्वराधीन होकर ही क्या सब कर्म करता है या उसकी अपनी स्वतन्त्र कतृत्व शक्ति भी है जिसके कारण वह अपनी निजी चेतना शक्ति के कारण कर्मों के प्रवाह को बदल सकता है ? यदि ईश्वर ही भाग्य निर्माता होता तब तो वह मनुष्य को बिना कर्म के ही स्वेच्छा से फल प्रदान कर देता । यदि ईश्वर यह कार्य कर सकता होता तो मनुष्य के पुरुषार्थ, धर्म, आचरण, त्याग एवं तपस्यामूलक जीवन व्यवहार की सार्थकता ही समाप्त हो जाती। यदि जीव ईश्वराधीन ही होकर कर्म करता होता तो इस संसार में दुःख एवं पीड़ा का अभाव होता। हम देखते हैं कि इस संसार में मनुष्य अनेक कष्टों को भोगता है । यदि ईश्वर या परमात्मा को ही निर्माता, नियंता एवं भाग्य विधाता माना जावे तो इसके अर्थ होते हैं कि ईश्वर इतना पर पीड़ाशील है कि वह ऐसे कर्म कराता है जिससे अधिकांश जीवों को दुःख प्राप्त होता है । निश्चय ही कोई भी परपीड़ाशील स्वरूप की कल्पना नहीं करना चाहेगा। इस स्थिति में जीव में कर्मों को करने माननी पड़ती है। व्यक्ति ईश्वर की की स्वातन्त्र्य शक्ति यह जिज्ञासा शेष रह जाती है कि कर्मों को सम्पादित करने की शक्ति या पुरुषार्थ की स्वीकृति मानने के अनन्तर क्या परमात्मा कर्मों के फल का विभाजन एक न्यायाधीश के रूप में करता है अथवा कर्मानुसार फल प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में फलोद्भोग में परमात्मा का अवलम्बन अंगीकार करना आवश्यक है अथवा नहीं ? तार्किक दृष्टि से यदि विचार करें तो ईश्वर को नियामक एवं पाप-पुण्य का फल देने वाला मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण कार्य के सिद्धान्त के आधार पर विश्व की समस्त घटनाओं की तार्किक व्याख्या करना सम्भव है । यदि ऐसा न होता तो प्रकृति के नियमों की कोई भी वैज्ञानिक शोध सम्भव न हो पाती । Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6