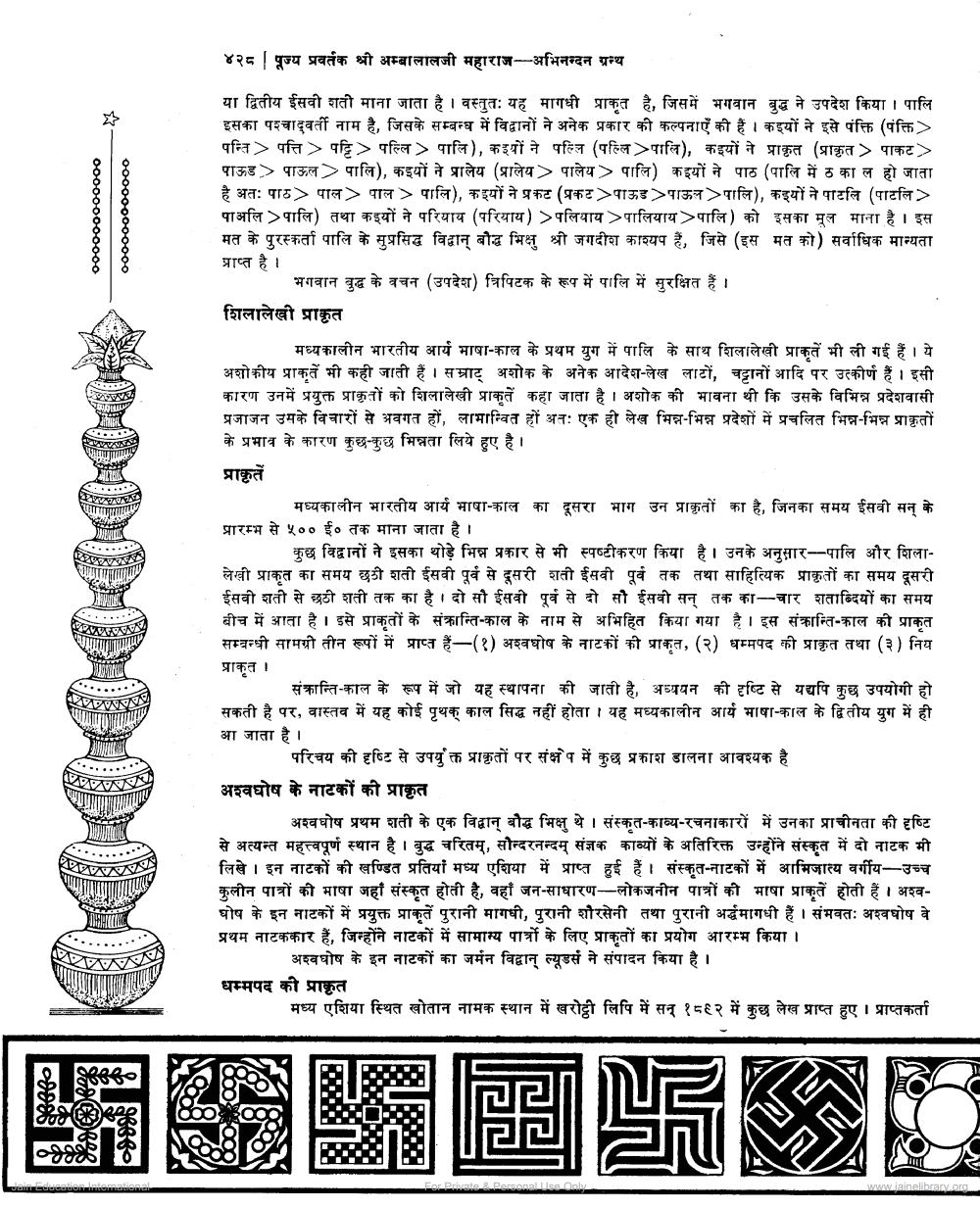Book Title: Jain Agam aur Prakrit Bhasha Vigyan ke Pariprekshya me Ek Parishilan Author(s): Shantidevi Jain Publisher: Z_Ambalalji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012038.pdf View full book textPage 6
________________ ४२८ | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ 000000000000 ०००००००००००० या द्वितीय ईसवी शती माना जाता है । वस्तुत: यह मागधी प्राकृत है, जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश किया। पालि इसका पश्चाद्वर्ती नाम है, जिसके सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएँ की हैं । कइयों ने इसे पंक्ति (पंक्ति> पन्ति > पत्ति > पट्टि > पल्लि > पालि), कइयों ने पल्लि (पल्लि>पालि), कइयों ने प्राकृत (प्राकृत > पाकट> पाऊड> पाऊल > पालि), कइयों ने प्रालेय (प्रालेय> पालेय > पालि) कइयों ने पाठ (पालि में ठ का ल हो जाता है अतः पाठ> पाल> पाल > पालि), कइयों ने प्रकट (प्रकट>पाऊड>पाऊल>पालि), कइयों ने पाटलि (पाटलि> पाअलि >पालि) तथा कइयों ने परियाय (परियाय)>पलियाय >पालियाय >पालि) को इसका मूल माना है । इस मत के पुरस्कर्ता पालि के सुप्रसिद्ध विद्वान् बौद्ध भिक्षु श्री जगदीश काश्यप हैं, जिसे (इस मत को) सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। भगवान बुद्ध के वचन (उपदेश) त्रिपिटक के रूप में पालि में सुरक्षित हैं । शिलालेखी प्राकृत __ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा-काल के प्रथम युग में पालि के साथ शिलालेखी प्राकृतें भी ली गई हैं । ये अशोकीय प्राकृत भी कही जाती हैं । सम्राट अशोक के अनेक आदेश-लेख लाटों, चट्टानों आदि पर उत्कीर्ण हैं । इसी कारण उनमें प्रयुक्त प्राकृतों को शिलालेखी प्राकृतें कहा जाता है । अशोक की भावना थी कि उसके विभिन्न प्रदेशवासी प्रजाजन उसके विचारों से अवगत हों, लाभान्वित हों अतः एक ही लेख भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्राकृतों के प्रभाव के कारण कुछ-कुछ भिन्नता लिये हुए है। स्वसBA ... WARNING LHIPRIK प्राकृतें Mon मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा-काल का दूसरा भाग उन प्राकृतों का है, जिनका समय ईसवी सन् के प्रारम्भ से ५००ई० तक माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसका थोड़े भिन्न प्रकार से भी स्पष्टीकरण किया है। उनके अनुसार-पालि और शिलालेखी प्राकृत का समय छठी शती ईसवी पूर्व से दूसरी शती ईसवी पूर्व तक तथा साहित्यिक प्राकृतों का समय दूसरी ईसवी शती से छठी शती तक का है। दो सौ ईसवी पूर्व से दो सौ ईसवी सन् तक का-चार शताब्दियों का समय बीच में आता है। इसे प्राकृतों के संक्रान्ति-काल के नाम से अभिहित किया गया है। इस संक्रान्ति-काल की प्राकृत सम्बन्धी सामग्री तीन रूपों में प्राप्त हैं-(१) अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, (२) धम्मपद की प्राकृत तथा (३) निय प्राकृत। संक्रान्ति-काल के रूप में जो यह स्थापना की जाती है, अध्ययन की दृष्टि से यद्यपि कुछ उपयोगी हो सकती है पर, वास्तव में यह कोई पृथक् काल सिद्ध नहीं होता। यह मध्यकालीन आर्य भाषा-काल के द्वितीय युग में ही आ जाता है। परिचय की दृष्टि से उपर्युक्त प्राकृतों पर संक्षेप में कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत अश्वघोष प्रथम शती के एक विद्वान् बौद्ध भिक्षु थे । संस्कृत-काव्य-रचनाकारों में उनका प्राचीनता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । बुद्ध चरितम्, सौन्दरनन्दम् संज्ञक काव्यों के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत में दो नाटक भी लिखे । इन नाटकों की खण्डित प्रतियां मध्य एशिया में प्राप्त हुई हैं। संस्कृत-नाटकों में आभिजात्य वर्गीय-उच्च कुलीन पात्रों की माषा जहाँ संस्कृत होती है, वहाँ जन-साधारण-लोकजनीन पात्रों की भाषा प्राकृतें होती हैं । अश्वघोष के इन नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतें पुरानी मागधी, पुरानी शौरसेनी तथा पुरानी अर्द्धमागधी हैं । संभवतः अश्वघोष वे प्रथम नाटककार हैं, जिन्होंने नाटकों में सामान्य पात्रों के लिए प्राकृतों का प्रयोग आरम्भ किया। अश्वघोष के इन नाटकों का जर्मन विद्वान् ल्यूडर्स ने संपादन किया है। धम्मपद की प्राकृत मध्य एशिया स्थित खोतान नामक स्थान में खरोट्ठी लिपि में सन् १८६२ में कुछ लेख प्राप्त हुए । प्राप्तकर्ता AV mEducationainamational For Davet Reconelise.ch www.jainelibrantinoPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12