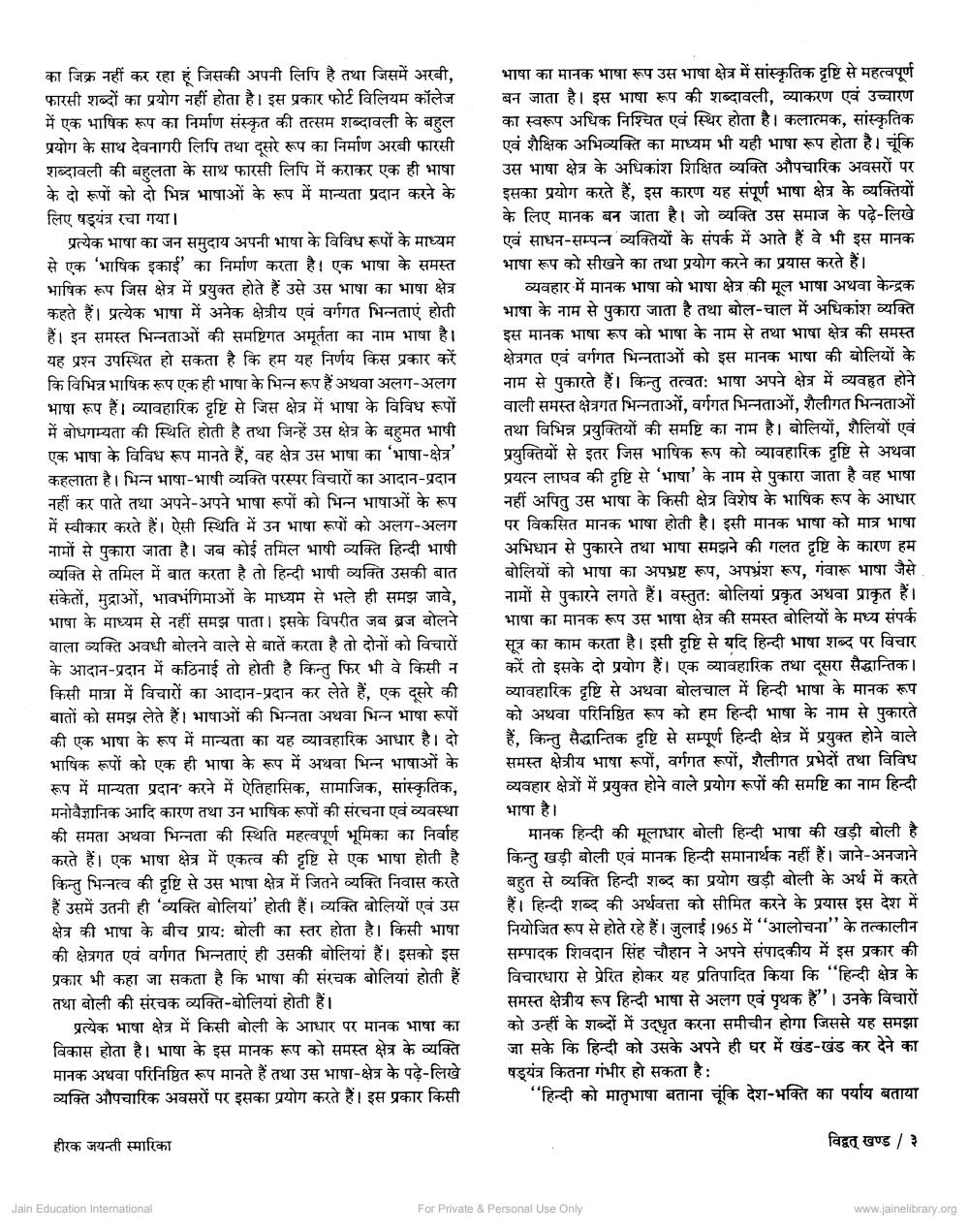Book Title: Hindi bhasha ke Vividh Rup Author(s): Mahaveer Saran Jain Publisher: Z_Jain_Vidyalay_Hirak_Jayanti_Granth_012029.pdf View full book textPage 2
________________ का जिक्र नहीं कर रहा हूं जिसकी अपनी लिपि है तथा जिसमें अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज में एक भाषिक रूप का निर्माण संस्कृत की तत्सम शब्दावली के बहुल प्रयोग के साथ देवनागरी लिपि तथा दूसरे रूप का निर्माण अरबी फारसी शब्दावली की बहुलता के साथ फारसी लिपि में कराकर एक ही भाषा के दो रूपों को दो भिन्न भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। प्रत्येक भाषा का जन समुदाय अपनी भाषा के विविध रूपों के माध्यम से एक 'भाषिक इकाई' का निर्माण करता है। एक भाषा के समस्त भाषिक रूप जिस क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं उसे उस भाषा का भाषा क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक क्षेत्रीय एवं वर्गगत भिन्नताएं होती हैं। इन समस्त भिन्नताओं की समष्टिगत अमूर्तता का नाम भाषा है। यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि हम यह निर्णय किस प्रकार करें कि विभिन्न भाषिक रूप एक ही भाषा के भिन्न रूप हैं अथवा अलग-अलग भाषा रूप हैं। व्यावहारिक दृष्टि से जिस क्षेत्र में भाषा के विविध रूपों में बोधगम्यता की स्थिति होती है तथा जिन्हें उस क्षेत्र के बहुमत भाषी एक भाषा के विविध रूप मानते हैं, वह क्षेत्र उस भाषा का भाषा-क्षेत्र' कहलाता है। भिन्न भाषा-भाषी व्यक्ति परस्पर विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर पाते तथा अपने-अपने भाषा रूपों को भिन्न भाषाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में उन भाषा रूपों को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। जब कोई तमिल भाषी व्यक्ति हिन्दी भाषी व्यक्ति से तमिल में बात करता है तो हिन्दी भाषी व्यक्ति उसकी बात संकेतों, मुद्राओं, भावभंगिमाओं के माध्यम से भले ही समझ जावे, भाषा के माध्यम से नहीं समझ पाता। इसके विपरीत जब ब्रज बोलने वाला व्यक्ति अवधी बोलने वाले से बातें करता है तो दोनों को विचारों के आदान-प्रदान में कठिनाई तो होती है किन्तु फिर भी वे किसी न किसी मात्रा में विचारों का आदान-प्रदान कर लेते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। भाषाओं की भिन्नता अथवा भिन्न भाषा रूपों की एक भाषा के रूप में मान्यता का यह व्यावहारिक आधार है। दो भाषिक रूपों को एक ही भाषा के रूप में अथवा भिन्न भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करने में ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आदि कारण तथा उन भाषिक रूपों की संरचना एवं व्यवस्था की समता अथवा भिन्नता की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक भाषा क्षेत्र में एकत्व की दृष्टि से एक भाषा होती है किन्तु भिन्नत्व की दृष्टि से उस भाषा क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसमें उतनी ही 'व्यक्ति बोलियां होती हैं। व्यक्ति बोलियों एवं उस क्षेत्र की भाषा के बीच प्रायः बोली का स्तर होता है। किसी भाषा की क्षेत्रगत एवं वर्गगत भिन्नताएं ही उसकी बोलियां हैं। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि भाषा की संरचक बोलियां होती हैं तथा बोली की संरचक व्यक्ति-बोलियां होती हैं। प्रत्येक भाषा क्षेत्र में किसी बोली के आधार पर मानक भाषा का विकास होता है। भाषा के इस मानक रूप को समस्त क्षेत्र के व्यक्ति मानक अथवा परिनिष्ठित रूप मानते हैं तथा उस भाषा-क्षेत्र के पढ़े-लिखे व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार किसी भाषा का मानक भाषा रूप उस भाषा क्षेत्र में सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। इस भाषा रूप की शब्दावली, व्याकरण एवं उच्चारण का स्वरूप अधिक निश्चित एवं स्थिर होता है। कलात्मक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी यही भाषा रूप होता है। चूंकि उस भाषा क्षेत्र के अधिकांश शिक्षित व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर इसका प्रयोग करते हैं, इस कारण यह संपूर्ण भाषा क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए मानक बन जाता है। जो व्यक्ति उस समाज के पढ़े-लिखे एवं साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं वे भी इस मानक भाषा रूप को सीखने का तथा प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। ___ व्यवहार में मानक भाषा को भाषा क्षेत्र की मूल भाषा अथवा केन्द्रक भाषा के नाम से पुकारा जाता है तथा बोल-चाल में अधिकांश व्यक्ति इस मानक भाषा रूप को भाषा के नाम से तथा भाषा क्षेत्र की समस्त क्षेत्रगत एवं वर्गगत भिन्नताओं को इस मानक भाषा की बोलियों के नाम से पुकारते हैं। किन्तु तत्वत: भाषा अपने क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली समस्त क्षेत्रगत भिन्नताओं, वर्गगत भिन्नताओं, शैलीगत भिन्नताओं तथा विभिन्न प्रयुक्तियों की समष्टि का नाम है। बोलियों, शैलियों एवं प्रयुक्तियों से इतर जिस भाषिक रूप को व्यावहारिक दृष्टि से अथवा प्रयत्न लाघव की दृष्टि से 'भाषा' के नाम से पुकारा जाता है वह भाषा नहीं अपितु उस भाषा के किसी क्षेत्र विशेष के भाषिक रूप के आधार पर विकसित मानक भाषा होती है। इसी मानक भाषा को मात्र भाषा अभिधान से पुकारने तथा भाषा समझने की गलत दृष्टि के कारण हम बोलियों को भाषा का अपभ्रष्ट रूप, अपभ्रंश रूप, गंवारू भाषा जैसे नामों से पुकारने लगते हैं। वस्तुतः बोलियां प्रकृत अथवा प्राकृत हैं। भाषा का मानक रूप उस भाषा क्षेत्र की समस्त बोलियों के मध्य संपर्क सूत्र का काम करता है। इसी दृष्टि से यदि हिन्दी भाषा शब्द पर विचार करें तो इसके दो प्रयोग हैं। एक व्यावहारिक तथा दूसरा सैद्धान्तिक। व्यावहारिक दृष्टि से अथवा बोलचाल में हिन्दी भाषा के मानक रूप को अथवा परिनिष्ठित रूप को हम हिन्दी भाषा के नाम से पुकारते हैं, किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले समस्त क्षेत्रीय भाषा रूपों, वर्गगत रूपों, शैलीगत प्रभेदों तथा विविध व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले प्रयोग रूपों की समष्टि का नाम हिन्दी भाषा है। ___ मानक हिन्दी की मूलाधार बोली हिन्दी भाषा की खड़ी बोली है किन्तु खड़ी बोली एवं मानक हिन्दी समानार्थक नहीं हैं। जाने-अनजाने बहुत से व्यक्ति हिन्दी शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के अर्थ में करते हैं। हिन्दी शब्द की अर्थवत्ता को सीमित करने के प्रयास इस देश में नियोजित रूप से होते रहे हैं। जुलाई 1965 में “आलोचना" के तत्कालीन सम्पादक शिवदान सिंह चौहान ने अपने संपादकीय में इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर यह प्रतिपादित किया कि “हिन्दी क्षेत्र के समस्त क्षेत्रीय रूप हिन्दी भाषा से अलग एवं पृथक हैं"। उनके विचारों को उन्हीं के शब्दों में उद्धृत करना समीचीन होगा जिससे यह समझा जा सके कि हिन्दी को उसके अपने ही घर में खंड-खंड कर देने का षड्यंत्र कितना गंभीर हो सकता है: "हिन्दी को मातृभाषा बताना चूंकि देश-भक्ति का पर्याय बताया हीरक जयन्ती स्मारिका विद्वत् खण्ड /३ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4