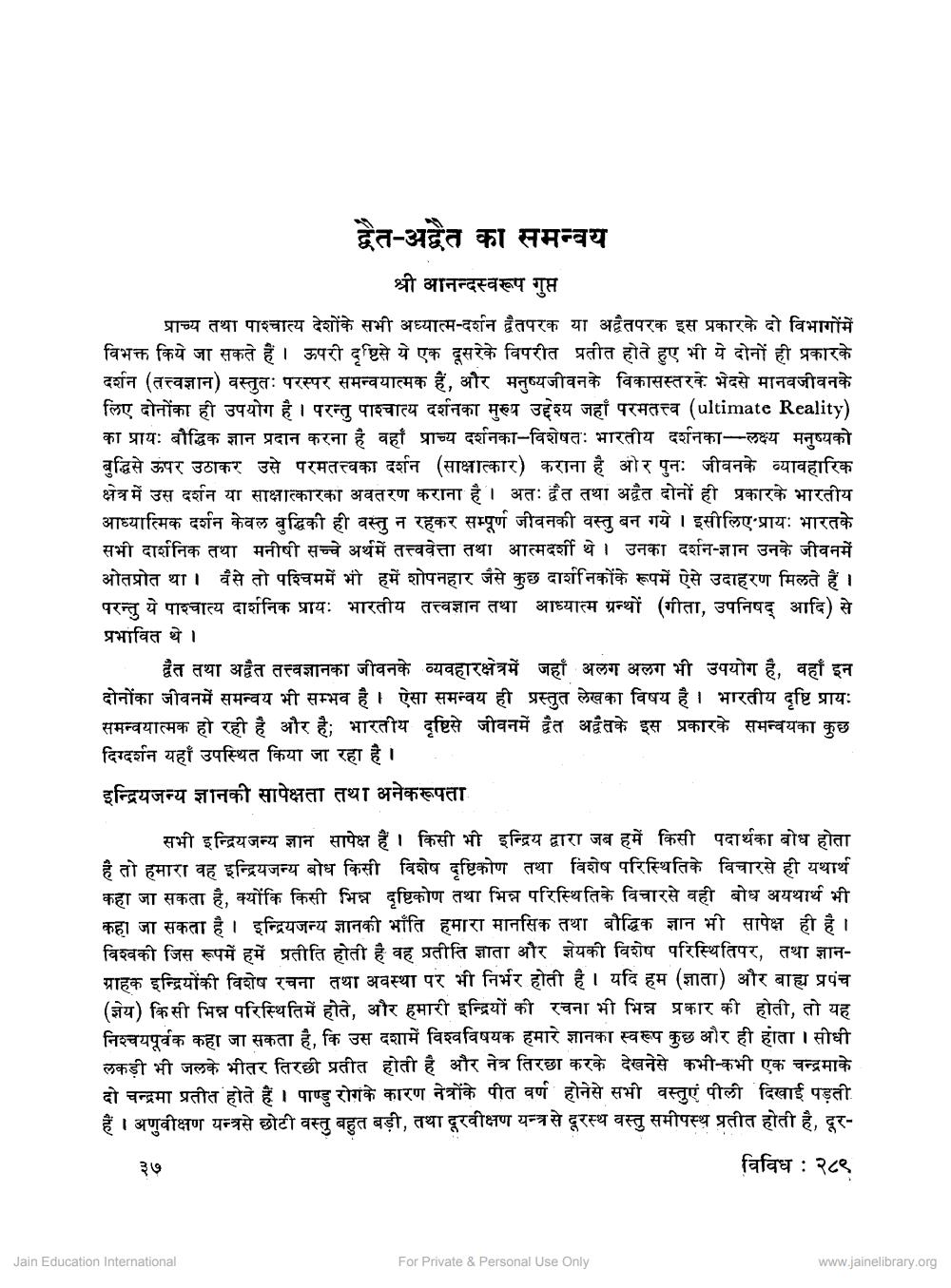Book Title: Dwait Adwait ka Samanvay Author(s): Anandswarup Gupt Publisher: Z_Nahta_Bandhu_Abhinandan_Granth_012007.pdf View full book textPage 1
________________ द्वैत-अद्वैत का समन्वय श्री आनन्दस्वरूप गुप्त प्राप्य तथा पाश्चात्य देशोंके सभी अध्यात्म-दर्शन द्वैतपरक या अद्वैतपरक इस प्रकारके दो विभागों में विभक्त किये जा सकते हैं। ऊपरी दृष्टिसे ये एक दूसरेके विपरीत प्रतीत होते हुए भी ये दोनों ही प्रकारके दर्शन ( तत्त्वज्ञान) वस्तुतः परस्पर समन्वयात्मक हैं, और मनुष्यजीवन के विकासस्तर के भेदसे मानवजीवनके लिए दोनोंका ही उपयोग है। परन्तु पाश्चात्य दर्शनका मुख्य उद्देश्य जहाँ परमतत्त्व ( ultimate Reality ) का प्रायः बौद्धिक ज्ञान प्रदान करना है वहाँ प्राच्य दर्शनका - विशेषतः भारतीय दर्शनका - लक्ष्य मनुष्यको बुद्धिसे ऊपर उठाकर उसे परमतत्त्वका दर्शन ( साक्षात्कार ) कराना है ओर पुनः जीवनके व्यावहारिक क्षेत्र में उस दर्शन या साक्षात्कारका अवतरण कराना है । अतः द्वैत तथा अद्वैत दोनों ही प्रकारके भारतीय आध्यात्मिक दर्शन केवल बुद्धिकी ही वस्तु न रहकर सम्पूर्ण जीवनकी वस्तु बन गये । इसीलिए प्रायः भारतके सभी दार्शनिक तथा मनीषी सच्चे अर्थमे तत्ववेत्ता तथा आत्मदर्शी थे। उनका दर्शन-ज्ञान उनके जीवनमें ओतप्रोत था । वैसे तो पश्चिममें भी हमें शोपनहार जैसे कुछ दार्शनिकोंके रूपमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं । परन्तु ये पाश्चात्य दार्शनिक प्रायः भारतीय तत्त्वज्ञान तथा आध्यात्म ग्रन्थों (गीता, उपनिषद् आदि) से प्रभावित थे । द्वैत तथा अद्वैत तत्वज्ञानका जीवनके व्यवहारक्षेत्रमें जहाँ अलग अलग भी उपयोग है, वहाँ इन दोनोंका जीवनमें समन्वय भी सम्भव है। ऐसा समन्वय ही प्रस्तुत लेखका विषय है। भारतीय दृष्टि प्रायः समन्वयात्मक हो रही है और है भारतीय दृष्टिसे जीवनमें द्वैत अद्वैत इस प्रकारके समन्वयका कुछ दिग्दर्शन यहाँ उपस्थित किया जा रहा है । इन्द्रियजन्य ज्ञानकी सापेक्षता तथा अनेकरूपता पदार्थका बोध होता विचारसे ही यथार्थ सभी इन्द्रियजन्य ज्ञान सापेक्ष है। किसी भी इन्द्रिय द्वारा जब हमें किसी है तो हमारा वह इन्द्रियजन्य बोध किसी विशेष दृष्टिकोण तथा विशेष परिस्थितिके कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भिन्न दृष्टिकोण तथा भिन्न परिस्थितिके विचारसे वही बोध अयथार्थ भी कहा जा सकता है । इन्द्रियजन्य ज्ञानकी भाँति हमारा मानसिक तथा बौद्धिक ज्ञान भी सापेक्ष ही है । विश्वकी जिस रूपमें हमें प्रतीति होती है वह प्रतीति ज्ञाता और ज्ञेयकी विशेष परिस्थितिपर, तथा ज्ञानग्राहक इन्द्रियोंकी विशेष रचना तथा अवस्था पर भी निर्भर होती है। यदि हम (ज्ञाता) और बाह्य प्रपंच (ज्ञेय) किसी भिन्न परिस्थितिमें होते और हमारी इन्द्रियों की रचना भी भिन्न प्रकार की होती, तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, कि उस दशामें विश्वविषयक हमारे ज्ञानका स्वरूप कुछ और ही होता । सीधी लकड़ी भी जलके भीतर तिरछी प्रतीत होती है और नेत्र तिरछा करके देखनेसे कभी-कभी एक चन्द्रमाके दो चन्द्रमा प्रतीत होते हैं। पाण्डु रोगके कारण नेत्रोंके पीत वर्ण होनेसे सभी वस्तुएं पीली दिखाई पड़ती हैं । अणुवीक्षण यन्त्रसे छोटी वस्तु बहुत बड़ी, तथा दूरवीक्षण यन्त्र से दूरस्थ वस्तु समीपस्थ प्रतीत होती है, दूरविविध २८९ ३७ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8