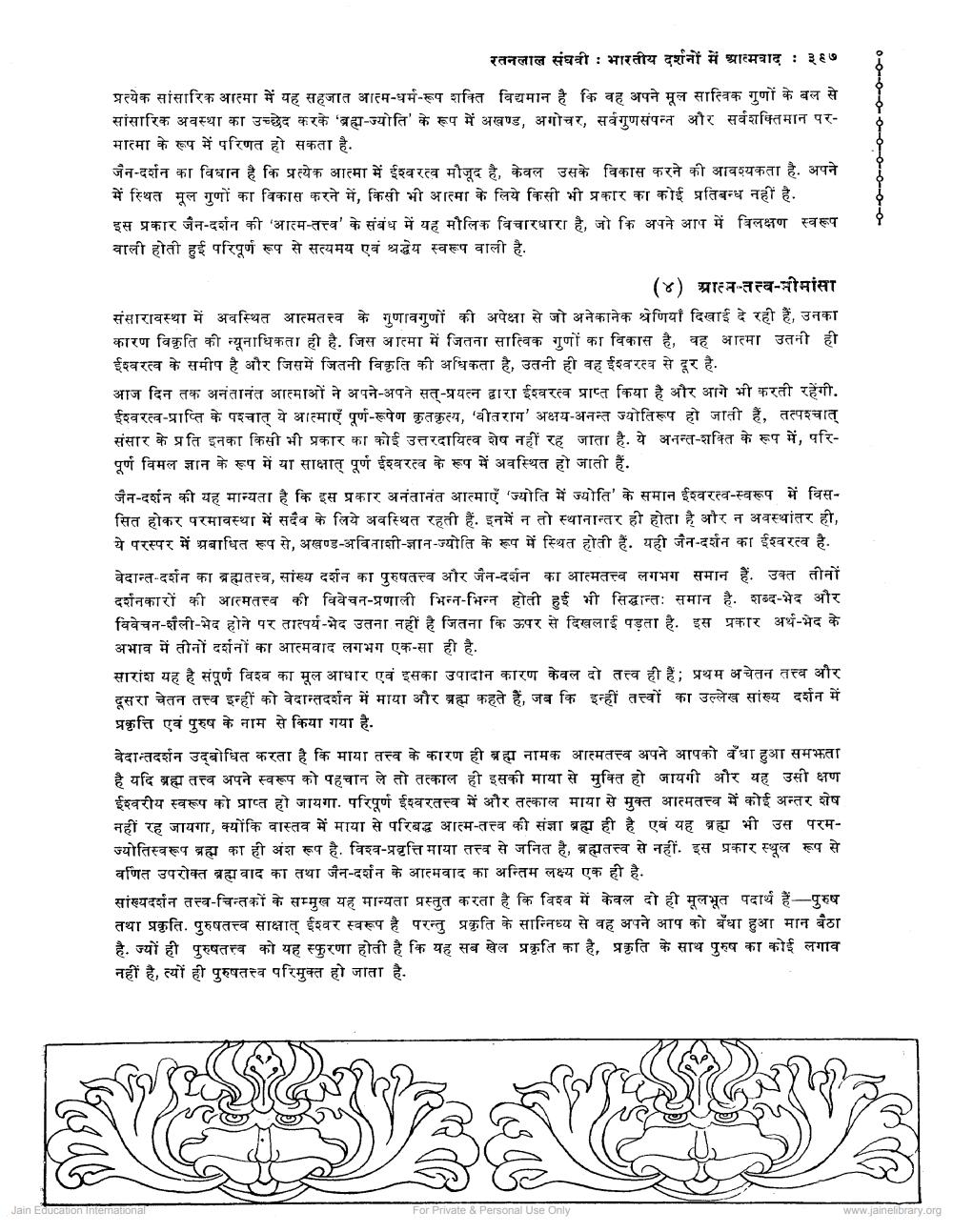Book Title: Bharatiya Darshano me Atmavad Author(s): Ratanlal Sanghvi Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 3
________________ रतनलाल संघवी : भारतीय दर्शनों में प्रात्मवाद : 367 प्रत्येक सांसारिक आत्मा में यह सहजात आत्म-धर्म-रूप शक्ति विद्यमान है कि वह अपने मूल सात्विक गुणों के बल से सांसारिक अवस्था का उच्छेद करके 'ब्रह्म-ज्योति' के रूप में अखण्ड, अगोचर, सर्वगुणसंपन्न और सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में परिणत हो सकता है. जैन-दर्शन का विधान है कि प्रत्येक आत्मा में ईश्वरत्व मौजूद है, केवल उसके विकास करने की आवश्यकता है. अपने में स्थित मूल गुणों का विकास करने में, किसी भी आत्मा के लिये किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है. इस प्रकार जैन-दर्शन की 'आत्म-तत्त्व' के संबंध में यह मौलिक विचारधारा है, जो कि अपने आप में विलक्षण स्वरूप वाली होती हुई परिपूर्ण रूप से सत्यमय एवं श्रद्धेय स्वरूप वाली है. (4) प्रात्म-तत्व-जीमांसा संसारावस्था में अवस्थित आत्मतत्त्व के गुणावगुणों की अपेक्षा से जो अनेकानेक श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं, उनका कारण विकृति की न्यूनाधिकता ही है. जिस आत्मा में जितना सात्विक गुणों का विकास है, वह आत्मा उतनी ही ईश्वरत्व के समीप है और जिसमें जितनी विकृति की अधिकता है, उतनी ही वह ईश्वरत्व से दूर है. आज दिन तक अनंतानंत आत्माओं ने अपने-अपने सत्-प्रयत्न द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है और आगे भी करती रहेंगी. ईश्वरत्व-प्राप्ति के पश्चात् ये आत्माएँ पूर्ण-रूपेण कृतकृत्य, 'वीतराग' अक्षय-अनन्त ज्योतिरूप हो जाती हैं, तत्पश्चात् संसार के प्रति इनका किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व शेष नहीं रह जाता है. ये अनन्त-शक्ति के रूप में, परिपूर्ण विमल ज्ञान के रूप में या साक्षात् पूर्ण ईश्वरत्व के रूप में अवस्थित हो जाती हैं. जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि इस प्रकार अनंतानंत आत्माएँ 'ज्योति में ज्योति' के समान ईश्वरत्व-स्वरूप में विससित होकर परमावस्था में सदैव के लिये अवस्थित रहती हैं. इनमें न तो स्थानान्तर ही होता है और न अवस्थांतर ही, ये परस्पर में अबाधित रूप से, अखण्ड-अविनाशी-ज्ञान-ज्योति के रूप में स्थित होती हैं. यही जैन-दर्शन का ईश्वरत्व है. वेदान्त-दर्शन का ब्रह्मतत्त्व, सांख्य दर्शन का पुरुषतत्त्व और जैन-दर्शन का आत्मतत्त्व लगभग समान हैं. उक्त तीनों दर्शनकारों की आत्मतत्त्व की विवेचन-प्रणाली भिन्न-भिन्न होती हई भी सिद्धान्तः समान है. शब्द-भेद और विवेचन-शैली-भेद होने पर तात्पर्य-भेद उतना नहीं है जितना कि ऊपर से दिखलाई पड़ता है. इस प्रकार अर्थ-भेद के अभाव में तीनों दर्शनों का आत्मवाद लगभग एक-सा ही है. सारांश यह है संपूर्ण विश्व का मूल आधार एवं इसका उपादान कारण केवल दो तत्त्व ही हैं ; प्रथम अचेतन तत्त्व और दूसरा चेतन तत्त्व इन्हीं को वेदान्तदर्शन में माया और ब्रह्म कहते हैं, जब कि इन्हीं तत्त्वों का उल्लेख सांख्य दर्शन में प्रकृत्ति एवं पुरुष के नाम से किया गया है. वेदान्तदर्शन उद्बोधित करता है कि माया तत्त्व के कारण ही ब्रह्म नामक आत्मतत्त्व अपने आपको बँधा हुआ समझता है यदि ब्रह्म तत्त्व अपने स्वरूप को पहचान ले तो तत्काल ही इसकी माया से मुक्ति हो जायगी और यह उसी क्षण ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त हो जायगा. परिपूर्ण ईश्वरतत्त्व में और तत्काल माया से मुक्त आत्मतत्त्व में कोई अन्तर शेष नहीं रह जायगा, क्योंकि वास्तव में माया से परिबद्ध आत्म-तत्त्व की संज्ञा ब्रह्म ही है एवं यह ब्रह्म भी उस परमज्योतिस्वरूप ब्रह्म का ही अंश रूप है, विश्व-प्रवृत्ति माया तत्त्व से जनित है, ब्रह्मतत्त्व से नहीं. इस प्रकार स्थूल रूप से वणित उपरोक्त ब्रह्म वाद का तथा जैन-दर्शन के आत्मवाद का अन्तिम लक्ष्य एक ही है. सांख्यदर्शन तत्त्व-चिन्तकों के सम्मुख यह मान्यता प्रस्तुत करता है कि विश्व में केवल दो ही मूलभूत पदार्थ हैं—पुरुष तथा प्रकृति. पुरुषतत्त्व साक्षात् ईश्वर स्वरूप है परन्तु प्रकृति के सान्निध्य से वह अपने आप को बँधा हुआ मान बैठा है. ज्यों ही पुरुषतत्त्व को यह स्फुरणा होती है कि यह सब खेल प्रकृति का है, प्रकृति के साथ पुरुष का कोई लगाव नहीं है, त्यों ही पुरुषतत्त्व परिमुक्त हो जाता है. Jain Education Intematonal For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3