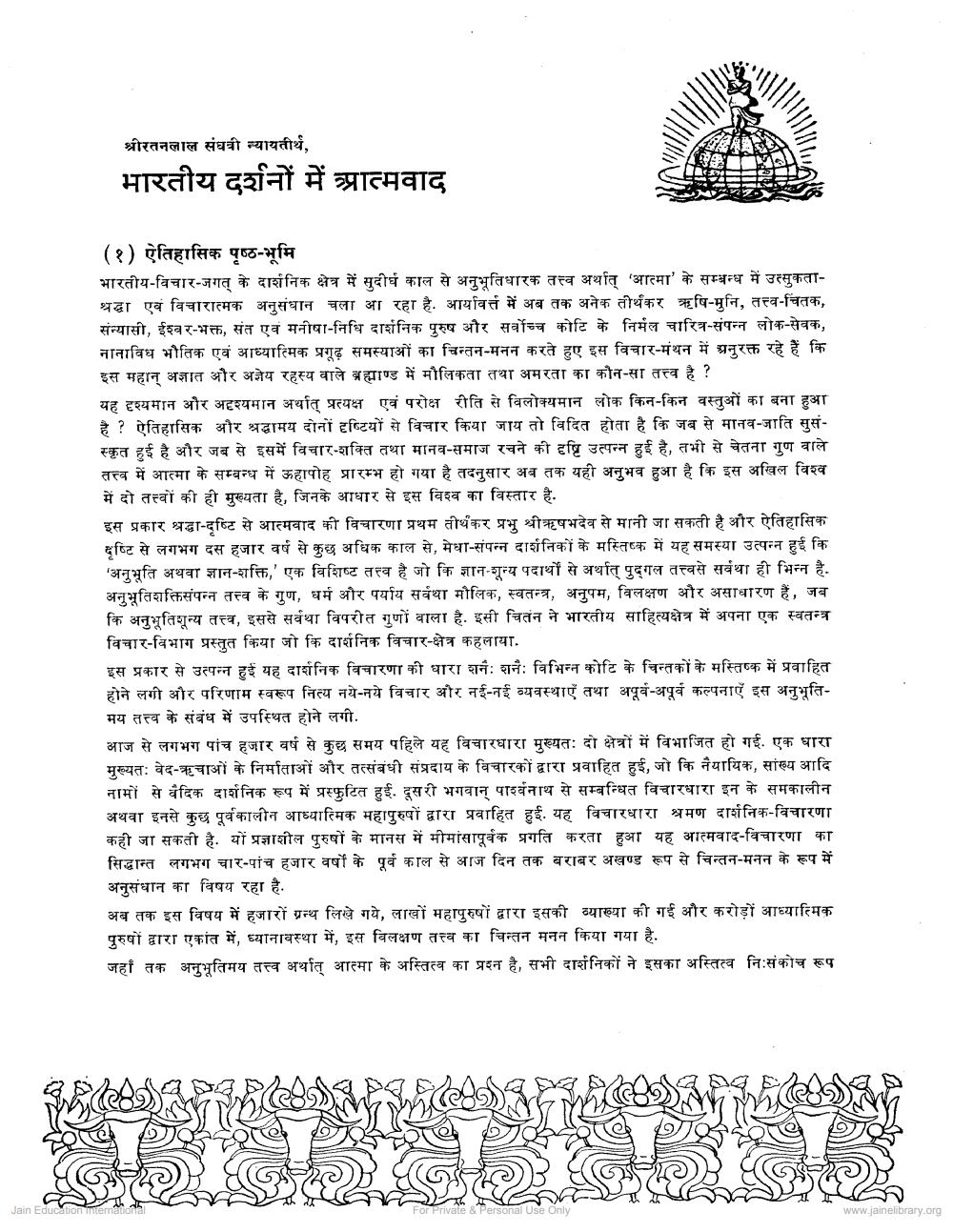Book Title: Bharatiya Darshano me Atmavad Author(s): Ratanlal Sanghvi Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 1
________________ श्रीरतनलाल संघवी न्यायतीर्थ, भारतीय दर्शनों में आत्मवाद Vim (१) ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि भारतीय-विचार-जगत् के दार्शनिक क्षेत्र में सुदीर्घ काल से अनुभूतिधारक तत्त्व अर्थात् 'आत्मा' के सम्बन्ध में उत्सुकताश्रद्धा एवं विचारात्मक अनुसंधान चला आ रहा है. आर्यावर्त में अब तक अनेक तीर्थंकर ऋषि-मुनि, तत्त्व-चिंतक, संन्यासी, ईश्वर-भक्त, संत एवं मनीषा-निधि दार्शनिक पुरुष और सर्वोच्च कोटि के निर्मल चारित्र-संपन्न लोक-सेवक, नानाविध भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगूढ़ समस्याओं का चिन्तन-मनन करते हुए इस विचार-मंथन में अनुरक्त रहे हैं कि इस महान् अज्ञात और अज्ञेय रहस्य वाले ब्रह्माण्ड में मौलिकता तथा अमरता का कौन-सा तत्त्व है ? यह दृश्यमान और अदृश्यमान अर्थात् प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रीति से विलोक्यमान लोक किन-किन वस्तुओं का बना हुआ है ? ऐतिहासिक और श्रद्धामय दोनों दृष्टियों से विचार किया जाय तो विदित होता है कि जब से मानव-जाति सुसंस्कृत हुई है और जब से इसमें विचार-शक्ति तथा मानव-समाज रचने की दृष्टि उत्पन्न हुई है, तभी से चेतना गुण वाले तत्त्व में आत्मा के सम्बन्ध में ऊहापोह प्रारम्भ हो गया है तदनुसार अब तक यही अनुभव हुआ है कि इस अखिल विश्व में दो तत्त्वों की ही मुख्यता है, जिनके आधार से इस विश्व का विस्तार है. इस प्रकार श्रद्धा-दृष्टि से आत्मवाद की विचारणा प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्रीऋषभदेव से मानी जा सकती है और ऐतिहासिक दृष्टि से लगभग दस हजार वर्ष से कुछ अधिक काल से, मेधा-संपन्न दार्शनिकों के मस्तिष्क में यह समस्या उत्पन्न हुई कि 'अनुभूति अथवा ज्ञान-शक्ति,' एक विशिष्ट तत्त्व है जो कि ज्ञान-शून्य पदार्थों से अर्थात् पुद्गल तत्त्वसे सर्वथा ही भिन्न है. अनुभूतिशक्तिसंपन्न तत्त्व के गुण, धर्म और पर्याय सर्वथा मौलिक, स्वतन्त्र, अनुपम, विलक्षण और असाधारण हैं, जब कि अनुभूतिशून्य तत्त्व, इससे सर्वथा विपरीत गुणों वाला है. इसी चितन ने भारतीय साहित्यक्षेत्र में अपना एक स्वतन्त्र विचार-विभाग प्रस्तुत किया जो कि दार्शनिक विचार-क्षेत्र कहलाया. इस प्रकार से उत्पन्न हुई यह दार्शनिक विचारणा की धारा शनैः शनैः विभिन्न कोटि के चिन्तकों के मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगी और परिणाम स्वरूप नित्य नये-नये विचार और नई-नई व्यवस्थाएँ तथा अपूर्व-अपूर्व कल्पनाएँ इस अनुभूतिमय तत्त्व के संबंध में उपस्थित होने लगी.. आज से लगभग पांच हजार वर्ष से कुछ समय पहिले यह विचारधारा मुख्यतः दो क्षेत्रों में विभाजित हो गई. एक धारा मुख्यतः वेद-ऋचाओं के निर्माताओं और तत्संबंधी संप्रदाय के विचारकों द्वारा प्रवाहित हुई, जो कि नैयायिक, सांख्य आदि नामों से वैदिक दार्शनिक रूप में प्रस्फुटित हुई. दूसरी भगवान् पाश्र्वनाथ से सम्बन्धित विचारधारा इन के समकालीन अथवा इनसे कुछ पूर्वकालीन आध्यात्मिक महापुरुषों द्वारा प्रवाहित हुई. यह विचारधारा श्रमण दार्शनिक-विचारणा कही जा सकती है. यों प्रज्ञाशील पुरुषों के मानस में मीमांसापूर्वक प्रगति करता हुआ यह आत्मवाद-विचारणा का सिद्धान्त लगभग चार-पांच हजार वर्षों के पूर्व काल से आज दिन तक बराबर अखण्ड रूप से चिन्तन-मनन के रूप में अनुसंधान का विषय रहा है. अब तक इस विषय में हजारों ग्रन्थ लिखे गये, लाखों महापुरुषों द्वारा इसकी व्याख्या की गई और करोड़ों आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा एकांत में, ध्यानावस्था में, इस विलक्षण तत्त्व का चिन्तन मनन किया गया है.. जहाँ तक अनुभूतिमय तत्त्व अर्थात् आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न है, सभी दार्शनिकों ने इसका अस्तित्व निःसंकोच रूप Jain Education Tremato For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3