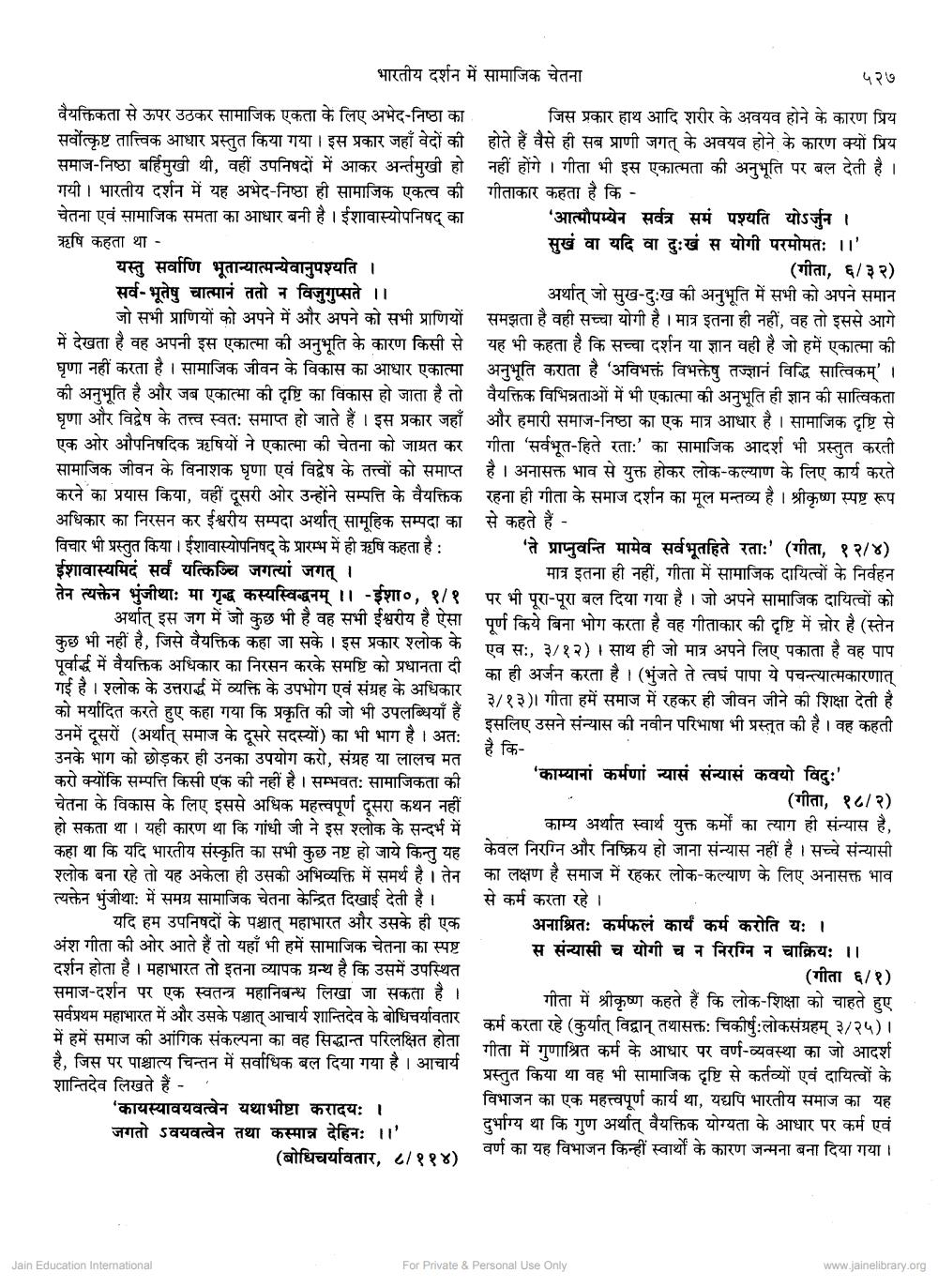Book Title: Bharatiya Darshan me Samajik Chetna Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 2
________________ भारतीय दर्शन में सामाजिक चेतना वैयक्तिकता से ऊपर उठकर सामाजिक एकता के लिए अभेद-निष्ठा का सर्वोत्कृष्ट तात्विक आधार प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार जहाँ वेदों की समाज-निष्ठा बर्हिमुखी थी, वहीं उपनिषदों में आकर अर्न्तमुखी हो गयी। भारतीय दर्शन में यह अभेद-निष्ठा ही सामाजिक एकत्व की चेतना एवं सामाजिक समता का आधार बनी है। ईशावास्योपनिषद् का ऋषि कहता था यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।। जो सभी प्राणियों को अपने में और अपने को सभी प्राणियों में देखता है वह अपनी इस एकात्मा की अनुभूति के कारण किसी से घृणा नहीं करता है । सामाजिक जीवन के विकास का आधार एकात्मा की अनुभूति है और जब एकात्मा की दृष्टि का विकास हो जाता है तो घृणा और विद्वेष के तत्त्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जहाँ एक ओर औपनिषदिक ऋषियों ने एकात्मा की चेतना को जाग्रत कर सामाजिक जीवन के विनाशक घृणा एवं विद्वेष के तत्त्वों को समाप्त करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार का निरसन कर ईश्वरीय सम्पदा अर्थात् सामूहिक सम्पदा का विचार भी प्रस्तुत किया। ईशावास्योपनिषद् के प्रारम्भ में ही ऋषि कहता है : ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चि जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृद्ध कस्यस्विद्धनम् ।। - ईशा०, १/१ अर्थात् इस जग में जो कुछ भी है वह सभी ईश्वरीय है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे वैयक्तिक कहा जा सके । इस प्रकार श्लोक के पूर्वार्द्ध में वैयक्तिक अधिकार का निरसन करके समष्टि को प्रधानता दी गई है। श्लोक के उत्तरार्द्ध में व्यक्ति के उपभोग एवं संग्रह के अधिकार को मर्यादित करते हुए कहा गया कि प्रकृति की जो भी उपलब्धियाँ हैं उनमें दूसरों (अर्थात् समाज के दूसरे सदस्यों) का भी भाग है। अतः उनके भाग को छोड़कर ही उनका उपयोग करो, संग्रह या लालच मत करो क्योंकि सम्पत्ति किसी एक की नहीं है। सम्भवतः सामाजिकता की चेतना के विकास के लिए इससे अधिक महत्त्वपूर्ण दूसरा कथन नहीं हो सकता था । यही कारण था कि गांधी जी ने इस श्लोक के सन्दर्भ में कहा था कि यदि भारतीय संस्कृति का सभी कुछ नष्ट हो जाये किन्तु यह श्लोक बना रहे तो यह अकेला ही उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ है । तेन त्यक्तेन भुंजीथा: में समग्र सामाजिक चेतना केन्द्रित दिखाई देती है। यदि हम उपनिषदों के पश्चात् महाभारत और उसके ही एक अंश गीता की ओर आते हैं तो यहाँ भी हमें सामाजिक चेतना का स्पष्ट दर्शन होता है। महाभारत तो इतना व्यापक ग्रन्थ है कि उसमें उपस्थित समाज - दर्शन पर एक स्वतन्त्र महानिबन्ध लिखा जा सकता है । सर्वप्रथम महाभारत में और उसके पश्चात् आचार्य शान्तिदेव के बोधिचर्यावतार में हमें समाज की आंगिक संकल्पना का वह सिद्धान्त परिलक्षित होता है, जिस पर पाश्चात्य चिन्तन में सर्वाधिक बल दिया गया है। आचार्य शान्तिदेव लिखते हैं 'कायस्यावयवत्वेन यथाभीष्टा करादयः । जगतो ऽवयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः ।।' (बोधिचर्यावतार, ८ / ११४) Jain Education International ५२७ जिस प्रकार हाथ आदि शरीर के अवयव होने के कारण प्रिय होते हैं वैसे ही सब प्राणी जगत् के अवयव होने के कारण क्यों प्रिय नहीं होंगे। गीता भी इस एकात्मता की अनुभूति पर बल देती है। गीताकार कहता है कि 'आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः ।।' (गीता, ६ / ३२) अर्थात् जो सुख-दुःख की अनुभूति में सभी को अपने समान समझता है वही सच्चा योगी है। मात्र इतना ही नहीं, वह तो इससे आगे यह भी कहता है कि सच्चा दर्शन या ज्ञान वही है जो हमें एकात्मा की अनुभूति कराता है 'अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्' । वैयक्तिक विभिन्नताओं में भी एकात्मा की अनुभूति ही ज्ञान की सात्विकता और हमारी समाज-निष्ठा का एक मात्र आधार है। सामाजिक दृष्टि से गीता 'सर्वभूतहिते रताः' का सामाजिक आदर्श भी प्रस्तुत करती है। अनासक्त भाव से युक्त होकर लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहना ही गीता के समाज दर्शन का मूल मन्तव्य है । श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं - - 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ' ( गीता, १२ / ४) मात्र इतना ही नहीं, गीता में सामाजिक दायित्वों के निर्वहन पर भी पूरा-पूरा बल दिया गया है जो अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण किये बिना भोग करता है वह गीताकार की दृष्टि में चोर है (स्तेन एव सः, ३/१२)। साथ ही जो मात्र अपने लिए पकाता है वह पाप काही अर्जन करता है । (भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् इसलिए उसने संन्यास की नवीन परिभाषा भी प्रस्तुत की है। वह कहती ३/१३)। गीता हमें समाज में रहकर ही जीवन जीने की शिक्षा देती हैं है कि 'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः (गीता, १८/२) काम्य अर्थात स्वार्थ युक्त कर्मों का त्याग ही संन्यास है, केवल निरग्नि और निष्क्रिय हो जाना संन्यास नहीं है । सच्चे संन्यासी का लक्षण है समाज में रहकर लोक-कल्याण के लिए अनासक्त भाव से कर्म करता रहे। अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः ।। (गीता ६/१) गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि लोक शिक्षा को चाहते हुए कर्म करता रहे (कुर्यात् विद्वान् तयासक्तः चिकीर्षुः लोकसंग्रहम् ३ / २५) । गीता में गुणाश्रित कर्म के आधार पर वर्ण-व्यवस्था का जो आदर्श प्रस्तुत किया था वह भी सामाजिक दृष्टि से कर्तव्यों एवं दायित्वों के विभाजन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य था, यद्यपि भारतीय समाज का यह दुर्भाग्य था कि गुण अर्थात् वैयक्तिक योग्यता के आधार पर कर्म एवं वर्ण का यह विभाजन किन्हीं स्वार्थों के कारण जन्मना बना दिया गया। For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3