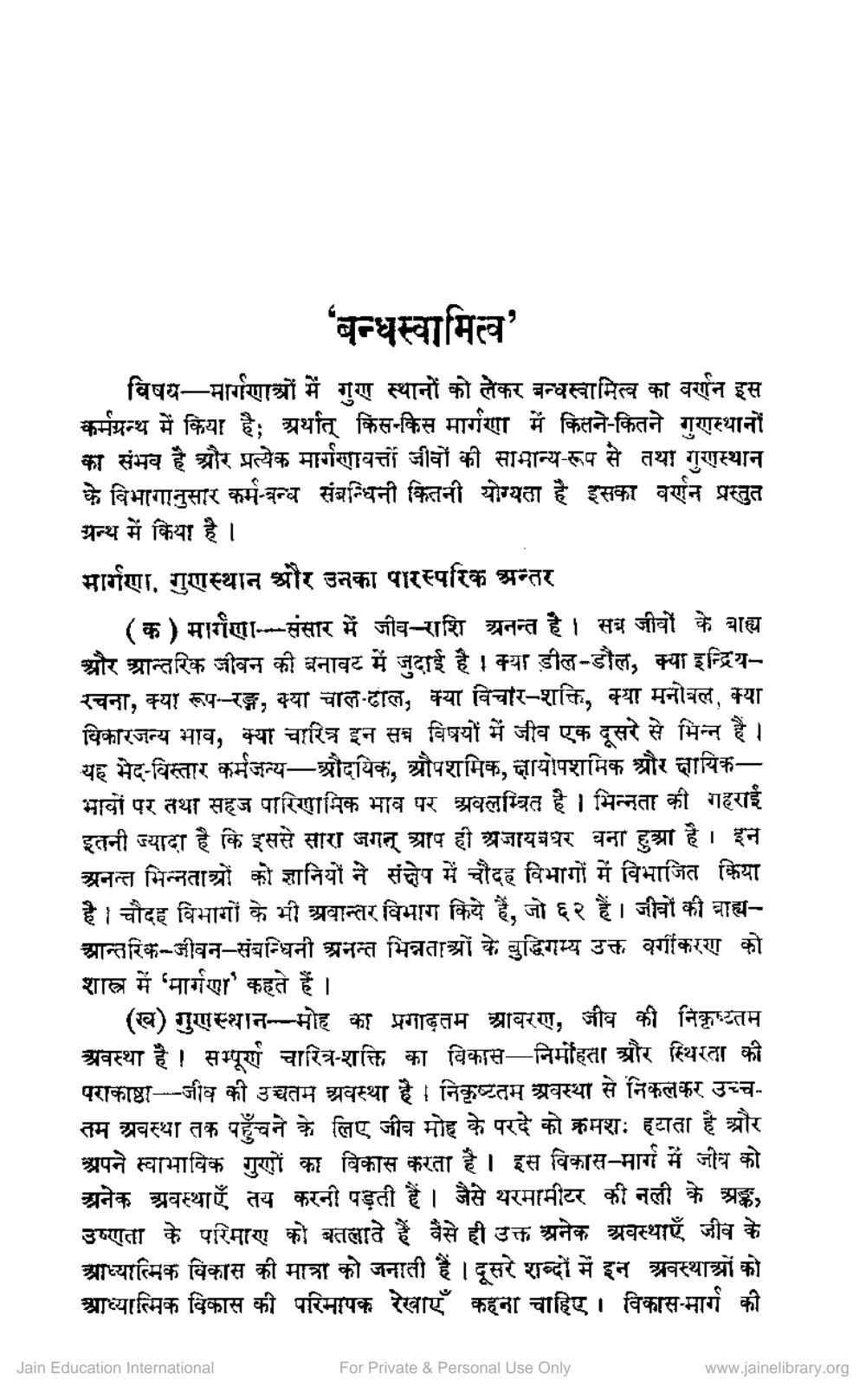Book Title: Bandhswamitva Author(s): Sukhlal Sanghavi Publisher: Z_Darshan_aur_Chintan_Part_1_2_002661.pdf View full book textPage 1
________________ 'बन्धस्वामित्व' विषय-मार्गणाओं में गुण स्थानों को लेकर बन्धस्वामित्व का वर्णन इस कर्मग्रन्थ में किया है। अर्थात् किस-किस मार्गणा में कितने-कितने गणस्थानों का संभव है और प्रत्येक मार्गणावत्तों जीवों की सामान्य रूप से तथा गुणस्थान के विभागानुसार कर्म-बन्ध संबन्धिनी कितनी योग्यता है इसका वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ में किया है। मार्गणा, गुणस्थान और उनका पारस्परिक अन्तर (क) मार्गणा-~-संसार में जीव-राशि अनन्त है। सब जीवों के बाह्य और अान्तरिक जीवन की बनावट में जुदाई है । क्या डील-डौल, क्या इन्द्रियरचना, क्या रूप-रङ्ग, क्या चाल-ढाल, क्या विचार-शक्ति, क्या मनोबल, क्या विकारजन्य भाव, क्या चारित्र इन सब विषयों में जीव एक दूसरे से भिन्न हैं। यह भेद-विस्तार कर्मजन्य-औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिकभावों पर तथा सहज पारिणामिक भाव पर अक्लम्बित है । भिन्नता की गहराई इतनी ज्यादा है कि इससे सारा जगत् श्राप ही अजायबघर बना हुआ है। इन अनन्त भिन्नतात्रों को ज्ञानियों ने संक्षेप में चौदह विभागों में विभाजित किया है। चौदह विभागों के भी अवान्तर विभाग किये हैं, जो ६२ हैं। जीवों की बाह्यआन्तरिक-जीवन-संबन्धिनी अनन्त भिन्नताओं के बुद्धिगम्य उक्त वर्गीकरण को शास्त्र में 'मार्गणा' कहते हैं । (ख) गुणस्थान-मोह का प्रगाढ़तम आवरण, जीव की निकृष्टतम अवस्था है। सम्पूर्ण चारित्र-शक्ति का विकास निर्मोहता और स्थिरता की पराकाष्ठा-----जीव की उच्चतम अवस्था है। निकृष्टतम अवस्था से निकलकर उच्चतम अवस्था तक पहुँचने के लिए जीव मोह के परदे को क्रमशः हटाता है और अपने स्वाभाविक गुणों का विकास करता है । इस विकास-मार्ग में जीव को अनेक अवस्थाएँ तय करनी पड़ती हैं। जैसे थरमामीटर की नली के अङ्क, उष्णता के परिमाण को बतलाते हैं वैसे ही उक्त अनेक अवस्थाएँ जीव के आध्यात्मिक विकास की मात्रा को जनाती हैं । दूसरे शब्दों में इन अवस्थाओं को श्राध्यात्मिक विकास की परिमापक रेखाएँ कहना चाहिए । विकास-मार्ग की Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5