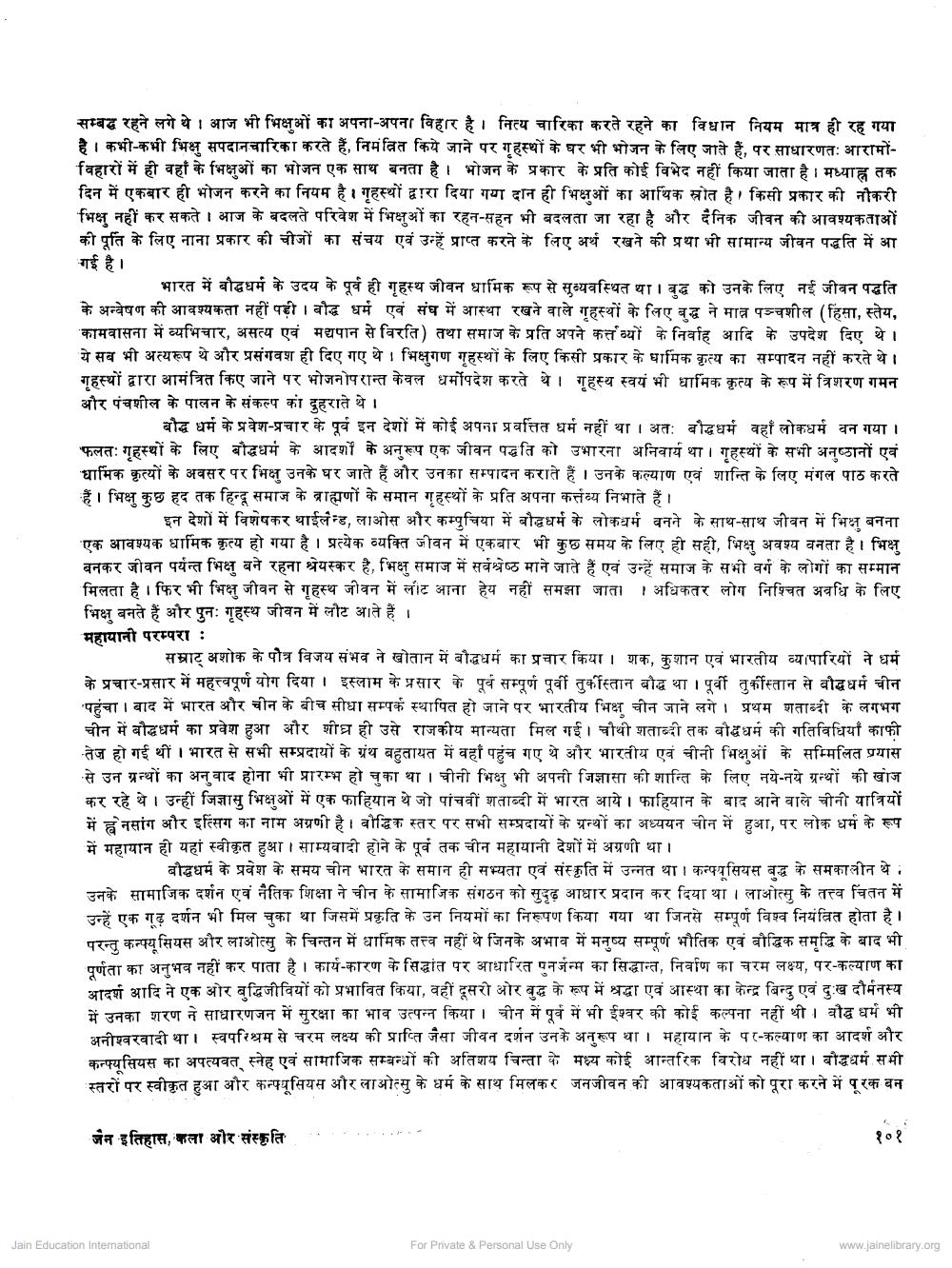Book Title: Ashiyai Sraman Parampara Ek Vihangam Drushti Author(s): Chandrashekhar Prasad Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 5
________________ सम्बद्ध रहने लगे थे। आज भी भिक्षुओं का अपना-अपना विहार है। नित्य चारिका करते रहने का विधान नियम मात्र ही रह गया है। कभी-कभी भिक्षु सपदानचारिका करते हैं, निमंत्रित किये जाने पर गृहस्थों के घर भी भोजन के लिए जाते हैं, पर साधारणतः आरामोंविहारों में ही वहाँ के भिक्षुओं का भोजन एक साथ बनता है। भोजन के प्रकार के प्रति कोई विभेद नहीं किया जाता है। मध्याह्न तक दिन में एकबार ही भोजन करने का नियम है। गृहस्थों द्वारा दिया गया दान ही भिक्षुओं का आर्थिक स्रोत है। किसी प्रकार की नौकरी भिक्ष नहीं कर सकते। आज के बदलते परिवेश में भिक्षुओं का रहन-सहन भी बदलता जा रहा है और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की चीजों का संचय एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए अर्थ रखने की प्रथा भी सामान्य जीवन पद्धति में आ गई है। भारत में बौद्धधर्म के उदय के पूर्व ही गृहस्थ जीवन धार्मिक रूप से सुव्यवस्थित था। बुद्ध को उनके लिए नई जीवन पद्धति के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं पड़ी । बौद्ध धर्म एवं संघ में आस्था रखने वाले गृहस्थों के लिए बुद्ध ने मान पञ्चशील (हिसा, स्तेय, कामवासना में व्यभिचार, असत्य एवं मद्यपान से विरति) तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह आदि के उपदेश दिए थे। ये सब भी अत्यरूप थे और प्रसंगवश ही दिए गए थे। भिक्षुगण गृहस्थों के लिए किसी प्रकार के धार्मिक कृत्य का सम्पादन नहीं करते थे। गहस्थों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भोजनोपरान्त केवल धर्मोपदेश करते थे। गृहस्थ स्वयं भी धार्मिक कृत्य के रूप में त्रिशरण गमन और पंचशील के पालन के संकल्प को दुहराते थे । बौद्ध धर्म के प्रवेश-प्रचार के पूर्व इन देशों में कोई अपना प्रवत्तित धर्म नहीं था । अत: बौद्धधर्म वहाँ लोकधर्म बन गया। फलतः गृहस्थों के लिए बौद्धधर्म के आदर्शों के अनुरूप एक जीवन पद्धति को उभारना अनिवार्य था। गृहस्थों के सभी अनुष्ठानों एवं धार्मिक कृत्यों के अवसर पर भिक्षु उनके घर जाते हैं और उनका सम्पादन कराते हैं । उनके कल्याण एवं शान्ति के लिए मंगल पाठ करते हैं । भिक्षु कुछ हद तक हिन्दू समाज के ब्राह्मणों के समान गृहस्थों के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाते हैं। इन देशों में विशेषकर थाईलन्ड, लाओस और कम्पुचिया में बौद्धधर्म के लोकधर्म बनने के साथ-साथ जीवन में भिक्षु बनना एक आवश्यक धार्मिक कृत्य हो गया है । प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एकबार भी कुछ समय के लिए ही सही, भिक्षु अवश्य बनता है। भिक्षु बनकर जीवन पर्यन्त भिक्षु बने रहना श्रेयस्कर है, भिक्षु समाज में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं एवं उन्हें समाज के सभी वर्ग के लोगों का सम्मान मिलता है । फिर भी भिक्षु जीवन से गृहस्थ जीवन में लौट आना हेय नहीं समझा जाता । अधिकतर लोग निश्चित अवधि के लिए भिक्षु बनते हैं और पुनः गृहस्थ जीवन में लौट आते हैं । महायानी परम्परा : सम्राट अशोक के पौत्र विजय संभव ने खोतान में बौद्धधर्म का प्रचार किया। शक, कुशान एवं भारतीय व्यापारियों ने धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योग दिया। इस्लाम के प्रसार के पूर्व सम्पूर्ण पूर्वी तुर्कीस्तान बौद्ध था । पूर्वी तुर्कीस्तान से बौद्ध धर्म चीन 'पहंचा । बाद में भारत और चीन के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाने पर भारतीय भिक्ष चीन जाने लगे। प्रथम शताब्दी के लगभग चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ और शीघ्र ही उसे राजकीय मान्यता मिल गई। चौथी शताब्दी तक बौद्धधर्म की गतिविधियाँ काफी तेज हो गई थीं। भारत से सभी सम्प्रदायों के ग्रंथ बहुतायत में वहाँ पहुंच गए थे और भारतीय एवं चीनी भिक्षुओं के सम्मिलित प्रयास से उन ग्रन्थों का अनुवाद होना भी प्रारम्भ हो चुका था। चीनी भिक्षु भी अपनी जिज्ञासा की शान्ति के लिए नये-नये ग्रन्थों की खोज कर रहे थे। उन्हीं जिज्ञासु भिक्षुओं में एक फाहियान थे जो पांचवीं शताब्दी में भारत आये। फाहियान के बाद आने वाले चीनी यात्रियों में हनसांग और इत्सिग का नाम अग्रणी है। बौद्धिक स्तर पर सभी सम्प्रदायों के ग्रन्थों का अध्ययन चीन में हुआ, पर लोक धर्म के रूप में महायान ही यहां स्वीकृत हुआ। साम्यवादी होने के पूर्व तक चीन महायानी देशों में अग्रणी था। बौद्धधर्म के प्रवेश के समय चीन भारत के समान ही सभ्यता एवं संस्कृति में उन्नत था। कन्फ्युसियस बुद्ध के समकालीन थे । उनके सामाजिक दर्शन एवं नैतिक शिक्षा ने चीन के सामाजिक संगठन को सुदृढ़ आधार प्रदान कर दिया था । लाओत्सु के तत्त्व चिंतन में उन्हें एक गढ़ दर्शन भी मिल चुका था जिसमें प्रकृति के उन नियमों का निरूपण किया गया था जिनसे सम्पूर्ण विश्व नियंत्रित होता है। परन्तु कन्फ्युसियस और लाओत्सु के चिन्तन में धार्मिक तत्त्व नहीं थे जिनके अभाव में मनुष्य सम्पूर्ण भौतिक एवं बौद्धिक समृद्धि के बाद भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता है। कार्य-कारण के सिद्धांत पर आधारित पुनर्जन्म का सिद्धान्त, निर्वाण का चरम लक्ष्य, पर-कल्याण का आदर्श आदि ने एक ओर बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर बुद्ध के रूप में श्रद्धा एवं आस्था का केन्द्र बिन्दु एवं दुःख दौर्मनस्य में उनका शरण ने साधारणजन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया। चीन में पूर्व में भी ईश्वर की कोई कल्पना नहीं थी। बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी था। स्वपरिश्रम से चरम लक्ष्य की प्राप्ति जैसा जीवन दर्शन उनके अनुरूप था। महायान के पर-कल्याण का आदर्श और कन्फ्यसियस का अपत्यवत स्नेह एवं सामाजिक सम्बन्धों की अतिशय चिन्ता के मध्य कोई आन्तरिक विरोध नहीं था। बौद्धधर्म सभी स्तरों पर स्वीकृत हुआ और कन्फ्यूसियस और लाओत्सु के धर्म के साथ मिलकर जनजीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरक बन जैन इतिहास, कला और संस्कृतिः......... - Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8