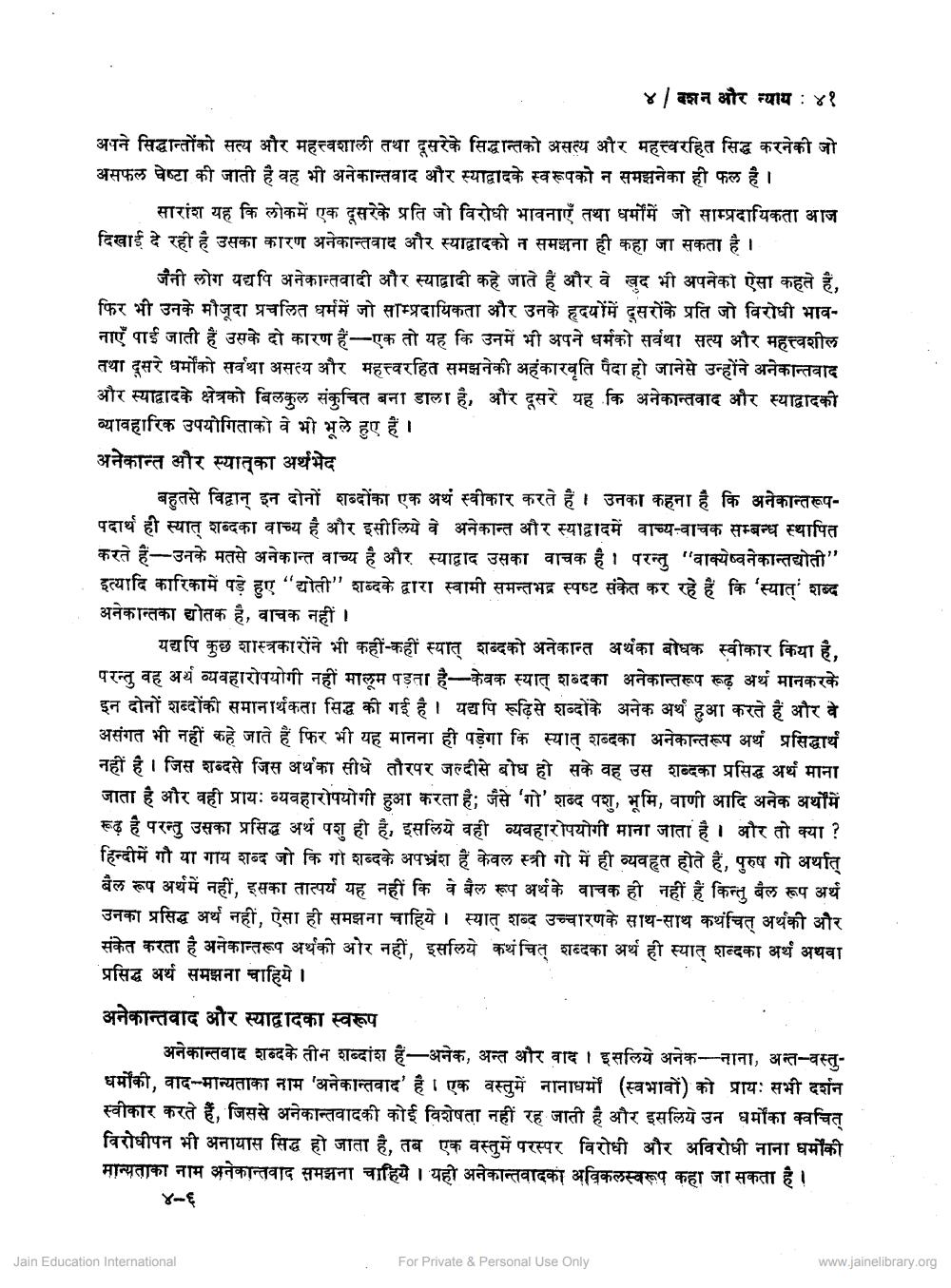Book Title: Anekantvad aur Syadwad Author(s): Bansidhar Pandit Publisher: Z_Bansidhar_Pandit_Abhinandan_Granth_012047.pdf View full book textPage 2
________________ ४ / बशन और न्याय ४१ अपने सिद्धान्तोंको सत्य और महत्त्वशाली तथा दूसरेके सिद्धान्तको असत्य और महत्त्वरहित सिद्ध करनेकी जो असफल चेष्टा की जाती है वह भी अनेकान्तवाद और स्याद्वादके स्वरूपको न समझनेका ही फल है । सारांश यह कि लोक में एक दूसरेके प्रति जो विरोधी भावनाएँ तथा धर्मोंमें जो साम्प्रदायिकता आज दिखाई दे रही है उसका कारण अनेकान्तवाद और स्याद्वादको न समझना ही कहा जा सकता है । जैनी लोग यद्यपि अनेकान्तवादी और स्याद्वादी कहे जाते हैं और वे खुद भी अपनेको ऐसा कहते हैं, फिर भी उनके मौजूदा प्रचलित धर्म में जो साम्प्रदायिकता और उनके हृदयोंमें दूसरोंके प्रति जो विरोधी भावनाएँ पाई जाती हैं उसके दो कारण हैं - एक तो यह कि उनमें भी अपने धर्मको सर्वथा सत्य और महत्त्वशील तथा दूसरे धर्मोको सर्वथा असत्य और महत्त्वरहित समझने की अहंकारवृति पैदा हो जानेसे उन्होंने अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के क्षेत्रको बिलकुल संकुचित बना डाला है, और दूसरे यह कि अनेकान्तवाद और स्याद्वादकी व्यावहारिक उपयोगिताको वे भी भूले हुए हैं । अनेकान्त और स्यात्का अर्थभेद बहुतसे विद्वान् इन दोनों शब्दोंका एक अथं स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि अनेकान्तरूपपदार्थ ही स्यात् शब्दका वाच्य है और इसीलिये वे अनेकान्त और स्याद्वादमें वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित करते हैं - उनके मतसे अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद उसका वाचक है । परन्तु " वाक्ये ष्व नेकान्तद्योती" इत्यादि कारिका में पड़े हुए " द्योती" शब्दके द्वारा स्वामी समन्तभद्र स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि 'स्यात्' शब्द अनेकान्तका द्योतक है, वाचक नहीं । यद्यपि कुछ शास्त्रकारोंने भी कहीं-कहीं स्यात् शब्दको अनेकान्त अर्थका बोधक स्वीकार किया है, अनेकान्तरूप रूढ़ अर्थ मानकरके अनेक अर्थ हुआ करते हैं और वे अनेकान्तरूप अर्थं प्रसिद्धार्थं शब्दका प्रसिद्ध अर्थं माना परन्तु वह अर्थ व्यवहारोपयोगी नहीं मालूम पड़ता है— केवक स्यात् शब्दका इन दोनों शब्दोंकी समानार्थकता सिद्ध की गई है । यद्यपि रूढ़ि से शब्दोंके असंगत भी नहीं कहे जाते हैं फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि स्यात् शब्दका नहीं है । जिस शब्दसे जिस अर्थका सीधे तौरपर जल्दीसे बोध हो सके वह उस जाता है और वही प्रायः व्यवहारोपयोगी हुआ करता है; जैसे 'गो' शब्द पशु, भूमि, वाणी आदि अनेक अर्थों में रूढ़ है परन्तु उसका प्रसिद्ध अर्थ पशु ही है, इसलिये वही व्यवहारोपयोगी माना जाता है । और तो क्या ? हिन्दी में गौ या गाय शब्द जो कि गो शब्दके अपभ्रंश हैं केवल स्त्री गो में ही व्यवहृत होते हैं, पुरुष गो अर्थात् बैल रूप अर्थ में नहीं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे बैल रूप अर्थ के वाचक ही नहीं हैं किन्तु बैल रूप अर्थ उनका प्रसिद्ध अर्थ नहीं, ऐसा ही समझना चाहिये । स्यात् शब्द उच्चारणके साथ-साथ कथंचित् अर्थकी और संकेत करता है अनेकान्तरूप अर्थकी ओर नहीं, इसलिये कथंचित् शब्दका अर्थ ही स्यात् शब्दका अर्थ अथवा प्रसिद्ध अर्थ समझना चाहिये । अनेकान्तवाद और स्याद्वादका स्वरूप अनेकान्तवाद शब्द के तीन शब्दांश हैं - अनेक, अन्त और वाद । इसलिये अनेक - नाना, अन्त-वस्तुधर्मोकी, वाद-मान्यताका नाम 'अनेकान्तवाद' है । एक वस्तुमें नानाधर्मों (स्वभावों) को प्रायः सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, जिससे अनेकान्तवादकी कोई विशेषता नहीं रह जाती है और इसलिये उन धर्मोका क्वचित् विरोधीपन भी अनायास सिद्ध हो जाता है, तब एक वस्तुमें परस्पर विरोधी और अविरोधी नाना धर्मोकी मान्यताका नाम अनेकान्तवाद समझना चाहिये । यही अनेकान्तवादका अविकलस्वरूप कहा जा सकता है । ४-६ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4