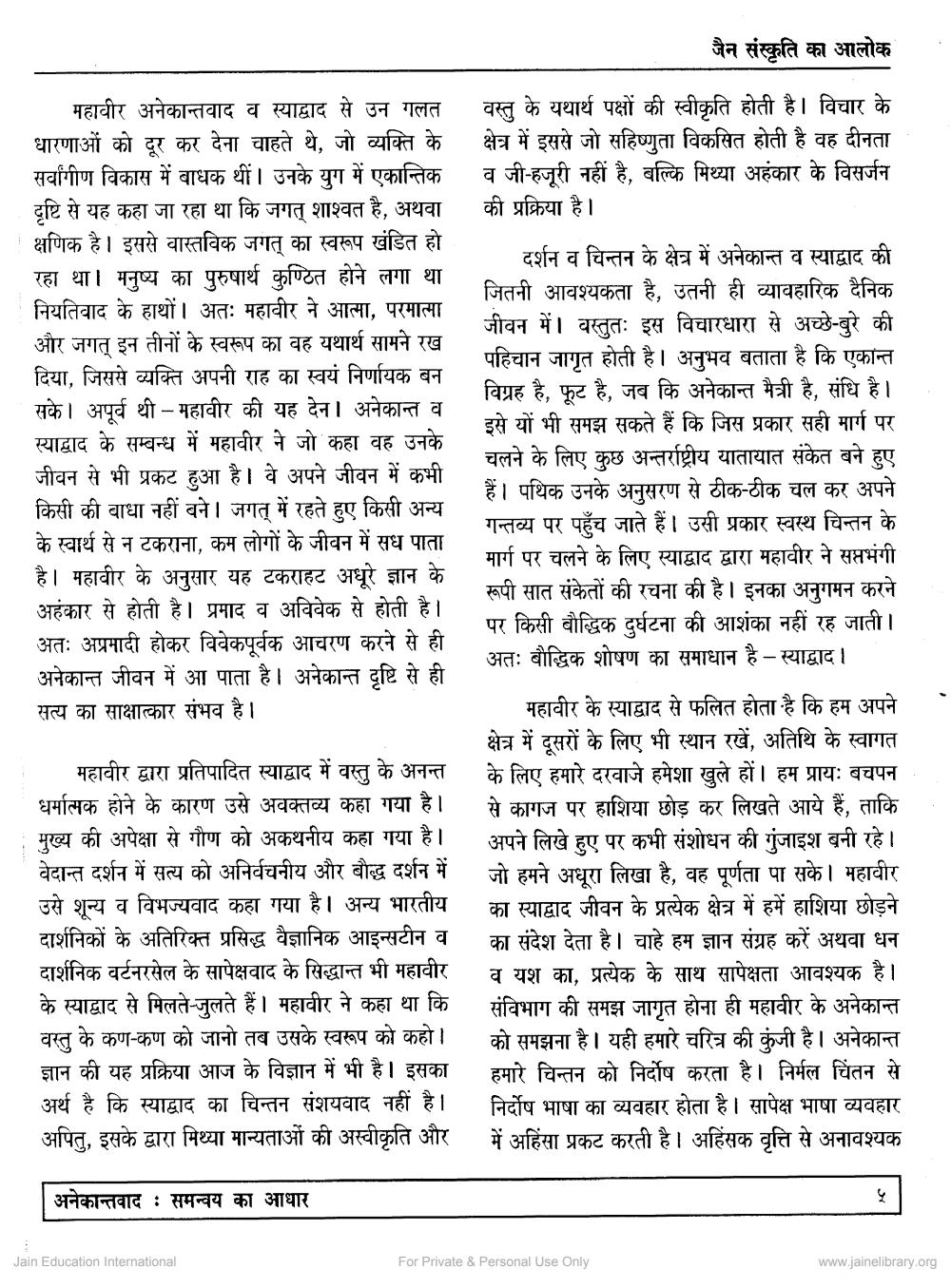Book Title: Anekant Samanvay ka Adhar Author(s): Prem Suman Jain Publisher: Z_Sumanmuni_Padmamaharshi_Granth_012027.pdf View full book textPage 5
________________ महावीर अनेकान्तवाद व स्याद्वाद से उन गलत धारणाओं को दूर कर देना चाहते थे, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक थीं । उनके युग में एकान्तिक दृष्टि से यह कहा जा रहा था कि जगत् शाश्वत है, अथवा क्षणिक है। इससे वास्तविक जगत् का स्वरूप खंडित हो रहा था। मनुष्य का पुरुषार्थ कुण्ठित होने लगा था नियतिवाद के हाथों । अतः महावीर ने आत्मा, परमात्मा और जगत् इन तीनों के स्वरूप का वह यथार्थ सामने रख दिया, जिससे व्यक्ति अपनी राह का स्वयं निर्णायक बन सके। अपूर्व थी - महावीर की यह देन । अनेकान्त व स्याद्वाद के सम्बन्ध में महावीर ने जो कहा वह उनके जीवन से भी प्रकट हुआ है। वे अपने जीवन में कभी किसी की बाधा नहीं बने। जगत् में रहते हुए किसी अन्य के स्वार्थ से न टकराना, कम लोगों के जीवन में सध पाता है। महावीर के अनुसार यह टकराहट अधूरे ज्ञान के अहंकार से होती है । प्रमाद व अविवेक से होती है। अतः अप्रमादी होकर विवेकपूर्वक आचरण करने ही अनेकान्त जीवन में आ पाता है । अनेकान्त दृष्टि सत्य का साक्षात्कार संभव है । ही महावीर द्वारा प्रतिपादित स्याद्वाद में वस्तु के अनन्त धर्मात्मक होने के कारण उसे अवक्तव्य कहा गया है। मुख्य की अपेक्षा से गौण को अकथनीय कहा गया है । वेदान्त दर्शन में सत्य को अनिर्वचनीय और बौद्ध दर्शन में उसे शून्य व विभज्यवाद कहा गया है । अन्य भारतीय दार्शनिकों के अतिरिक्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्सटीन व दार्शनिक वर्टनरसेल के सापेक्षवाद के सिद्धान्त भी महावीर स्याद्वाद से मिलते-जुलते हैं । महावीर ने कहा था कि वस्तु के कण-कण को जानो तब उसके स्वरूप को कहो । ज्ञान की यह प्रक्रिया आज के विज्ञान में भी है । इसका अर्थ है कि स्याद्वाद का चिन्तन संशयवाद नहीं है । अपितु, इसके द्वारा मिथ्या मान्यताओं की अस्वीकृति और अनेकान्तवाद : समन्वय का आधार Jain Education International जैन संस्कृति का आलोक वस्तु के यथार्थ पक्षों की स्वीकृति होती है । विचार के क्षेत्र में इससे जो सहिष्णुता विकसित होती है वह दीनता व जी - हजूरी नहीं है, बल्कि मिथ्या अहंकार के विसर्जन की प्रक्रिया है । दर्शन व चिन्तन के क्षेत्र में अनेकान्त व स्याद्वाद की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही व्यावहारिक दैनिक जीवन में । वस्तुतः इस विचारधारा से अच्छे-बुरे की पहिचान जागृत होती है। अनुभव बताता है कि एकान्त विग्रह है, फूट है, जब कि अनेकान्त मैत्री है, संधि है । इसे यों भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सही मार्ग पर चलने के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात संकेत बने हुए हैं । पथिक उनके अनुसरण से ठीक-ठीक चल कर अपने गन्तव्य पर पहुँच जाते हैं । उसी प्रकार स्वस्थ चिन्तन के मार्ग पर चलने के लिए स्याद्वाद द्वारा महावीर ने सप्तभंगी रूपी सात संकेतों की रचना की है। इनका अनुगमन करने पर किसी बौद्धिक दुर्घटना की आशंका नहीं रह जाती । अतः बौद्धिक शोषण का समाधान है - स्याद्वाद । महावीर के स्याद्वाद से फलित होता है कि हम अपने क्षेत्र में दूसरों के लिए भी स्थान रखें, अतिथि के स्वागत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हों । हम प्रायः बचपन से कागज पर हाशिया छोड़ कर लिखते आये हैं, ताकि अपने लिखे हुए पर कभी संशोधन की गुंजाइश बनी रहे । जो हमने अधूरा लिखा है, वह पूर्णता पा सके । महावीर का स्याद्वाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें हाशिया छोड़ने का संदेश देता है। चाहे हम ज्ञान संग्रह करें अथवा धन व यश का, प्रत्येक के साथ सापेक्षता आवश्यक है । संविभाग की समझ जागृत होना ही महावीर के अनेकान्त को समझना है । यही हमारे चरित्र की कुंजी है । अनेकान्त हमारे चिन्तन को निर्दोष करता है। निर्मल चिंतन से निर्दोष भाषा का व्यवहार होता है । सापेक्ष भाषा व्यवहार में अहिंसा प्रकट करती है । अहिंसक वृत्ति से अनावश्यक For Private & Personal Use Only ५ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6