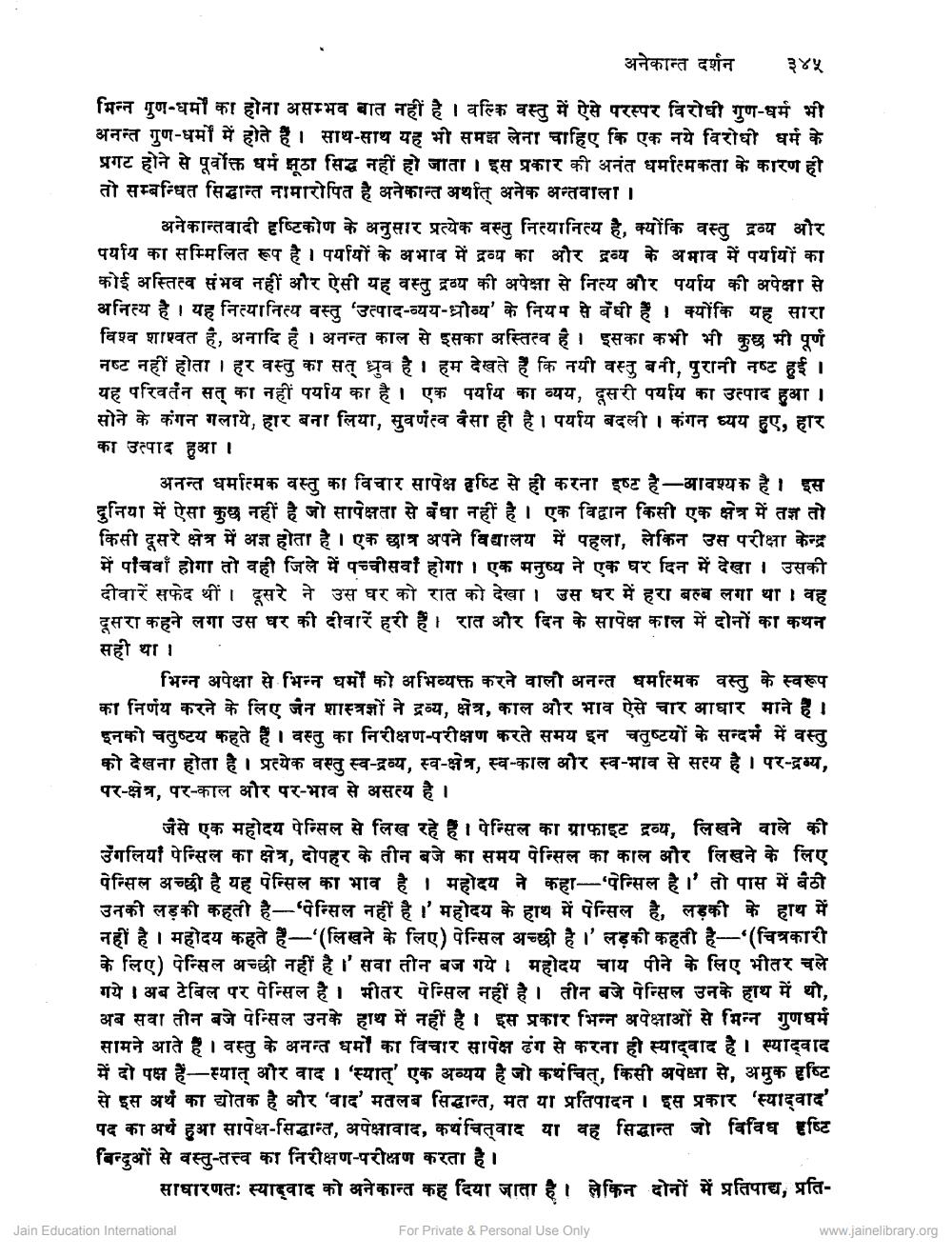Book Title: Anekant Darshan Author(s): U B Kothari Publisher: Z_Munidway_Abhinandan_Granth_012006.pdf View full book textPage 2
________________ अनेकान्त दर्शन ३४५ मिन्न गुण-धर्मों का होना असम्भव बात नहीं है। बल्कि वस्तु में ऐसे परस्पर विरोधी गुण-धर्म भी अनन्त गुण-धर्मों में होते हैं। साथ-साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि एक नये विरोधी धर्म के प्रगट होने से पूर्वोक्त धर्म झूठा सिद्ध नहीं हो जाता। इस प्रकार की अनंत धर्मात्मकता के कारण ही तो सम्बन्धित सिद्धान्त नामारोपित है अनेकान्त अर्थात् अनेक अन्तवाला। अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है, क्योंकि वस्तु द्रव्य और पर्याय का सम्मिलित रूप है। पर्यायों के अभाव में द्रव्य का और द्रव्य के अभाव में पर्यायों का कोई अस्तित्व संभव नहीं और ऐसी यह वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। यह नित्यानित्य वस्तु 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य' के नियम से बँधी हैं। क्योंकि यह सारा विश्व शाश्वत है, अनादि है । अनन्त काल से इसका अस्तित्व है। इसका कभी भी कुछ भी पूर्ण नष्ट नहीं होता । हर वस्तु का सत् ध्रुव है। हम देखते हैं कि नयी वस्तु बनी, पुरानी नष्ट हुई । यह परिवर्तन सत् का नहीं पर्याय का है। एक पर्याय का व्यय, दूसरी पर्याय का उत्पाद हुआ । सोने के कंगन गलाये, हार बना लिया, सुवर्णत्व वैसा ही है। पर्याय बदली । कंगन ध्यय हुए, हार का उत्पाद हुआ। अनन्त धर्मात्मक वस्तु का विचार सापेक्ष दृष्टि से ही करना इष्ट है-आवश्यक है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो सापेक्षता से बंधा नहीं है। एक विद्वान किसी एक क्षेत्र में तज्ञ तो किसी दूसरे क्षेत्र में अज्ञ होता है । एक छात्र अपने विद्यालय में पहला, लेकिन उस परीक्षा केन्द्र में पांचवाँ होगा तो वही जिले में पच्चीसवां होगा। एक मनुष्य ने एक घर दिन में देखा । उसकी दीवारें सफेद थीं। दूसरे ने उस घर को रात को देखा। उस घर में हरा बल्ब लगा था। वह दूसरा कहने लगा उस घर की दीवारें हरी हैं। रात और दिन के सापेक्ष काल में दोनों का कथन सही था। भिन्न अपेक्षा से भिन्न धर्मों को अभिव्यक्त करने वाली अनन्त धर्मात्मक वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए जैन शास्त्रज्ञों ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ऐसे चार आधार माने है। इनको चतुष्टय कहते हैं। वस्तु का निरीक्षण-परीक्षण करते समय इन चतुष्टयों के सन्दर्भ में वस्तु को देखना होता है। प्रत्येक वस्तु स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव से सत्य है। पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल और पर-भाव से असत्य है । जैसे एक महोदय पेन्सिल से लिख रहे हैं। पेन्सिल का ग्राफाइट द्रव्य, लिखने वाले की उँगलियां पेन्सिल का क्षेत्र, दोपहर के तीन बजे का समय पेन्सिल का काल और लिखने के लिए पेन्सिल अच्छी है यह पेन्सिल का भाव है । महोदय ने कहा-'पेन्सिल है।' तो पास में बैठी उनकी लड़की कहती है-'पेन्सिल नहीं है।' महोदय के हाथ में पेन्सिल है, लड़की के हाथ में नहीं है। महोदय कहते हैं-(लिखने के लिए) पेन्सिल अच्छी है।' लड़की कहती है-'(चित्रकारी के लिए) पेन्सिल अच्छी नहीं है।' सवा तीन बज गये। महोदय चाय पीने के लिए भीतर चले गये । अब टेबिल पर पेन्सिल है। भीतर पेन्सिल नहीं है। तीन बजे पेन्सिल उनके हाथ में थी, अब सवा तीन बजे पेन्सिल उनके हाथ में नहीं है। इस प्रकार भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न गुणधर्म सामने आते है । वस्तु के अनन्त धर्मों का विचार सापेक्ष ढंग से करना ही स्याद्वाद है। स्याद्वाद में दो पक्ष हैं-स्यात् और वाद । 'स्यात्' एक अव्यय है जो कथंचित्, किसी अपेक्षा से, अमुक दृष्टि से इस अर्थ का द्योतक है और 'वाद' मतलब सिद्धान्त, मत या प्रतिपादन । इस प्रकार 'स्याद्वाद' पद का अर्थ हुआ सापेक्ष-सिद्धान्त, अपेक्षावाद, कथंचित्वाद या वह सिद्धान्त जो विविध दृष्टि बिन्दुओं से वस्तु-तत्त्व का निरीक्षण-परीक्षण करता है। साधारणतः स्याद्वाद को अनेकान्त कह दिया जाता है। लेकिन दोनों में प्रतिपाद्य, प्रति Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4