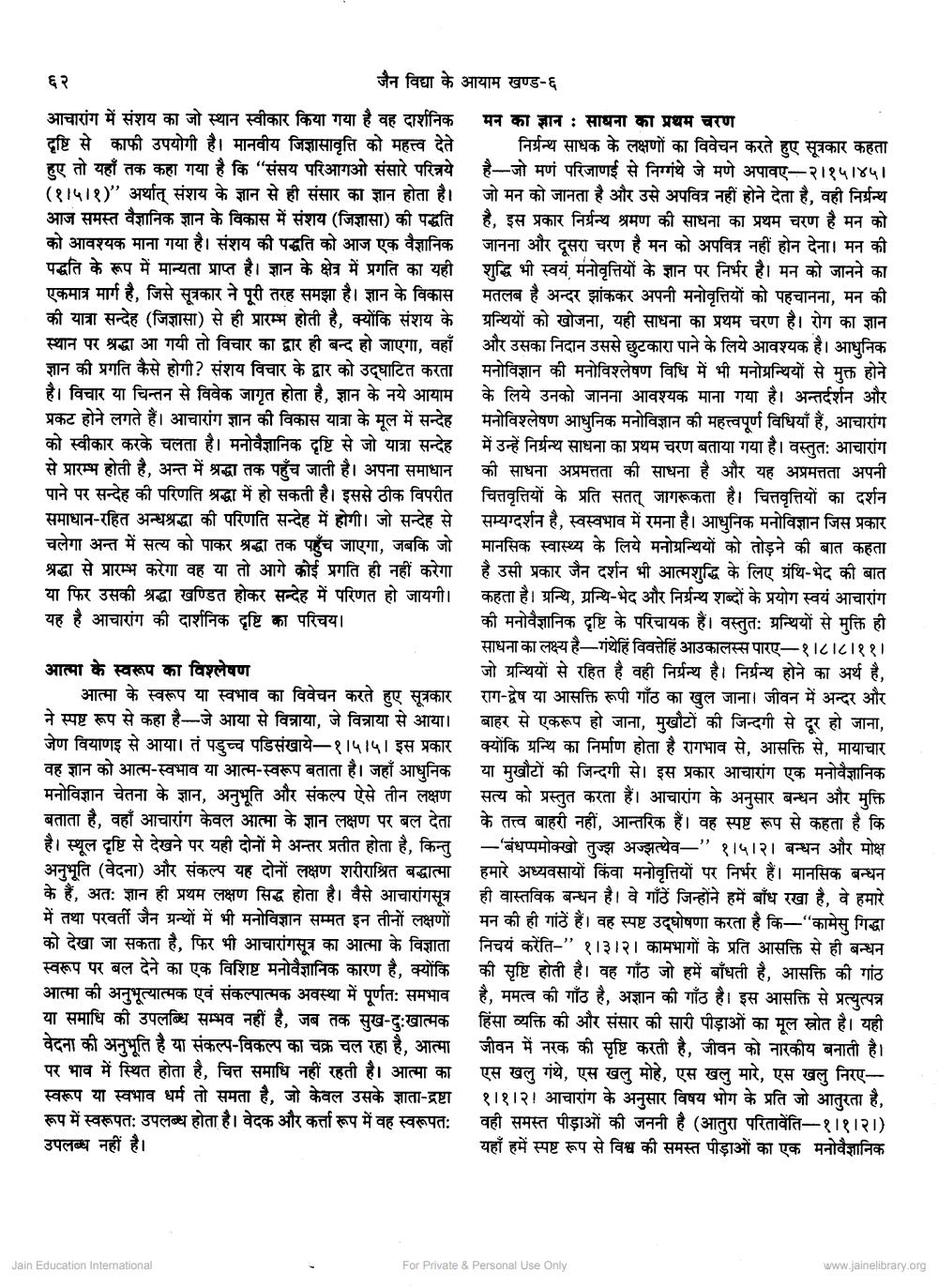Book Title: Acharangsutra Ek Vishleshan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 2
________________ ६२ आचारांग में संशय का जो स्थान स्वीकार किया गया है वह दार्शनिक दृष्टि से काफी उपयोगी है। मानवीय जिज्ञासावृत्ति को महत्त्व देते हुए तो यहाँ तक कहा गया है कि "संसय परिआगओ संसारे परिनये (१।५।१) " अर्थात् संशय के ज्ञान से ही संसार का ज्ञान होता है। आज समस्त वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में संशय (जिज्ञासा) की पद्धति को आवश्यक माना गया है। संशय की पद्धति को आज एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का यही एकमात्र मार्ग है, जिसे सूत्रकार ने पूरी तरह समझा है। ज्ञान के विकास की यात्रा सन्देह ( जिज्ञासा) से ही प्रारम्भ होती है, क्योंकि संशय के स्थान पर श्रद्धा आ गयी तो विचार का द्वार ही बन्द हो जाएगा, वहाँ ज्ञान की प्रगति कैसे होगी? संशय विचार के द्वार को उद्घाटित करता है । विचार या चिन्तन से विवेक जागृत होता है, ज्ञान के नये आयाम प्रकट होने लगते हैं। आचारांग ज्ञान की विकास यात्रा के मूल में सन्देह को स्वीकार करके चलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो यात्रा सन्देह से प्रारम्भ होती है, अन्त में श्रद्धा तक पहुँच जाती है। अपना समाधान पाने पर सन्देह की परिणति श्रद्धा में हो सकती है। इससे ठीक विपरीत समाधान-रहित अन्धश्रद्धा की परिणति सन्देह में होगी। जो सन्देह से चलेगा अन्त में सत्य को पाकर श्रद्धा तक पहुँच जाएगा, जबकि जो श्रद्धा से प्रारम्भ करेगा वह या तो आगे कोई प्रगति ही नहीं करेगा या फिर उसकी श्रद्धा खण्डित होकर सन्देह में परिणत हो जायगी । यह है आचारांग की दार्शनिक दृष्टि का परिचय | जैन विद्या के आयाम खण्ड - ६ आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण आत्मा के स्वरूप या स्वभाव का विवेचन करते हुए सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से कहा है- जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया। जेण वियाण से आया। तं पडुच्च पडिसंखाये - १1५1५1 इस प्रकार वह ज्ञान को आत्म-स्वभाव या आत्म-स्वरूप बताता है। जहाँ आधुनिक मनोविज्ञान चेतना के ज्ञान, अनुभूति और संकल्प ऐसे तीन लक्षण बताता है, वहाँ आचारांग केवल आत्मा के ज्ञान लक्षण पर बल देता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर यही दोनों में अन्तर प्रतीत होता है, किन्तु अनुभूति (वेदना) और संकल्प यह दोनों लक्षण शरीराश्रितद्धामा के हैं, अतः ज्ञान ही प्रथम लक्षण सिद्ध होता है। वैसे आचारांगसूत्र में तथा परवर्ती जैन ग्रन्थों में भी मनोविज्ञान सम्मत इन तीनों लक्षणों को देखा जा सकता है, फिर भी आचारांगसूत्र का आत्मा के विज्ञाता स्वरूप पर बल देने का एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि आत्मा की अनुभूत्यात्मक एवं संकल्पात्मक अवस्था में पूर्णतः समभाव या समाधि की उपलब्धि सम्भव नहीं है, जब तक सुख-दुःखात्मक वेदना की अनुभूति है या संकल्प-विकल्प का चक्र चल रहा है, आत्मा पर भाव में स्थित होता है, वित्त समाधि नहीं रहती है। आत्मा का स्वरूप या स्वभाव धर्म तो समता है, जो केवल उसके ज्ञाता-द्रष्टा रूप में स्वरूपतः उपलब्ध होता है वेदक और कर्ता रूप में वह स्वरूपतः उपलब्ध नहीं है। Jain Education International मन का ज्ञान साधना का प्रथम चरण निर्ग्रन्थ साधक के लक्षणों का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहता है जो मणं परिजाणई से निग्गंधे जे मणे अपावए - २।१५।४५ ॥ जो मन को जानता है और उसे अपवित्र नहीं होने देता है, वही निर्ग्रन्थ है, इस प्रकार निर्ग्रन्थ श्रमण की साधना का प्रथम चरण है मन को जानना और दूसरा चरण है मन को अपवित्र नहीं होन देना। मन की शुद्धि भी स्वयं मनोवृत्तियों के ज्ञान पर निर्भर है। मन को जानने का मतलब है अन्दर झांककर अपनी मनोवृत्तियों को पहचानना, मन की प्रन्थियों को खोजना, यही साधना का प्रथम चरण है। रोग का ज्ञान और उसका निदान उससे छुटकारा पाने के लिये आवश्यक है। आधुनिक मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण विधि में भी मनोग्रन्थियों से मुक्त होने के लिये उनको जानना आवश्यक माना गया है। अन्तर्दर्शन और मनोविश्लेषण आधुनिक मनोविज्ञान की महत्त्वपूर्ण विधियाँ हैं, आचारांग में उन्हें निर्मन्थ साधना का प्रथम चरण बताया गया है। वस्तुतः आचारांग की साधना अप्रमत्तता की साधना है और यह अप्रमत्तता अपनी चित्तवृत्तियों के प्रति सतत् जागरूकता है । चित्तवृत्तियों का दर्शन सम्यग्दर्शन है, स्वस्वभाव में रमना है आधुनिक मनोविज्ञान जिस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिये मनोग्रन्थियों को तोड़ने की बात कहता है उसी प्रकार जैन दर्शन भी आत्मशुद्धि के लिए ग्रंथि भेद की बात कहता है । ग्रन्थि, ग्रन्थि-भेद और निर्ग्रन्थ शब्दों के प्रयोग स्वयं आचारांग की मनोवैज्ञानिक दृष्टि के परिचायक हैं। वस्तुतः ग्रन्थियों से मुक्ति ही साधना का लक्ष्य है— गंथेहिं विवत्तेहिं आउकालस्स पारए - ११८ | ८ | ११ | जो ग्रन्थियों से रहित है वही निर्मन्य है। निर्मन्थ होने का अर्थ है, राग-द्वेष या आसक्ति रूपी गाँठ का खुल जाना जीवन में अन्दर और बाहर से एकरूप हो जाना, मुखौटों की जिन्दगी से दूर हो जाना, क्योंकि प्रन्थि का निर्माण होता है रागभाव से आसक्ति से, मायाचार या मुखौटों की जिन्दगी से। इस प्रकार आचारांग एक मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रस्तुत करता हैं। आचारांग के अनुसार बन्धन और मुक्ति के तत्व बाहरी नहीं, आन्तरिक हैं। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि - 'बंधप्यमोक्खो तुज्झ अज्झत्थेव – १२५|२| बन्धन और मोक्ष हमारे अध्यवसायों किंवा मनोवृत्तियों पर निर्भर हैं। मानसिक बन्धन ही वास्तविक बन्धन है वे गाँठें जिन्होंने हमें बाँध रखा है, वे हमारे मन की ही गांठें हैं। वह स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि - "कामेसु गिद्धा निचयं करेति " १।३।२। कामभागों के प्रति आसक्ति से ही बन्धन की सृष्टि होती है। वह गाँठ जो हमें बाँधती है, आसक्ति की गांठ है, ममत्व की गाँठ है, अज्ञान की गाँठ है। इस आसक्ति से प्रत्युत्पन्न हिंसा व्यक्ति की और संसार की सारी पीड़ाओं का मूल स्रोत है। यही जीवन में नरक की सृष्टि करती है, जीवन को नारकीय बनाती है। एस खलु गंधे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए१ । १ । २ । आचारांग के अनुसार विषय भोग के प्रति जो आतुरता है, वही समस्त पीड़ाओं की जननी है (आतुरा परितावेति - १।१।२ । ) यहाँ हमें स्पष्ट रूप से विश्व की समस्त पीड़ाओं का एक मनोवैज्ञानिक 33 For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 41