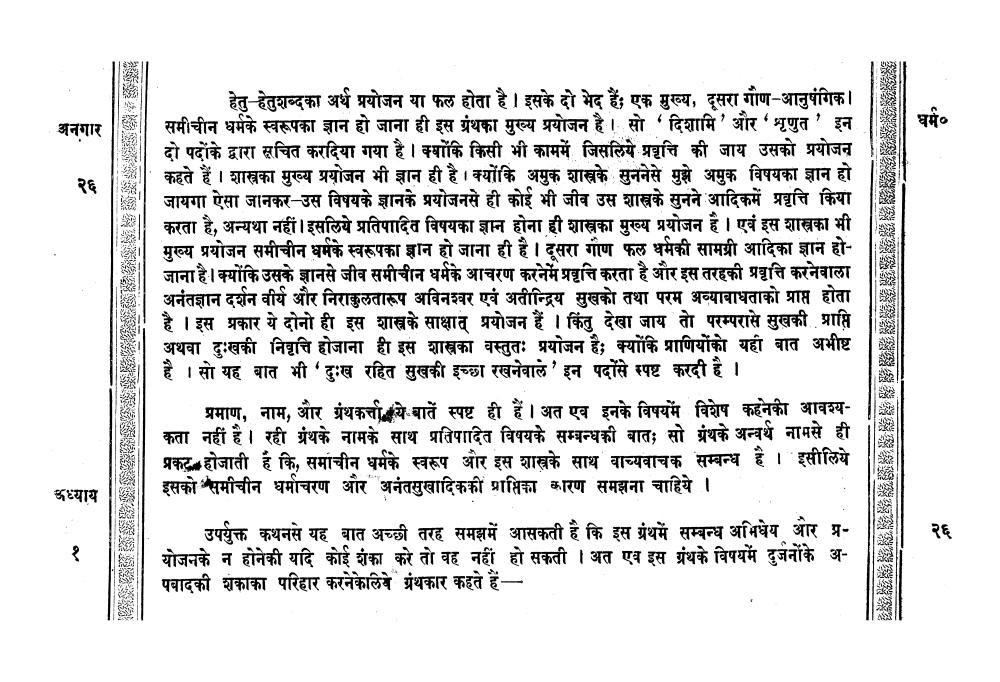________________
अनगार
हेतु-हेतुशब्दका अर्थ प्रयोजन या फल होता है । इसके दो भेद हैं; एक मुख्य, दूसरा गौण-आनुषंगिक । समीचीन धर्मके स्वरूपका ज्ञान हो जाना ही इस ग्रंथका मुख्य प्रयोजन है। सो 'दिशामि' और 'शृणुत' इन दो पदोंके द्वारा सचित करदिया गया है। क्योंकि किसी भी काममें जिसलिये प्रवृत्ति की जाय उसको प्रयोजन कहते हैं । शास्त्रका मुख्य प्रयोजन भी ज्ञान ही है। क्योंकि अमुक शास्त्रके सुननेसे मुझे अमुक विषयका ज्ञान हो जायगा ऐसा जानकर-उस विषयके ज्ञानके प्रयोजनसे ही कोई भी जीव उस शास्त्रके सुनने आदिकमें प्रवृत्ति किया करता है, अन्यथा नहीं। इसलिये प्रतिपादित विषयका ज्ञान होना ही शास्त्रका मुख्य प्रयोजन है । एवं इस शास्त्रका भी मुख्य प्रयोजन समीचीन धर्मके स्वरूपका ज्ञान हो जाना ही है । दूसरा गौण फल धर्मकी सामग्री आदिका ज्ञान होजाना है। क्योंकि उसके ज्ञानसे जीव समीचीन धर्मके आचरण करनेमें प्रवृत्ति करता है और इस तरहकी प्रवृत्ति करनेवाला अनंतज्ञान दर्शन वीर्य और निराकुलतारूप अविनश्वर एवं अतीन्द्रिय सुखको तथा परम अव्यावाधताको प्राप्त होता है । इस प्रकार ये दोनो ही इस शास्त्रके साक्षात् प्रयोजन हैं । किंतु देखा जाय तो परम्परासे सुखकी प्राप्ति अथवा दुःखकी निवृत्ति होजाना ही इस शास्त्रका वस्तुतः प्रयोजन है; क्योंक प्राणियोंको यही बात अभीष्ट है । सो यह बात भी 'दुःख रहित सुखकी इच्छा रखनेवाले' इन पदोंसे स्पष्ट करदी है ।
प्रमाण, नाम, और ग्रंथकर्ता, ये बातें स्पष्ट ही हैं। अत एव इनके विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। रही ग्रंथके नामके साथ प्रतिपादित विषयके सम्बन्धकी बात; सो ग्रंथके अन्वर्थ नामसे ही प्रकट होजाती है कि, समाचीन धर्मके स्वरूप और इस शास्त्रके साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध है । इसीलिये इसको समीचीन धर्माचरण और अनंतसुखादिककी प्राप्तिका कारण समझना चाहिये ।
अध्याया
उपर्युक्त कथनसे यह बात अच्छी तरह समझमें आसकती है कि इस ग्रंथमें सम्बन्ध अभिधेय और प्रयोजनके न होनेकी यदि कोई शंका करे तो वह नहीं हो सकती । अत एव इस ग्रंथके विषयमें दुजनोंके अपबादकी शकाका परिहार करनेकेलिये ग्रंथकार कहते हैं