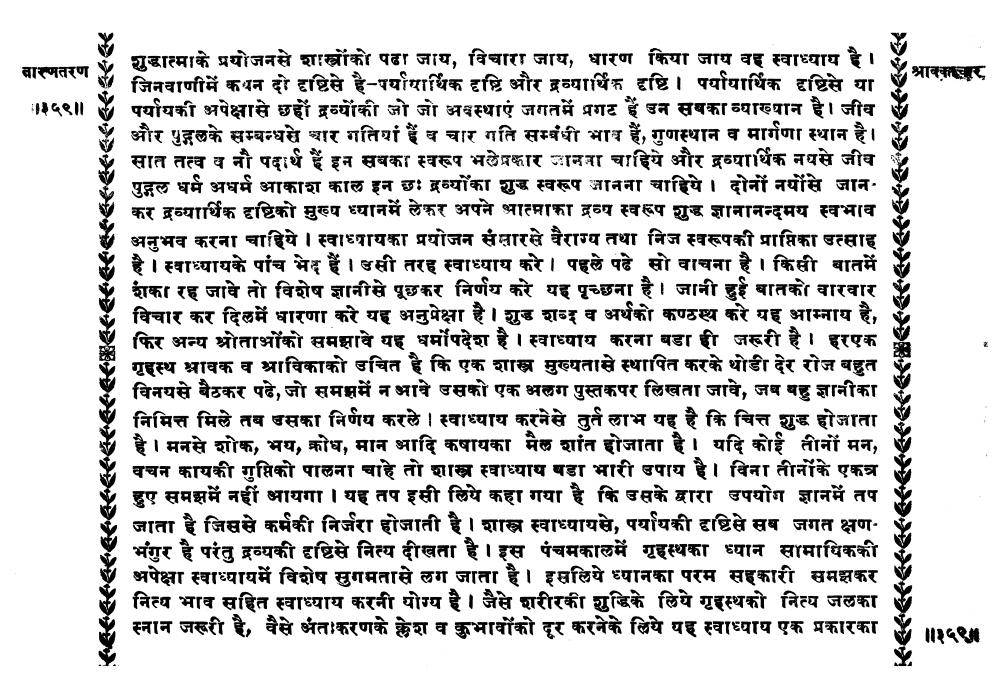________________
वारणतरण
शुद्धात्माके प्रयोजनसे शास्त्रोंको पढा जाय, विचारा जाय, धारण किया जाय वह स्वाध्याय है। जिनवाणीमें कथन दो दृष्टिसे है-पर्यायार्थिक दृष्टि और द्रव्यार्थिक दृष्टि। पर्यायार्थिक दृष्टिसे या पर्यायकी अपेक्षासे छहों द्रव्योंकी जो जो अवस्थाएं जगतमें प्रगट है उन सबका व्याख्यान है। जीव और पुद्गलके सम्बन्धसे चार गतिणं व चार गति सम्बंधी भाव हैं, गुणस्थान व मार्गणा स्थान है। सात तत्व व नौ पदार्थ हैं इन सबका स्वरूप भले प्रकार जानना चाहिये और द्रव्यार्थिक नबसे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन छ: द्रव्योंका शुद्ध स्वरूप जानना चाहिये। दोनों नयोंसे जानकर द्रव्यार्थिक दृष्टिको मुख्य ध्यानमें लेकर अपने आत्माका द्रव्य स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभाव अनुभव करना चाहिये । स्वाध्यायका प्रयोजन संसारसे वैराग्य तथा निज स्वरूपकी प्राप्तिका उत्साह है। स्वाध्यायके पांच भेद हैं। उसी तरह स्वाध्याय करे। पहले पढे सो वाचना है। किसी बातमें शंका रह जावे तो विशेष ज्ञानीसे पूछकर निर्णय करे यह पृच्छना है। जानी हुई बातको वारवार विचार कर दिल में धारणा करे यह अनुपेक्षा है। शुद्ध शब्द व अर्थको कण्ठस्थ करे यह आम्नाय है, फिर अन्य श्रोताओंको समझावे यह धर्मोपदेश है । स्वाध्याय करना बडा ही जरूरी है। हरएक
गृहस्थ श्रावक व श्राविकाको उचित है कि एक शास्त्र मुख्यतासे स्थापित करके थोडी देर रोज बहुत ॐ विनयसे बैठकर पढे, जो समझ में न आवे उसको एक अलग पुस्तकपर लिखता जावे, जब बहु ज्ञानीका निमित्त मिले तब उसका निर्णय करले । स्वाध्याय करनेसे तुर्त लाभ यह है कि चित्त शुद्ध होजाता है। मनसे शोक, भय, क्रोध, मान आदि कषायका मैल शांत होजाता है। यदि कोई तीनों मन, वचन कायकी गुप्तिको पालना चाहे तो शास्त्र स्वाध्याय बडा भारी उपाय है। विना तीनोंके एकत्र हुए समझमें नहीं आयगा । यह तप इसी लिये कहा गया है कि उसके द्वारा उपयोग ज्ञानमें तप जाता है जिससे कर्मकी निर्जरा होजाती है। शास्त्र स्वाध्यायसे, पर्यायकी दृष्टिसे सब जगत क्षणभंगुर है परंतु द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य दीखता है। इस पंचमकालमें गृहस्थका ध्यान सामायिककी अपेक्षा स्वाध्यायमें विशेष सुगमतासे लग जाता है। इसलिये ध्यानका परम सहकारी समझकर नित्य भाव सहित स्वाध्याय करनी योग्य है। जैसे शरीरकी शुद्धिके लिये गृहस्थको नित्य जलका स्नान जरूरी है, वैसे अंताकरणके क्लेश व कुभावोंको दूर करनेके लिये यह स्वाध्याय एक प्रकारका