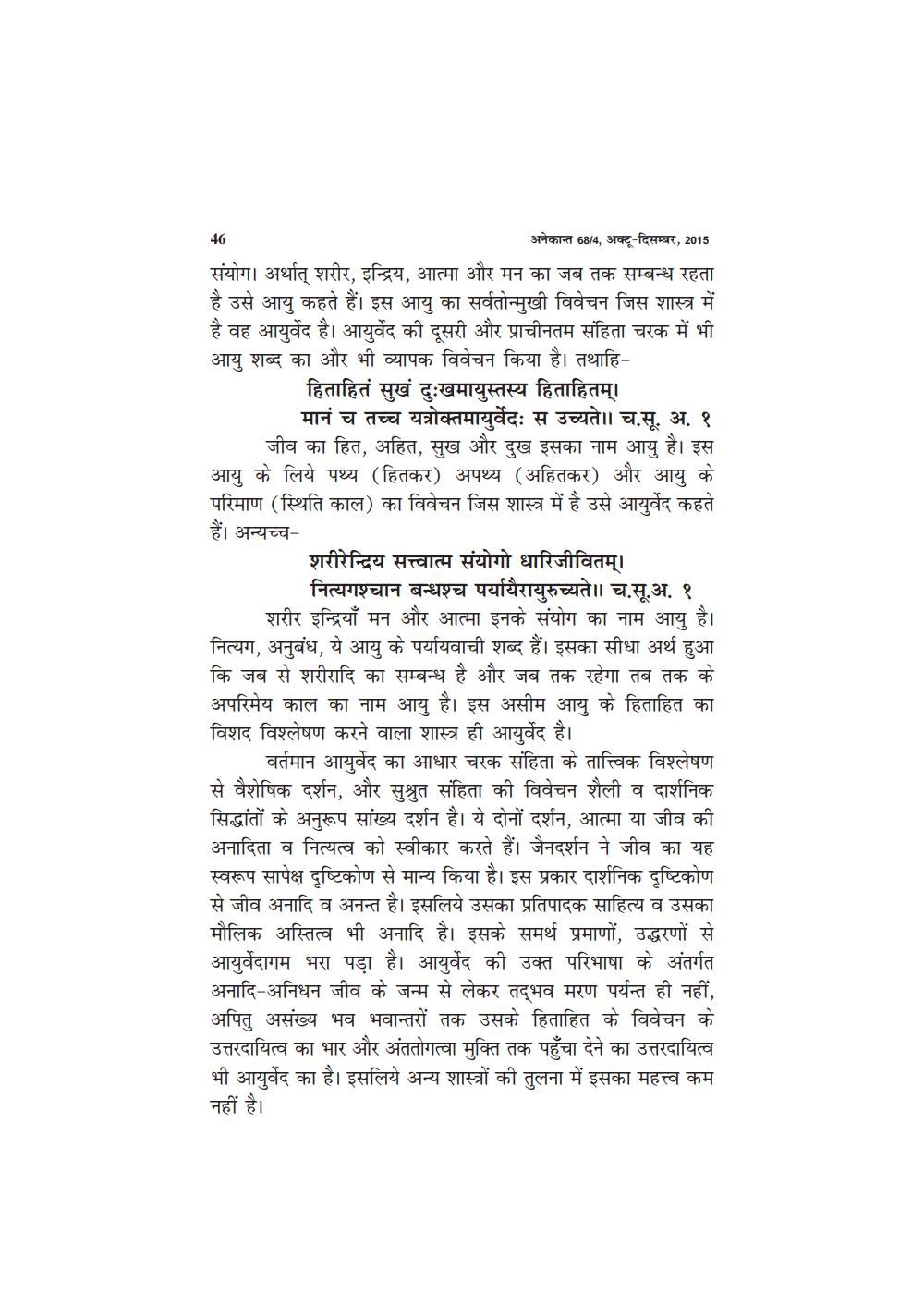________________
अनेकान्त 68/4, अक्टू-दिसम्बर, 2015 संयोग। अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, आत्मा और मन का जब तक सम्बन्ध रहता है उसे आयु कहते हैं। इस आयु का सर्वतोन्मुखी विवेचन जिस शास्त्र में है वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद की दूसरी और प्राचीनतम संहिता चरक में भी आयु शब्द का और भी व्यापक विवेचन किया है। तथाहि
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥ च.सू. अ. १
जीव का हित, अहित, सुख और दुख इसका नाम आयु है। इस आयु के लिये पथ्य (हितकर) अपथ्य (अहितकर) और आयु के परिमाण (स्थिति काल) का विवेचन जिस शास्त्र में है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अन्यच्च
शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्म संयोगो धारिजीवितम्।
नित्यगश्चान बन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते॥ च.सू.अ. १
शरीर इन्द्रियाँ मन और आत्मा इनके संयोग का नाम आयु है। नित्यग, अनुबंध, ये आयु के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका सीधा अर्थ हुआ कि जब से शरीरादि का सम्बन्ध है और जब तक रहेगा तब तक के
अपरिमेय काल का नाम आयु है। इस असीम आयु के हिताहित का विशद विश्लेषण करने वाला शास्त्र ही आयुर्वेद है।
वर्तमान आयुर्वेद का आधार चरक संहिता के तात्त्विक विश्लेषण से वैशेषिक दर्शन, और सुश्रुत संहिता की विवेचन शैली व दार्शनिक सिद्धांतों के अनुरूप सांख्य दर्शन है। ये दोनों दर्शन, आत्मा या जीव की अनादिता व नित्यत्व को स्वीकार करते हैं। जैनदर्शन ने जीव का यह स्वरूप सापेक्ष दृष्टिकोण से मान्य किया है। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टिकोण से जीव अनादि व अनन्त है। इसलिये उसका प्रतिपादक साहित्य व उसका मौलिक अस्तित्व भी अनादि है। इसके समर्थ प्रमाणों, उद्धरणों से आयुर्वेदागम भरा पड़ा है। आयुर्वेद की उक्त परिभाषा के अंतर्गत अनादि-अनिधन जीव के जन्म से लेकर तद्भव मरण पर्यन्त ही नहीं, अपितु असंख्य भव भवान्तरों तक उसके हिताहित के विवेचन के उत्तरदायित्व का भार और अंततोगत्वा मुक्ति तक पहुँचा देने का उत्तरदायित्व भी आयुर्वेद का है। इसलिये अन्य शास्त्रों की तुलना में इसका महत्त्व कम नहीं है।