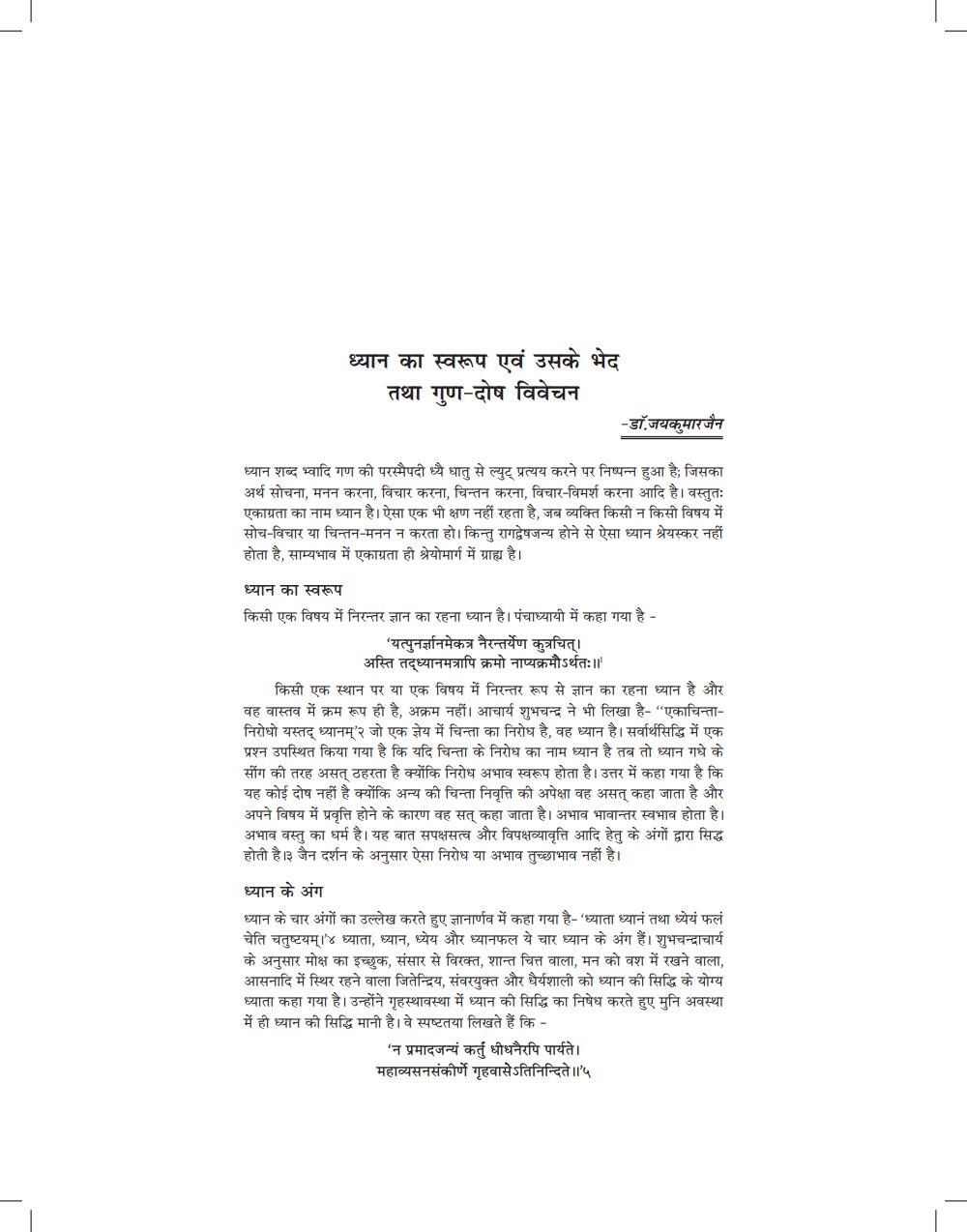________________
ध्यान का स्वरूप एवं उसके भेद तथा गुण-दोष विवेचन
-डॉ.जयकुमारजैन
ध्यान शब्द भ्वादि गण की परस्मैपदी ध्यै धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है; जिसका अर्थ सोचना, मनन करना, विचार करना, चिन्तन करना, विचार-विमर्श करना आदि है। वस्तुतः एकाग्रता का नाम ध्यान है। ऐसा एक भी क्षण नहीं रहता है, जब व्यक्ति किसी न किसी विषय में सोच-विचार या चिन्तन-मनन न करता हो। किन्तु रागद्वेषजन्य होने से ऐसा ध्यान श्रेयस्कर नहीं होता है, साम्यभाव में एकाग्रता ही श्रेयोमार्ग में ग्राह्य है।
ध्यान का स्वरूप किसी एक विषय में निरन्तर ज्ञान का रहना ध्यान है। पंचाध्यायी में कहा गया है -
'यत्पुनर्ज्ञानमेकत्र नैरन्तर्येण कुत्रचित्।
अस्ति तद्ध्यानमत्रापि क्रमो नाप्यक्रमौऽर्थतः॥ किसी एक स्थान पर या एक विषय में निरन्तर रूप से ज्ञान का रहना ध्यान है और वह वास्तव में क्रम रूप ही है, अक्रम नहीं। आचार्य शुभचन्द्र ने भी लिखा है- “एकाचिन्तानिरोधो यस्तद ध्यानम्'२ जो एक ज्ञेय में चिन्ता का निरोध है. वह ध्यान है। सर्वार्थसिद्धि में एक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि यदि चिन्ता के निरोध का नाम ध्यान है तब तो ध्यान गधे के सींग की तरह असत् ठहरता है क्योंकि निरोध अभाव स्वरूप होता है। उत्तर में कहा गया है कि यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अन्य की चिन्ता निवृत्ति की अपेक्षा वह असत् कहा जाता है और अपने विषय में प्रवृत्ति होने के कारण वह सत् कहा जाता है। अभाव भावान्तर स्वभाव होता है। अभाव वस्तु का धर्म है। यह बात सपक्षसत्व और विपक्षव्यावृत्ति आदि हेतु के अंगों द्वारा सिद्ध होती है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा निरोध या अभाव तुच्छाभाव नहीं है।
ध्यान के अंग ध्यान के चार अंगों का उल्लेख करते हए ज्ञानार्णव में कहा गया है- 'ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं फलं चेति चतुष्टयम्।'४ ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यानफल ये चार ध्यान के अंग हैं। शुभचन्द्राचार्य के अनुसार मोक्ष का इच्छुक, संसार से विरक्त, शान्त चित्त वाला, मन को वश में रखने वाला, आसनादि में स्थिर रहने वाला जितेन्द्रिय, संवरयुक्त और धैर्यशाली को ध्यान की सिद्धि के योग्य ध्याता कहा गया है। उन्होंने गृहस्थावस्था में ध्यान की सिद्धि का निषेध करते हुए मुनि अवस्था में ही ध्यान की सिद्धि मानी है। वे स्पष्टतया लिखते हैं कि -
'न प्रमादजन्यं कर्तु धीधनैरपि पार्यते। महाव्यसनसंकीर्णे गृहवासेऽतिनिन्दिते॥५