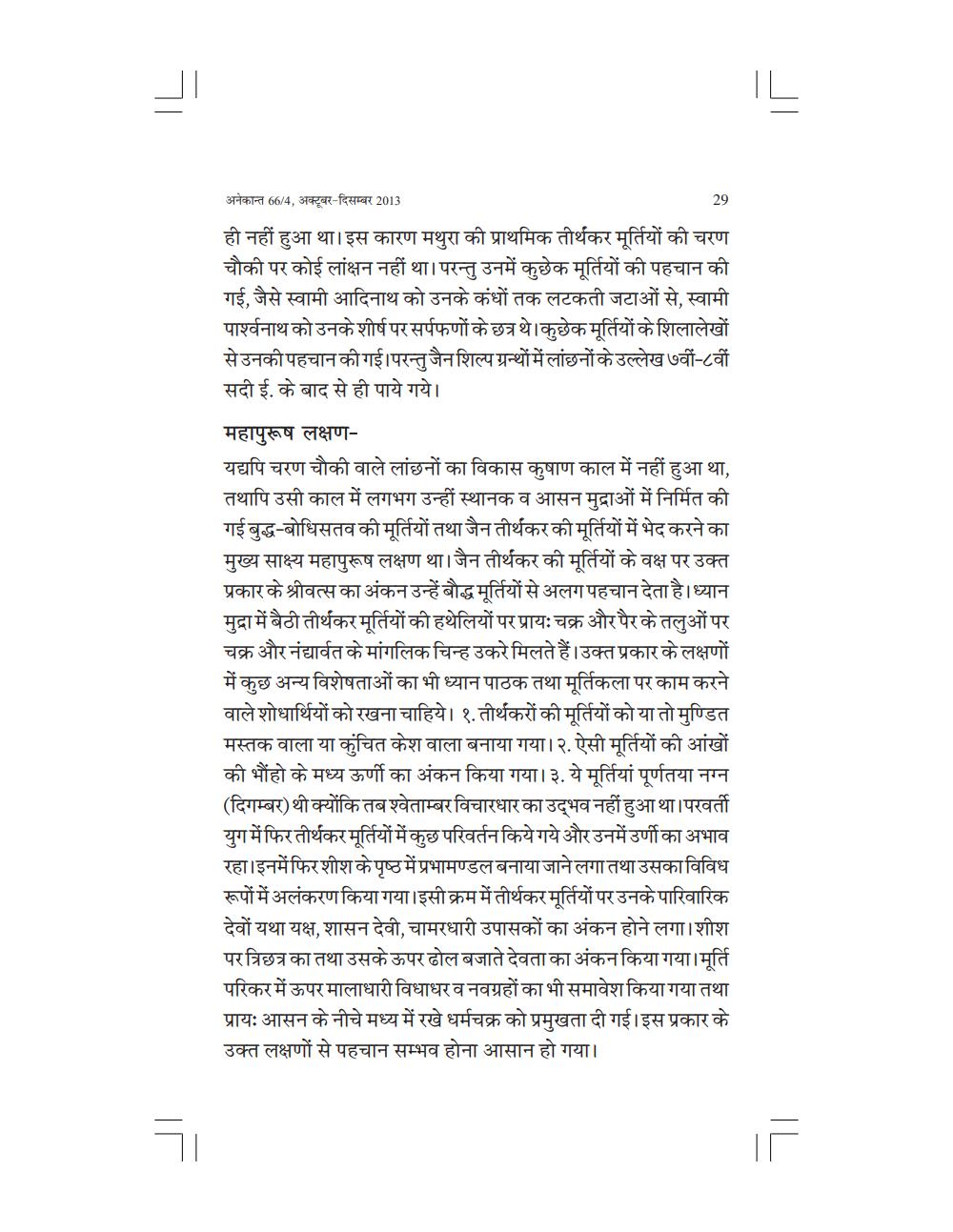________________
अनेकान्त 66/4, अक्टूबर-दिसम्बर 2013 ही नहीं हुआ था। इस कारण मथुरा की प्राथमिक तीर्थकर मूर्तियों की चरण चौकी पर कोई लांक्षन नहीं था। परन्तु उनमें कुछेक मूर्तियों की पहचान की गई, जैसे स्वामी आदिनाथ को उनके कंधों तक लटकती जटाओं से, स्वामी पार्श्वनाथ को उनके शीर्ष पर सर्पफणों के छत्र थे।कुछेक मूर्तियों के शिलालेखों से उनकी पहचान की गई।परन्तुजैन शिल्प ग्रन्थों में लांछनों के उल्लेख ७वीं-८वीं सदी ई. के बाद से ही पाये गये।
महापुरूष लक्षणयद्यपि चरण चौकी वाले लांछनों का विकास कुषाण काल में नहीं हुआ था, तथापि उसी काल में लगभग उन्हीं स्थानक व आसन मुद्राओं में निर्मित की गई बुद्ध-बोधिसतव की मूर्तियों तथा जैन तीर्थकर की मूर्तियों में भेद करने का मुख्य साक्ष्य महापुरूष लक्षण था। जैन तीर्थकर की मूर्तियों के वक्ष पर उक्त प्रकार के श्रीवत्स का अंकन उन्हें बौद्ध मूर्तियों से अलग पहचान देता है। ध्यान मुद्रा में बैठी तीर्थकर मूर्तियों की हथेलियों पर प्रायः चक्र और पैर के तलुओं पर चक्र और नंद्यार्वत के मांगलिक चिन्ह उकरे मिलते हैं। उक्त प्रकार के लक्षणों में कुछ अन्य विशेषताओं का भी ध्यान पाठक तथा मूर्तिकला पर काम करने वाले शोधार्थियों को रखना चाहिये। १. तीर्थकरों की मूर्तियों को या तो मुण्डित मस्तक वाला या कुंचित केश वाला बनाया गया। २. ऐसी मूर्तियों की आंखों की भौंहो के मध्य ऊर्णी का अंकन किया गया। ३. ये मूर्तियां पूर्णतया नग्न (दिगम्बर) थी क्योंकि तब श्वेताम्बर विचारधार का उद्भव नहीं हुआ था।परवर्ती युग में फिर तीर्थकर मूर्तियों में कुछ परिवर्तन किये गये और उनमें उर्णी का अभाव रहा।इनमें फिरशीश के पृष्ठ में प्रभामण्डल बनाया जाने लगा तथा उसका विविध रूपों में अलंकरण किया गया।इसी क्रम में तीर्थकर मूर्तियों पर उनके पारिवारिक देवों यथा यक्ष, शासन देवी, चामरधारी उपासकों का अंकन होने लगा।शीश पर त्रिछत्र का तथा उसके ऊपर ढोल बजाते देवता का अंकन किया गया।मूर्ति परिकर में ऊपर मालाधारी विधाधर व नवग्रहों का भी समावेश किया गया तथा प्रायः आसन के नीचे मध्य में रखे धर्मचक्र को प्रमुखता दी गई। इस प्रकार के उक्त लक्षणों से पहचान सम्भव होना आसान हो गया।