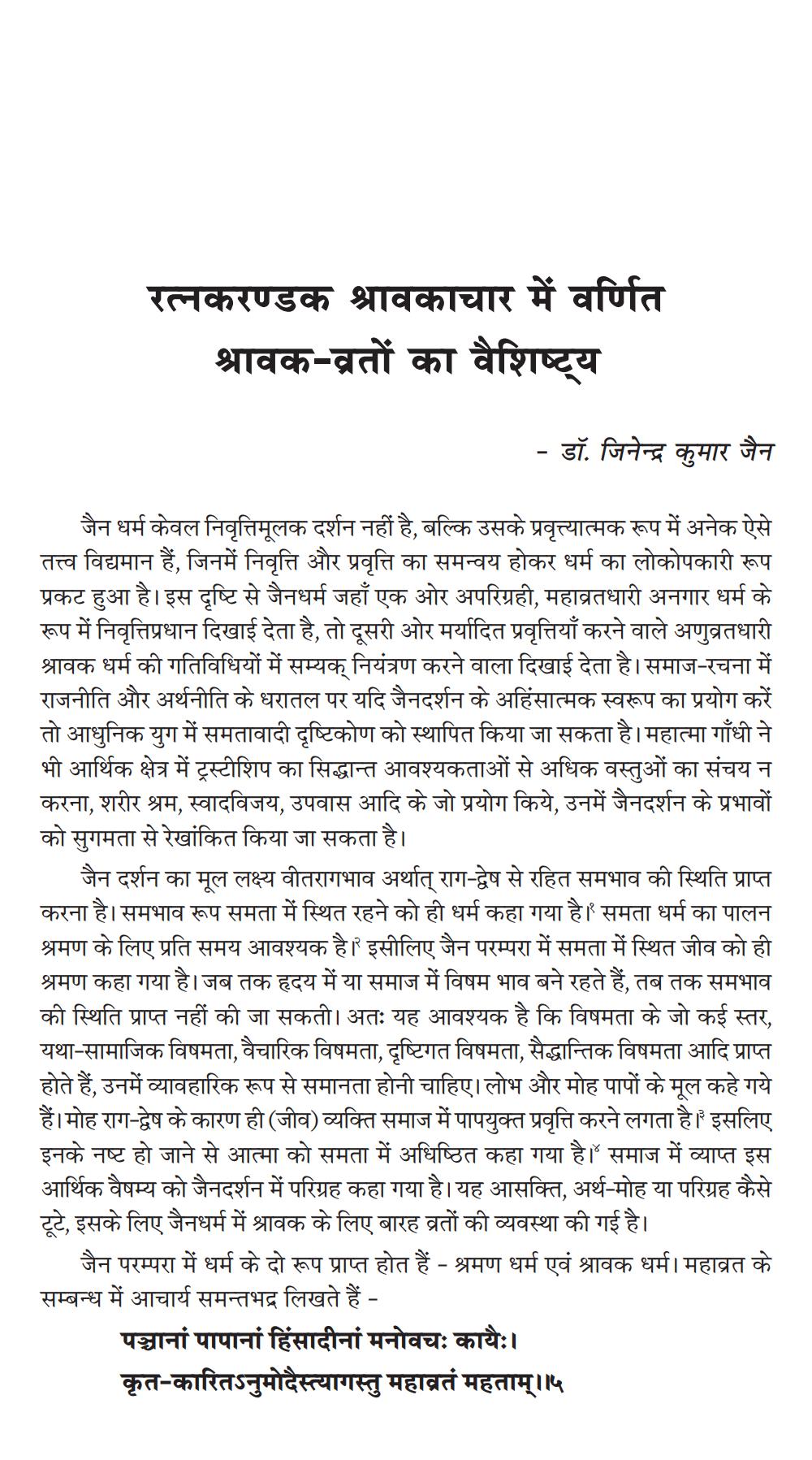________________
रत्नकरण्डक श्रावकाचार में वर्णित
श्रावक-व्रतों का वैशिष्ट्य
- डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन
जैन धर्म केवल निवृत्तिमूलक दर्शन नहीं है, बल्कि उसके प्रवृत्त्यात्मक रूप में अनेक ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं, जिनमें निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय होकर धर्म का लोकोपकारी रूप प्रकट हुआ है। इस दृष्टि से जैनधर्म जहाँ एक ओर अपरिग्रही, महाव्रतधारी अनगार धर्म के रूप में निवृत्तिप्रधान दिखाई देता है, तो दूसरी ओर मर्यादित प्रवृत्तियाँ करने वाले अणुव्रतधारी श्रावक धर्म की गतिविधियों में सम्यक् नियंत्रण करने वाला दिखाई देता है। समाज-रचना में राजनीति और अर्थनीति के धरातल पर यदि जैनदर्शन के अहिंसात्मक स्वरूप का प्रयोग करें तो आधुनिक युग में समतावादी दृष्टिकोण को स्थापित किया जा सकता है। महात्मा गाँधी ने भी आर्थिक क्षेत्र में ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संचय न करना, शरीर श्रम, स्वादविजय, उपवास आदि के जो प्रयोग किये, उनमें जैनदर्शन के प्रभावों को सुगमता से रेखांकित किया जा सकता है।
जैन दर्शन का मूल लक्ष्य वीतरागभाव अर्थात् राग-द्वेष से रहित समभाव की स्थिति प्राप्त करना है। समभाव रूप समता में स्थित रहने को ही धर्म कहा गया है। समता धर्म का पालन श्रमण के लिए प्रति समय आवश्यक है। इसीलिए जैन परम्परा में समता में स्थित जीव को ही श्रमण कहा गया है। जब तक हृदय में या समाज में विषम भाव बने रहते हैं, तब तक समभाव की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः यह आवश्यक है कि विषमता के जो कई स्तर, यथा-सामाजिक विषमता, वैचारिक विषमता, दृष्टिगत विषमता, सैद्धान्तिक विषमता आदि प्राप्त होते हैं, उनमें व्यावहारिक रूप से समानता होनी चाहिए। लोभ और मोह पापों के मूल कहे गये हैं। मोह राग-द्वेष के कारण ही (जीव) व्यक्ति समाज में पापयुक्त प्रवृत्ति करने लगता है। इसलिए इनके नष्ट हो जाने से आत्मा को समता में अधिष्ठित कहा गया है। समाज में व्याप्त इस आर्थिक वैषम्य को जैनदर्शन में परिग्रह कहा गया है। यह आसक्ति, अर्थ-मोह या परिग्रह कैसे टूटे, इसके लिए जैनधर्म में श्रावक के लिए बारह व्रतों की व्यवस्था की गई है। ___ जैन परम्परा में धर्म के दो रूप प्राप्त होत हैं - श्रमण धर्म एवं श्रावक धर्म। महाव्रत के सम्बन्ध में आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं -
पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः। कृत-कारितऽनुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्॥५