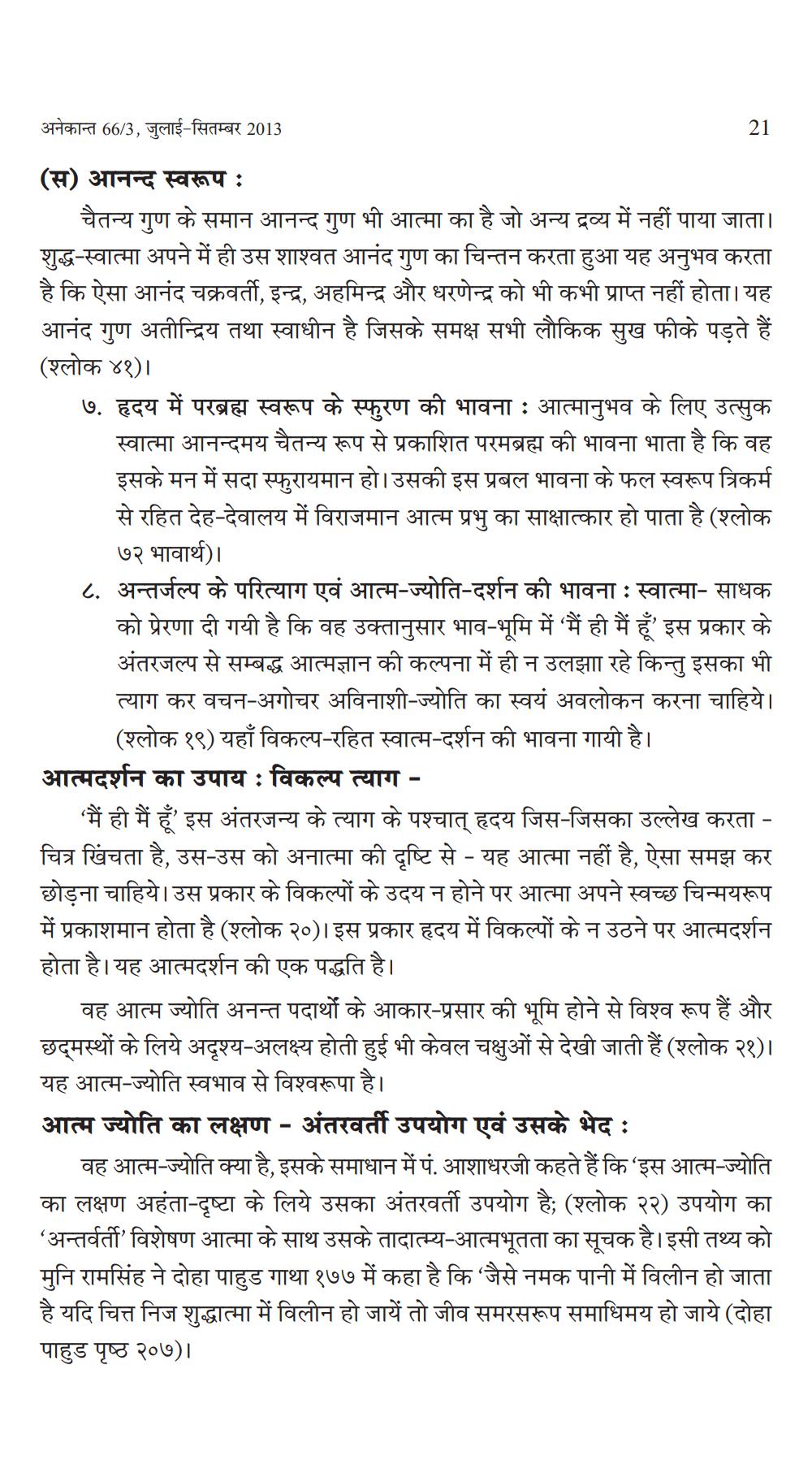________________
अनेकान्त 66/3, जुलाई-सितम्बर 2013
(स) आनन्द स्वरूप __ चैतन्य गुण के समान आनन्द गुण भी आत्मा का है जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। शुद्ध-स्वात्मा अपने में ही उस शाश्वत आनंद गुण का चिन्तन करता हुआ यह अनुभव करता है कि ऐसा आनंद चक्रवर्ती, इन्द्र, अहमिन्द्र और धरणेन्द्र को भी कभी प्राप्त नहीं होता। यह आनंद गुण अतीन्द्रिय तथा स्वाधीन है जिसके समक्ष सभी लौकिक सुख फीके पड़ते हैं (श्लोक ४१)।
७. हृदय में परब्रह्म स्वरूप के स्फुरण की भावना : आत्मानुभव के लिए उत्सुक
स्वात्मा आनन्दमय चैतन्य रूप से प्रकाशित परमब्रह्म की भावना भाता है कि वह इसके मन में सदा स्फुरायमान हो। उसकी इस प्रबल भावना के फल स्वरूप त्रिकर्म से रहित देह-देवालय में विराजमान आत्म प्रभु का साक्षात्कार हो पाता है (श्लोक
७२ भावार्थ)। ८. अन्तर्जल्प के परित्याग एवं आत्म-ज्योति-दर्शन की भावना : स्वात्मा- साधक
को प्रेरणा दी गयी है कि वह उक्तानुसार भाव-भूमि में 'मैं ही मैं हूँ' इस प्रकार के अंतरजल्प से सम्बद्ध आत्मज्ञान की कल्पना में ही न उलझा रहे किन्तु इसका भी त्याग कर वचन-अगोचर अविनाशी-ज्योति का स्वयं अवलोकन करना चाहिये।
(श्लोक १९) यहाँ विकल्प-रहित स्वात्म-दर्शन की भावना गायी है। आत्मदर्शन का उपाय : विकल्प त्याग -
_ 'मैं ही मैं हूँ' इस अंतरजन्य के त्याग के पश्चात् हृदय जिस-जिसका उल्लेख करता - चित्र खिंचता है, उस-उस को अनात्मा की दृष्टि से - यह आत्मा नहीं है, ऐसा समझ कर छोड़ना चाहिये। उस प्रकार के विकल्पों के उदय न होने पर आत्मा अपने स्वच्छ चिन्मयरूप में प्रकाशमान होता है (श्लोक २०)। इस प्रकार हृदय में विकल्पों के न उठने पर आत्मदर्शन होता है। यह आत्मदर्शन की एक पद्धति है।
वह आत्म ज्योति अनन्त पदार्थों के आकार-प्रसार की भूमि होने से विश्व रूप हैं और छद्मस्थों के लिये अदृश्य-अलक्ष्य होती हुई भी केवल चक्षुओं से देखी जाती हैं (श्लोक २१)। यह आत्म-ज्योति स्वभाव से विश्वरूपा है। आत्म ज्योति का लक्षण - अंतरवर्ती उपयोग एवं उसके भेद :
वह आत्म-ज्योति क्या है, इसके समाधान में पं. आशाधरजी कहते हैं कि 'इस आत्म-ज्योति का लक्षण अहंता-दृष्टा के लिये उसका अंतरवर्ती उपयोग है; (श्लोक २२) उपयोग का 'अन्तर्वर्ती' विशेषण आत्मा के साथ उसके तादात्म्य-आत्मभूतता का सूचक है। इसी तथ्य को मुनि रामसिंह ने दोहा पाहुड गाथा १७७ में कहा है कि जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है यदि चित्त निज शुद्धात्मा में विलीन हो जायें तो जीव समरसरूप समाधिमय हो जाये (दोहा पाहुड पृष्ठ २०७)।