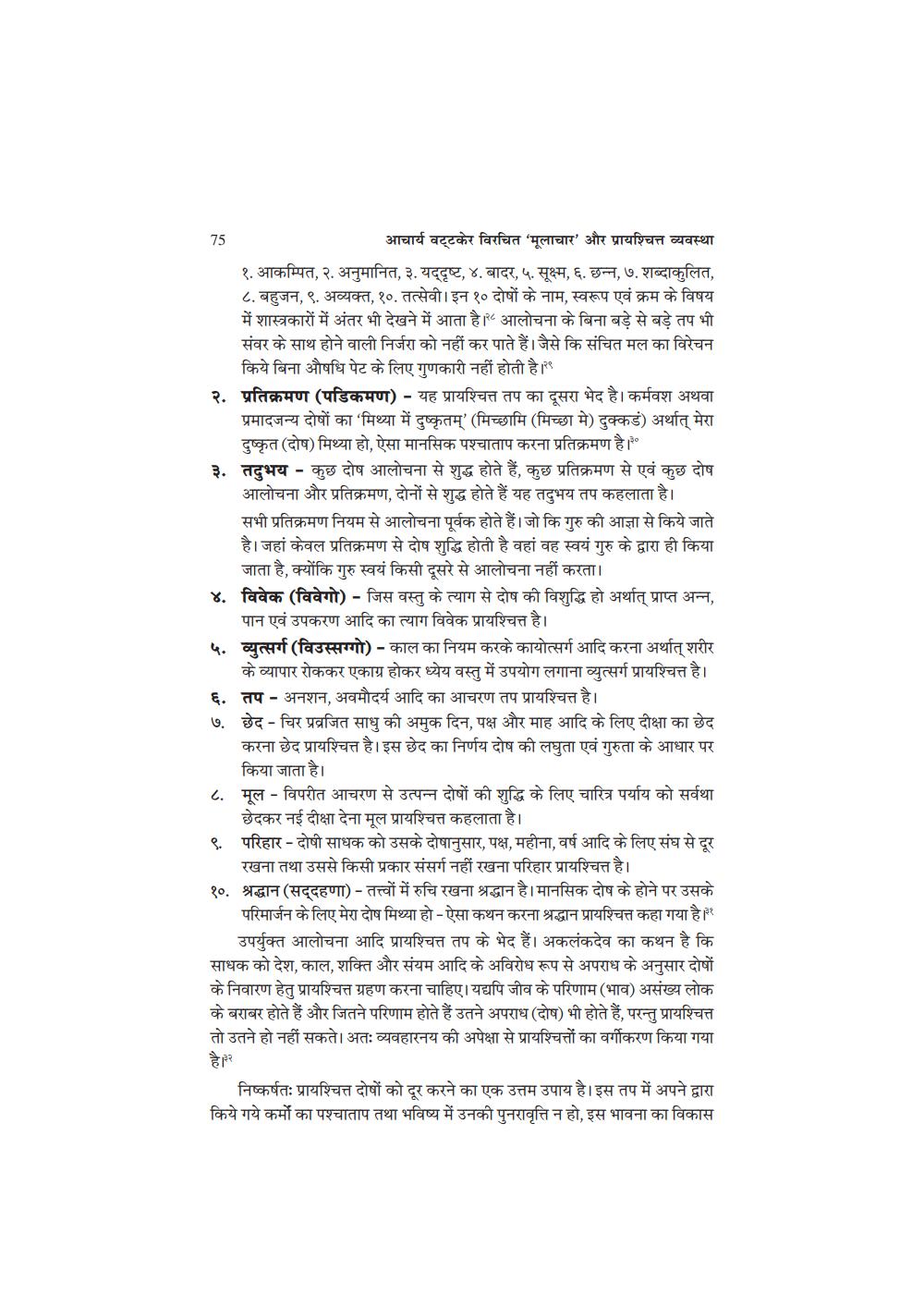________________
आचार्य वट्टकेर विरचित 'मूलाचार' और प्रायश्चित्त व्यवस्था १. आकम्पित, २. अनुमानित, ३. यदृष्ट, ४. बादर, ५. सूक्ष्म, ६. छन्न, ७. शब्दाकुलित, ८. बहुजन, ९. अव्यक्त, १०. तत्सेवी। इन १० दोषों के नाम, स्वरूप एवं क्रम के विषय में शास्त्रकारों में अंतर भी देखने में आता है। आलोचना के बिना बड़े से बड़े तप भी संवर के साथ होने वाली निर्जरा को नहीं कर पाते हैं। जैसे कि संचित मल का विरेचन किये बिना औषधि पेट के लिए गुणकारी नहीं होती है। प्रतिक्रमण (पडिकमण)- यह प्रायश्चित्त तप का दूसरा भेद है। कर्मवश अथवा प्रमादजन्य दोषों का 'मिथ्या में दुष्कृतम्' (मिच्छामि (मिच्छा मे) दुक्कड) अर्थात् मेरा
दुष्कृत (दोष) मिथ्या हो, ऐसा मानसिक पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है।' ३. तदुभय - कुछ दोष आलोचना से शुद्ध होते हैं, कुछ प्रतिक्रमण से एवं कुछ दोष
आलोचना और प्रतिक्रमण, दोनों से शुद्ध होते हैं यह तदुभय तप कहलाता है। सभी प्रतिक्रमण नियम से आलोचना पूर्वक होते हैं। जो कि गुरु की आज्ञा से किये जाते है। जहां केवल प्रतिक्रमण से दोष शुद्धि होती है वहां वह स्वयं गुरु के द्वारा ही किया
जाता है, क्योंकि गुरु स्वयं किसी दूसरे से आलोचना नहीं करता। ४. विवेक (विवेगो)- जिस वस्तु के त्याग से दोष की विशुद्धि हो अर्थात् प्राप्त अन्न,
पान एवं उपकरण आदि का त्याग विवेक प्रायश्चित्त है। ५. व्युत्सर्ग (विउस्सग्गो) - काल का नियम करके कायोत्सर्ग आदि करना अर्थात् शरीर
के व्यापार रोककर एकाग्र होकर ध्येय वस्तु में उपयोग लगाना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है।
तप - अनशन, अवमौदर्य आदि का आचरण तप प्रायश्चित्त है। ७. छेद - चिर प्रव्रजित साधु की अमुक दिन, पक्ष और माह आदि के लिए दीक्षा का छेद
करना छेद प्रायश्चित्त है। इस छेद का निर्णय दोष की लघुता एवं गुरुता के आधार पर किया जाता है। मूल - विपरीत आचरण से उत्पन्न दोषों की शुद्धि के लिए चारित्र पर्याय को सर्वथा छेदकर नई दीक्षा देना मूल प्रायश्चित्त कहलाता है। परिहार - दोषी साधक को उसके दोषानुसार, पक्ष, महीना, वर्ष आदि के लिए संघ से दूर
रखना तथा उससे किसी प्रकार संसर्ग नहीं रखना परिहार प्रायश्चित्त है। १०. श्रद्धान (सद्दहणा) - तत्त्वों में रुचि रखना श्रद्धान है। मानसिक दोष के होने पर उसके
परिमार्जन के लिए मेरा दोष मिथ्या हो-ऐसा कथन करना श्रद्धान प्रायश्चित्त कहा गया है।
उपर्युक्त आलोचना आदि प्रायश्चित्त तप के भेद हैं। अकलंकदेव का कथन है कि साधक को देश, काल, शक्ति और संयम आदि के अविरोध रूप से अपराध के अनुसार दोषों के निवारण हेतु प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि जीव के परिणाम (भाव) असंख्य लोक के बराबर होते हैं और जितने परिणाम होते हैं उतने अपराध (दोष) भी होते हैं, परन्तु प्रायश्चित्त तो उतने हो नहीं सकते। अतः व्यवहारनय की अपेक्षा से प्रायश्चित्तों का वर्गीकरण किया गया
९.
पाप
निष्कर्षतः प्रायश्चित्त दोषों को दूर करने का एक उत्तम उपाय है। इस तप में अपने द्वारा किये गये कर्मों का पश्चाताप तथा भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो, इस भावना का विकास