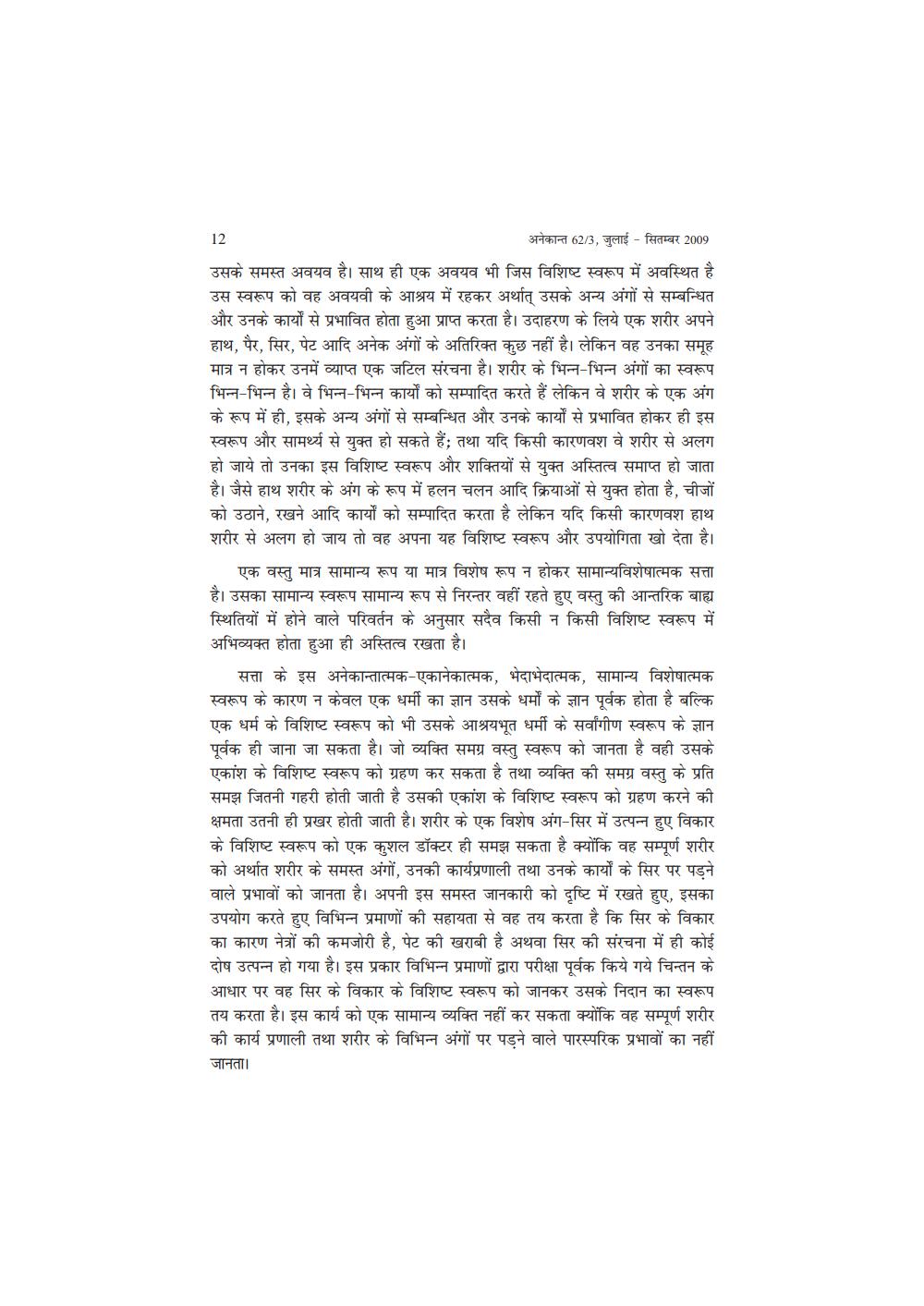________________
अनेकान्त 62/3, जुलाई-सितम्बर 2009
उसके समस्त अवयव है। साथ ही एक अवयव भी जिस विशिष्ट स्वरूप में अवस्थित है उस स्वरूप को वह अवयवी के आश्रय में रहकर अर्थात् उसके अन्य अंगों से सम्बन्धित
और उनके कार्यों से प्रभावित होता हुआ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिये एक शरीर अपने हाथ, पैर, सिर, पेट आदि अनेक अंगों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन वह उनका समूह मात्र न होकर उनमें व्याप्त एक जटिल संरचना है। शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों का स्वरूप भिन्न-भिन्न है। वे भिन्न-भिन्न कार्यों को सम्पादित करते हैं लेकिन वे शरीर के एक अंग के रूप में ही, इसके अन्य अंगों से सम्बन्धित और उनके कार्यों से प्रभावित होकर ही इस स्वरूप और सामर्थ्य से युक्त हो सकते हैं; तथा यदि किसी कारणवश वे शरीर से अलग हो जाये तो उनका इस विशिष्ट स्वरूप और शक्तियों से युक्त अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे हाथ शरीर के अंग के रूप में हलन चलन आदि क्रियाओं से युक्त होता है, चीजों को उठाने, रखने आदि कार्यों को सम्पादित करता है लेकिन यदि किसी कारणवश हाथ शरीर से अलग हो जाय तो वह अपना यह विशिष्ट स्वरूप और उपयोगिता खो देता है।
एक वस्तु मात्र सामान्य रूप या मात्र विशेष रूप न होकर सामान्यविशेषात्मक सत्ता है। उसका सामान्य स्वरूप सामान्य रूप से निरन्तर वहीं रहते हुए वस्तु की आन्तरिक बाह्य स्थितियों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार सदैव किसी न किसी विशिष्ट स्वरूप में अभिव्यक्त होता हुआ ही अस्तित्व रखता है।
सत्ता के इस अनेकान्तात्मक-एकानेकात्मक, भेदाभेदात्मक, सामान्य विशेषात्मक स्वरूप के कारण न केवल एक धर्मी का ज्ञान उसके धर्मों के ज्ञान पूर्वक होता है बल्कि एक धर्म के विशिष्ट स्वरूप को भी उसके आश्रयभूत धर्मी के सर्वांगीण स्वरूप के ज्ञान पूर्वक ही जाना जा सकता है। जो व्यक्ति समग्र वस्तु स्वरूप को जानता है वही उसके एकांश के विशिष्ट स्वरूप को ग्रहण कर सकता है तथा व्यक्ति की समग्र वस्तु के प्रति समझ जितनी गहरी होती जाती है उसकी एकांश के विशिष्ट स्वरूप को ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही प्रखर होती जाती है। शरीर के एक विशेष अंग-सिर में उत्पन्न हुए विकार के विशिष्ट स्वरूप को एक कुशल डॉक्टर ही समझ सकता है क्योंकि वह सम्पूर्ण शरीर को अर्थात शरीर के समस्त अंगों, उनकी कार्यप्रणाली तथा उनके कार्यों के सिर पर पड़ने वाले प्रभावों को जानता है। अपनी इस समस्त जानकारी को दृष्टि में रखते हुए, इसका उपयोग करते हुए विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वह तय करता है कि सिर के विकार का कारण नेत्रों की कमजोरी है, पेट की खराबी है अथवा सिर की संरचना में ही कोई दोष उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार विभिन्न प्रमाणों द्वारा परीक्षा पूर्वक किये गये चिन्तन के आधार पर वह सिर के विकार के विशिष्ट स्वरूप को जानकर उसके निदान का स्वरूप तय करता है। इस कार्य को एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि वह सम्पूर्ण शरीर की कार्य प्रणाली तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले पारस्परिक प्रभावों का नहीं जानता।