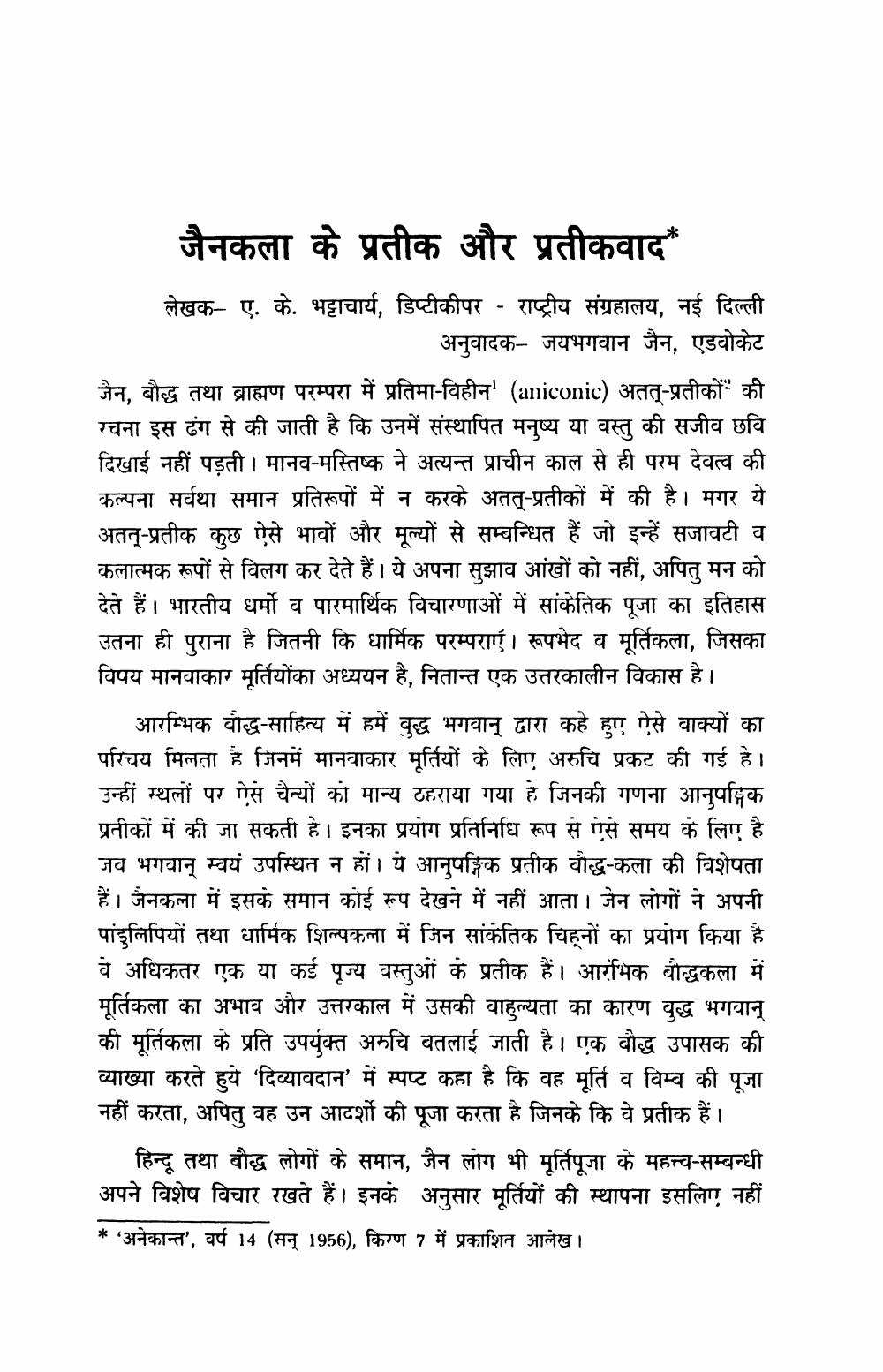________________
जैनकला के प्रतीक और प्रतीकवाद *
लेखक - ए. के. भट्टाचार्य, डिप्टीकीपर - राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली अनुवादक - जयभगवान जैन, एडवोकेट जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण परम्परा में प्रतिमा - विहीन' (aniconic) अतत्-प्रतीकों" की रचना इस ढंग से की जाती है कि उनमें संस्थापित मनुष्य या वस्तु की सजीव छवि दिखाई नहीं पड़ती। मानव मस्तिष्क ने अत्यन्त प्राचीन काल से ही परम देवत्व की कल्पना सर्वथा समान प्रतिरूपों में न करके अतत्-प्रतीकों में की है। मगर ये अतत्-प्रतीक कुछ ऐसे भावों और मूल्यों से सम्बन्धित हैं जो इन्हें सजावटी व कलात्मक रूपों से विलग कर देते हैं । ये अपना सुझाव आंखों को नहीं, अपितु मन को देते हैं। भारतीय धर्मो व पारमार्थिक विचारणाओं में सांकेतिक पूजा का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि धार्मिक परम्पराएं । रूपभेद व मूर्तिकला, जिसका विषय मानवाकार मूर्तियोंका अध्ययन है, नितान्त एक उत्तरकालीन विकास है।
आरम्भिक बौद्ध साहित्य में हमें बुद्ध भगवान् द्वारा कहे हुए ऐसे वाक्यों का परिचय मिलता है जिनमें मानवाकार मूर्तियों के लिए अरुचि प्रकट की गई है। उन्हीं स्थलों पर ऐसे चैन्यों की मान्य ठहराया गया है जिनकी गणना आनुषङ्गिक प्रतीकों में की जा सकती है। इनका प्रयोग प्रतिनिधि रूप से ऐसे समय के लिए है। जव भगवान् स्वयं उपस्थित न हों। ये आनुषङ्गिक प्रतीक बौद्ध कला की विशेषता हैं। जैनकला में इसके समान कोई रूप देखने में नहीं आता । जेन लोगों ने अपनी पांडुलिपियों तथा धार्मिक शिल्पकला में जिन सांकेतिक चिह्नों का प्रयोग किया है। वे अधिकतर एक या कई पूज्य वस्तुओं के प्रतीक हैं। आरंभिक बौद्धकला में मूर्तिकला का अभाव और उत्तरकाल में उसकी बाहुल्यता का कारण बुद्ध भगवान् की मूर्तिकला के प्रति उपर्युक्त अरुचि वतलाई जाती है। एक बौद्ध उपासक की व्याख्या करते हुये 'दिव्यावदान' में स्पष्ट कहा है कि वह मूर्ति व विम्ब की पूजा नहीं करता, अपितु वह उन आदर्शो की पूजा करता है जिनके कि वे प्रतीक हैं ।
हिन्दू तथा बौद्ध लोगों के समान, जैन लोग भी मूर्तिपूजा के महत्त्व - सम्बन्धी अपने विशेष विचार रखते हैं। इनके अनुसार मूर्तियों की स्थापना इसलिए नहीं * 'अनेकान्त', वर्ष 14 ( सन् 1956), किरण 7 में प्रकाशित आलेख ।