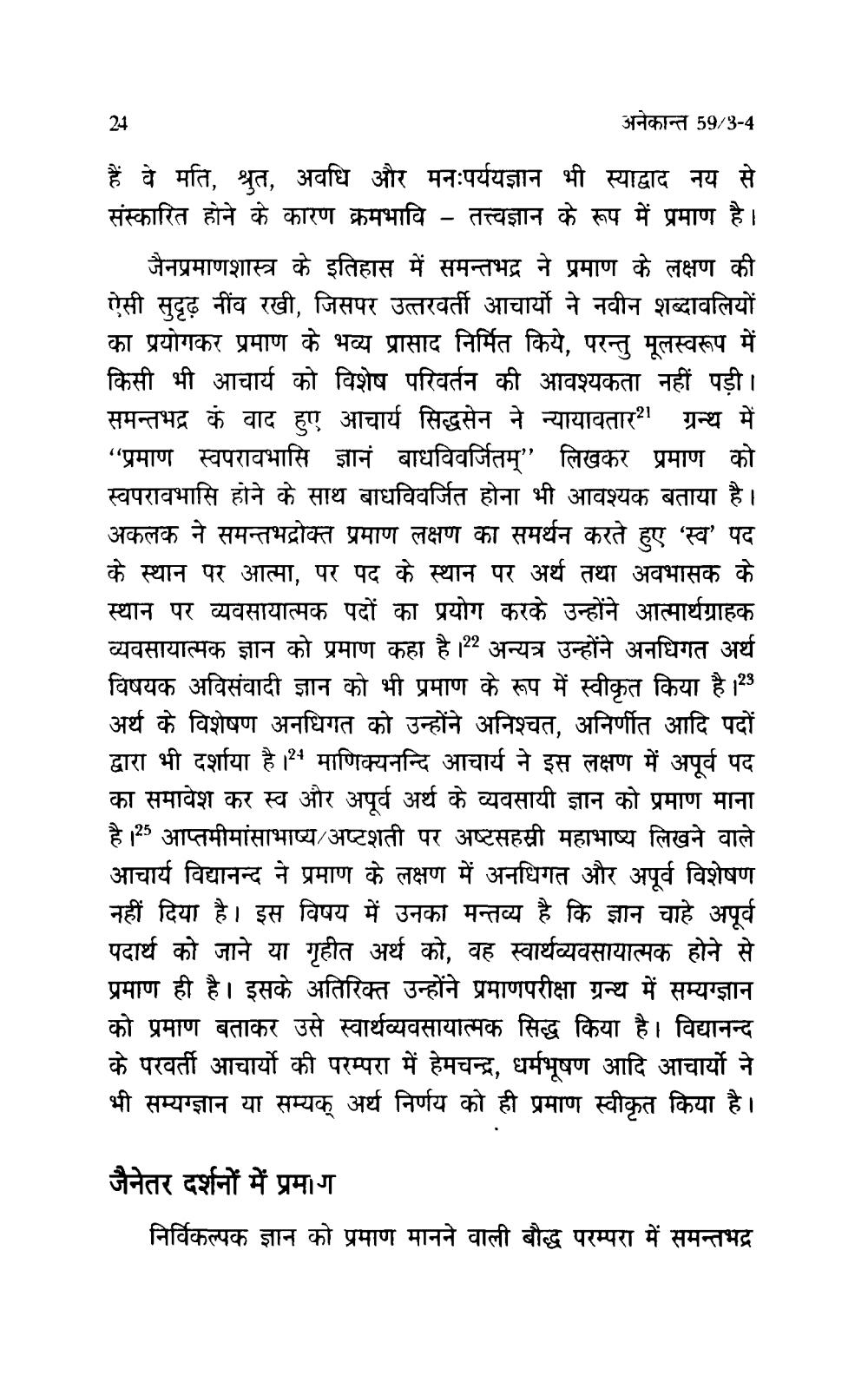________________
अनेकान्त 59/3-4
हैं वे मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययज्ञान भी स्याद्वाद नय से संस्कारित होने के कारण क्रमभावि - तत्त्वज्ञान के रूप में प्रमाण है।
जैनप्रमाणशास्त्र के इतिहास में समन्तभद्र ने प्रमाण के लक्षण की ऐसी सुदृढ़ नींव रखी, जिसपर उत्तरवर्ती आचार्यों ने नवीन शब्दावलियों का प्रयोगकर प्रमाण के भव्य प्रासाद निर्मित किये, परन्तु मूलस्वरूप में किसी भी आचार्य को विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। समन्तभद्र कं वाद हुए आचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार ग्रन्थ में "प्रमाण स्वपरावभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्" लिखकर प्रमाण को स्वपरावभासि होने के साथ बाधविवर्जित होना भी आवश्यक बताया है। अकलक ने समन्तभद्रोक्त प्रमाण लक्षण का समर्थन करते हुए 'स्व' पद के स्थान पर आत्मा, पर पद के स्थान पर अर्थ तथा अवभासक के स्थान पर व्यवसायात्मक पदों का प्रयोग करके उन्होंने आत्मार्थग्राहक व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा है।22 अन्यत्र उन्होंने अनधिगत अर्थ विषयक अविसंवादी ज्ञान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया है।23 अर्थ के विशेषण अनधिगत को उन्होंने अनिश्चत, अनिर्णीत आदि पदों द्वारा भी दर्शाया है। माणिक्यनन्दि आचार्य ने इस लक्षण में अपूर्व पद का समावेश कर स्व और अपूर्व अर्थ के व्यवसायी ज्ञान को प्रमाण माना है।25 आप्तमीमांसाभाष्य/अप्टशती पर अष्टसहस्री महाभाष्य लिखने वाले आचार्य विद्यानन्द ने प्रमाण के लक्षण में अनधिगत और अपूर्व विशेषण नहीं दिया है। इस विषय में उनका मन्तव्य है कि ज्ञान चाहे अपूर्व पदार्थ को जाने या गृहीत अर्थ को, वह स्वार्थव्यवसायात्मक होने से प्रमाण ही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रमाणपरीक्षा ग्रन्थ में सम्यग्ज्ञान को प्रमाण बताकर उसे स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है। विद्यानन्द के परवर्ती आचार्यो की परम्परा में हेमचन्द्र, धर्मभूषण आदि आचार्यों ने भी सम्यग्ज्ञान या सम्यक् अर्थ निर्णय को ही प्रमाण स्वीकृत किया है।
जैनेतर दर्शनों में प्रमाग निर्विकल्पक ज्ञान को प्रमाण मानने वाली बौद्ध परम्परा में समन्तभद्र