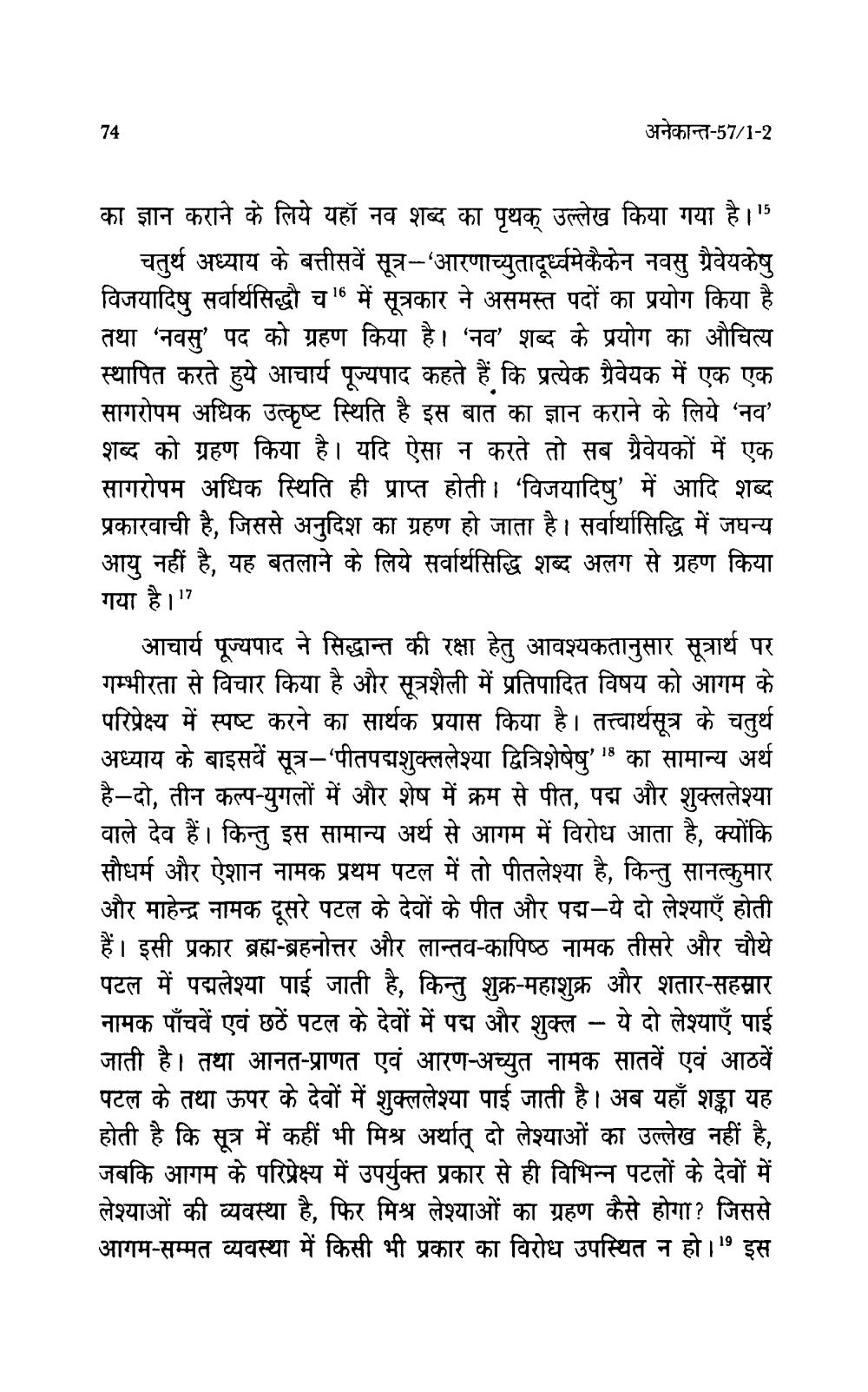________________
अनेकान्त-57/1-2
का ज्ञान कराने के लिये यहाँ नव शब्द का पृथक् उल्लेख किया गया है।
चतुर्थ अध्याय के बत्तीसवें सूत्र-'आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च में सूत्रकार ने असमस्त पदों का प्रयोग किया है तथा 'नवसु' पद को ग्रहण किया है। 'नव' शब्द के प्रयोग का औचित्य स्थापित करते हुये आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि प्रत्येक ग्रैवेयक में एक एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है इस बात का ज्ञान कराने के लिये 'नव' शब्द को ग्रहण किया है। यदि ऐसा न करते तो सब ग्रैवेयकों में एक सागरोपम अधिक स्थिति ही प्राप्त होती। 'विजयादिषु' में आदि शब्द प्रकारवाची है, जिससे अनुदिश का ग्रहण हो जाता है। सर्वार्थासिद्धि में जघन्य आय नहीं है, यह बतलाने के लिये सर्वार्थसिद्धि शब्द अलग से ग्रहण किया गया है।” ___ आचार्य पूज्यपाद ने सिद्धान्त की रक्षा हेतु आवश्यकतानुसार सूत्रार्थ पर गम्भीरता से विचार किया है और सूत्रशैली में प्रतिपादित विषय को आगम के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने का सार्थक प्रयास किया है। तत्त्वार्थसूत्र के चतुर्थ अध्याय के बाइसवें सूत्र- 'पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु' 18 का सामान्य अर्थ है-दो, तीन कल्प-युगलों में और शेष में क्रम से पीत, पद्म और शक्ललेश्या वाले देव हैं। किन्तु इस सामान्य अर्थ से आगम में विरोध आता है, क्योंकि सौधर्म और ऐशान नामक प्रथम पटल में तो पीतलेश्या है, किन्तु सानत्कुमार
और माहेन्द्र नामक दूसरे पटल के देवों के पीत और पद्म-ये दो लेश्याएँ होती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म-ब्रहनोत्तर और लान्तव-कापिष्ठ नामक तीसरे और चौथे पटल में पद्मलेश्या पाई जाती है, किन्तु शुक्र-महाशुक्र और शतार-सहस्रार नामक पाँचवें एवं छठे पटल के देवों में पद्य और शुक्ल - ये दो लेश्याएँ पाई जाती है। तथा आनत-प्राणत एवं आरण-अच्युत नामक सातवें एवं आठवें पटल के तथा ऊपर के देवों में शुक्ललेश्या पाई जाती है। अब यहाँ शङ्का यह होती है कि सत्र में कहीं भी मिश्र अर्थात दो लेश्याओं का उल्लेख नहीं है, जबकि आगम के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त प्रकार से ही विभिन्न पटलों के देवों में लेश्याओं की व्यवस्था है, फिर मिश्र लेश्याओं का ग्रहण कैसे होगा? जिससे आगम-सम्मत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विरोध उपस्थित न हो। इस