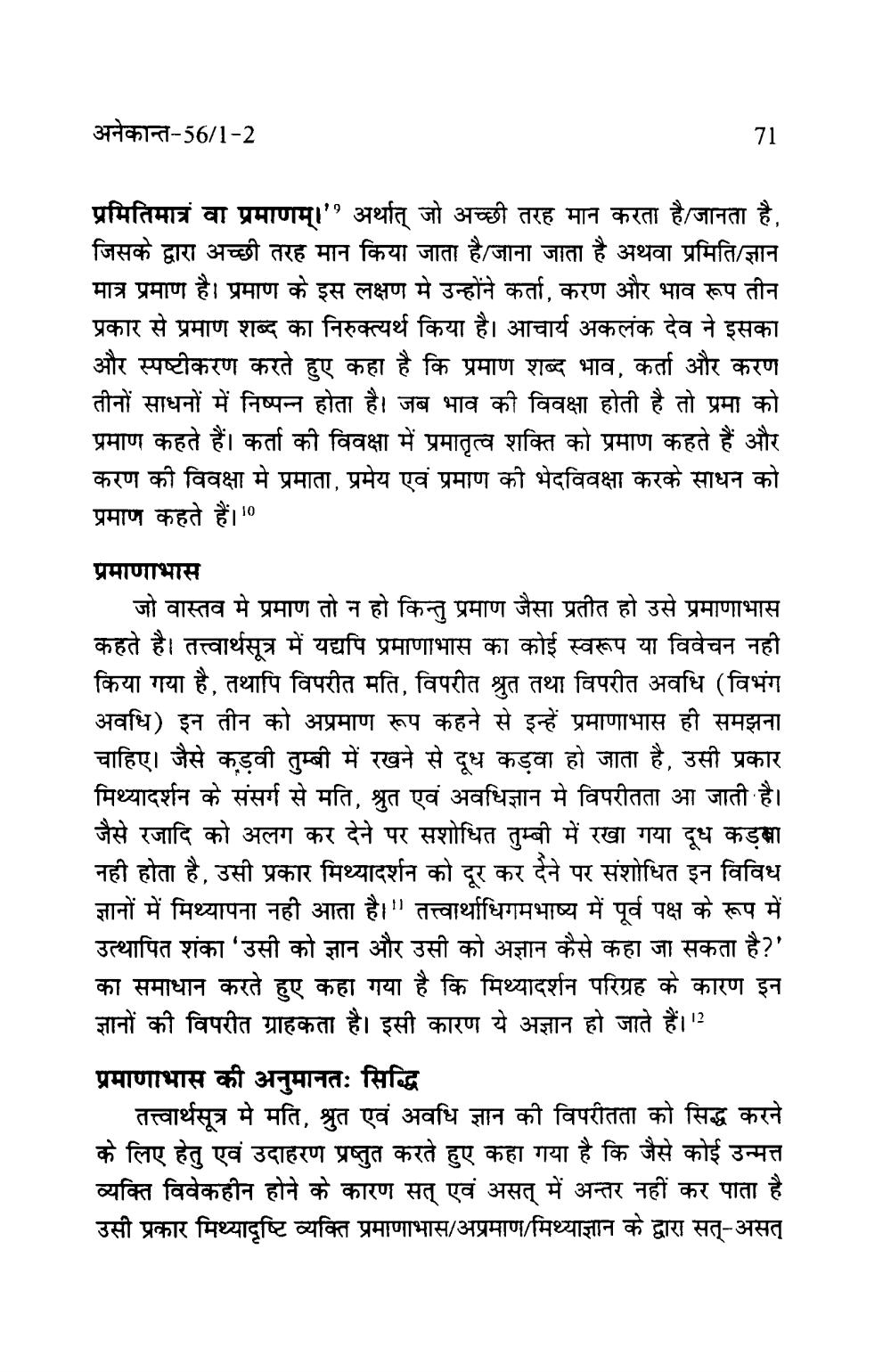________________
अनेकान्त-56/1-2
प्रमितिमात्र वा प्रमाणम्।'' अर्थात् जो अच्छी तरह मान करता है/जानता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है/जाना जाता है अथवा प्रमिति/ज्ञान मात्र प्रमाण है। प्रमाण के इस लक्षण मे उन्होंने कर्ता, करण और भाव रूप तीन प्रकार से प्रमाण शब्द का निरुक्त्यर्थ किया है। आचार्य अकलंक देव ने इसका
और स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्रमाण शब्द भाव, कर्ता और करण तीनों साधनों में निष्पन्न होता है। जब भाव की विवक्षा होती है तो प्रमा को प्रमाण कहते हैं। कर्ता की विवक्षा में प्रमातृत्व शक्ति को प्रमाण कहते हैं और करण की विवक्षा मे प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण की भेदविवक्षा करके साधन को प्रमाण कहते हैं।
प्रमाणाभास
जो वास्तव मे प्रमाण तो न हो किन्तु प्रमाण जैसा प्रतीत हो उसे प्रमाणाभास कहते है। तत्त्वार्थसूत्र में यद्यपि प्रमाणाभास का कोई स्वरूप या विवेचन नही किया गया है, तथापि विपरीत मति, विपरीत श्रुत तथा विपरीत अवधि (विभंग अवधि) इन तीन को अप्रमाण रूप कहने से इन्हें प्रमाणाभास ही समझना चाहिए। जैसे कड़वी तुम्बी में रखने से दूध कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादर्शन के संसर्ग से मति, श्रुत एवं अवधिज्ञान मे विपरीतता आ जाती है। जैसे रजादि को अलग कर देने पर सशोधित तुम्बी में रखा गया दूध कड़बा नही होता है, उसी प्रकार मिथ्यादर्शन को दूर कर देने पर संशोधित इन विविध ज्ञानों में मिथ्यापना नही आता है। तत्त्वार्थाधिगमभाष्य में पूर्व पक्ष के रूप में उत्थापित शंका 'उसी को ज्ञान और उसी को अज्ञान कैसे कहा जा सकता है?' का समाधान करते हुए कहा गया है कि मिथ्यादर्शन परिग्रह के कारण इन ज्ञानों की विपरीत ग्राहकता है। इसी कारण ये अज्ञान हो जाते हैं। 12
प्रमाणाभास की अनुमानतः सिद्धि
तत्त्वार्थसूत्र मे मति, श्रुत एवं अवधि ज्ञान की विपरीतता को सिद्ध करने के लिए हेतु एवं उदाहरण प्रष्तुत करते हुए कहा गया है कि जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति विवेकहीन होने के कारण सत् एवं असत् में अन्तर नहीं कर पाता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि व्यक्ति प्रमाणाभास/अप्रमाण/मिथ्याज्ञान के द्वारा सत्-असत्