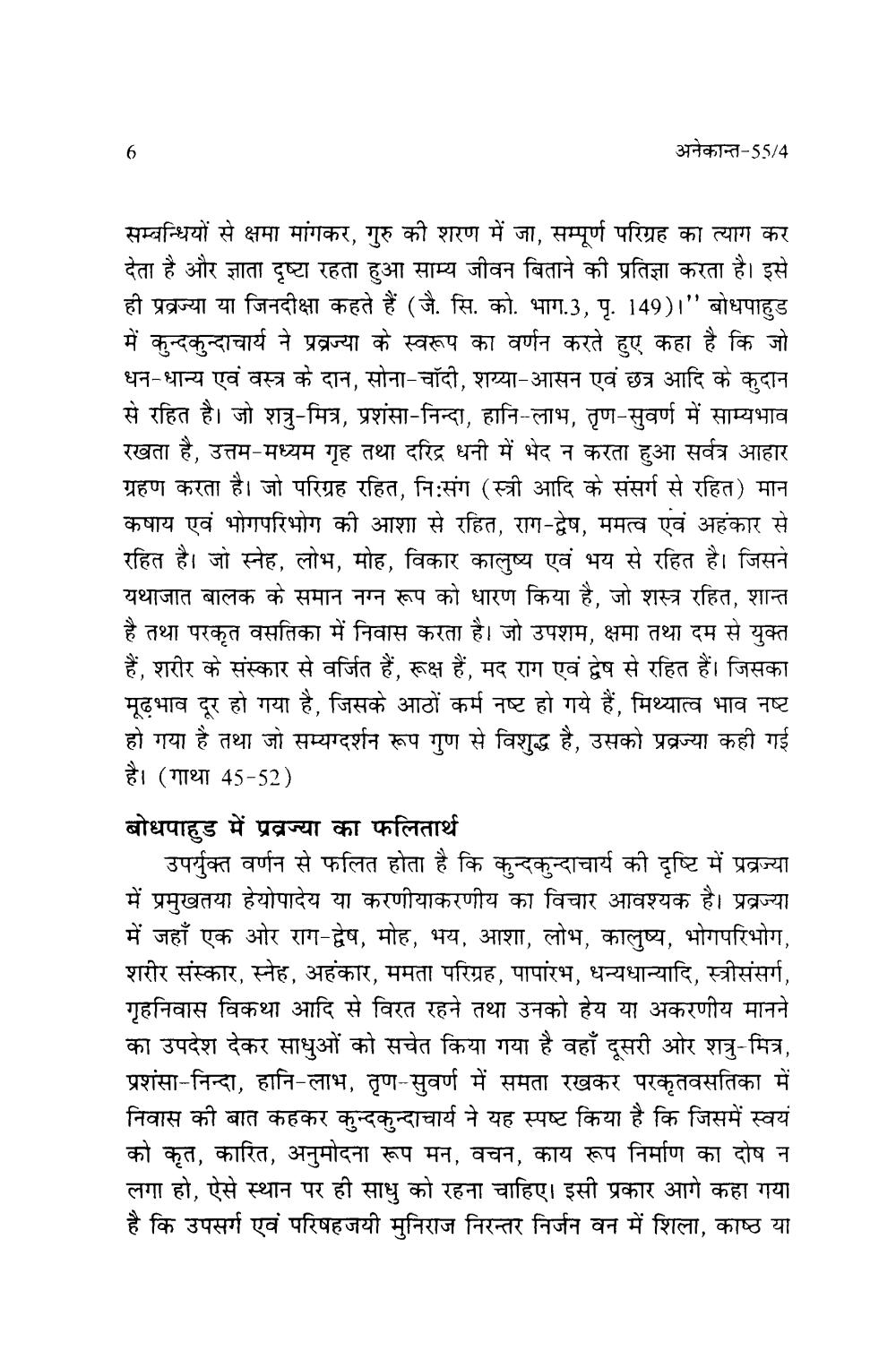________________
6
अनेकान्त-55/4
सम्बन्धियों से क्षमा मांगकर, गुरु की शरण में जा, सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर देता है और ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ साम्य जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करता है। इसे ही प्रव्रज्या या जिनदीक्षा कहते हैं (जै. सि. को. भाग. 3, पृ. 149 ) । " बोधपाहुड में कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रव्रज्या के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि जो धन-धान्य एवं वस्त्र के दान, सोना-चाँदी, शय्या - आसन एवं छत्र आदि के कुदान से रहित है। जो शत्रु - मित्र, प्रशंसा - निन्दा, हानि-लाभ, तृण- सुवर्ण में साम्यभाव रखता है, उत्तम - मध्यम गृह तथा दरिद्र धनी में भेद न करता हुआ सर्वत्र आहार ग्रहण करता है। जो परिग्रह रहित, निःसंग (स्त्री आदि के संसर्ग से रहित ) मान कषाय एवं भोगपरिभोग की आशा से रहित, राग-द्वेष, ममत्व एवं अहंकार से रहित है। जो स्नेह, लोभ, मोह, विकार कालुष्य एवं भय से रहित है। जिसने यथाजात बालक के समान नग्न रूप को धारण किया है, जो शस्त्र रहित, शान्त है तथा परकृत वसतिका में निवास करता है। जो उपशम, क्षमा तथा दम से युक्त हैं, शरीर के संस्कार से वर्जित हैं, रूक्ष हैं, मद राग एवं द्वेष से रहित हैं। जिसका मूढ़ भाव दूर हो गया है, जिसके आठों कर्म नष्ट हो गये हैं, मिथ्यात्व भाव नष्ट हो गया है तथा जो सम्यग्दर्शन रूप गुण से विशुद्ध है, उसको प्रव्रज्या कही गई है। (गाथा 45-52)
है।
बोधपाहुड में प्रव्रज्या का फलितार्थ
उपर्युक्त वर्णन से फलित होता है कि कुन्दकुन्दाचार्य की दृष्टि में प्रव्रज्या में प्रमुखतया हेयोपादेय या करणीयाकरणीय का विचार आवश्यक है। प्रव्रज्या में जहाँ एक ओर राग- - द्वेष, मोह, भय, आशा, लोभ, कालुष्य, भोगपरिभोग, शरीर संस्कार, स्नेह, अहंकार, ममता परिग्रह, पापांरंभ, धन्यधान्यादि, स्त्रीसंसर्ग, गृहनिवास विकथा आदि से विरत रहने तथा उनको हेय या अकरणीय मानने का उपदेश देकर साधुओं को सचेत किया गया है वहाँ दूसरी ओर शत्रु-मित्र, प्रशंसा - निन्दा, हानि-लाभ, तृण- सुवर्ण में समता रखकर परकृतवसतिका में निवास की बात कहकर कुन्दकुन्दाचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि जिसमें स्वयं को कृत, कारित, अनुमोदना रूप मन, वचन, काय रूप निर्माण का दोष न लगा हो, ऐसे स्थान पर ही साधु को रहना चाहिए। इसी प्रकार आगे कहा गया है कि उपसर्ग एवं परिषहजयी मुनिराज निरन्तर निर्जन वन में शिला, काष्ठ या