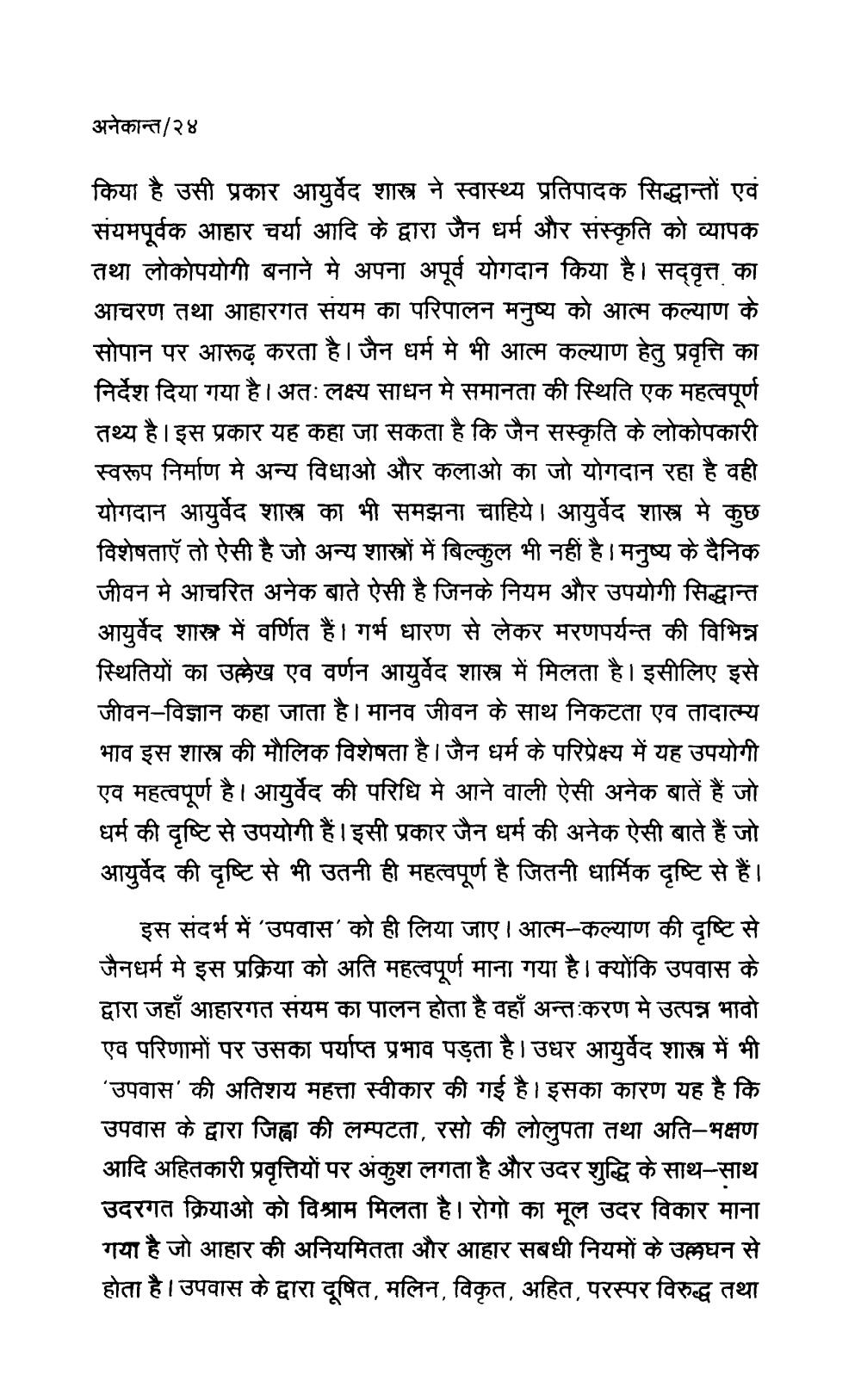________________
अनेकान्त/२४
किया है उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र ने स्वास्थ्य प्रतिपादक सिद्धान्तों एवं संयमपूर्वक आहार चर्या आदि के द्वारा जैन धर्म और संस्कृति को व्यापक तथा लोकोपयोगी बनाने में अपना अपूर्व योगदान किया है। सद्वृत्त का आचरण तथा आहारगत संयम का परिपालन मनुष्य को आत्म कल्याण के सोपान पर आरूढ़ करता है। जैन धर्म मे भी आत्म कल्याण हेतु प्रवृत्ति का निर्देश दिया गया है। अतः लक्ष्य साधन मे समानता की स्थिति एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जैन सस्कृति के लोकोपकारी स्वरूप निर्माण मे अन्य विधाओ और कलाओ का जो योगदान रहा है वही योगदान आयुर्वेद शास्त्र का भी समझना चाहिये। आयुर्वेद शास्त्र मे कुछ विशेषताएँ तो ऐसी है जो अन्य शास्त्रों में बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य के दैनिक जीवन मे आचरित अनेक बाते ऐसी है जिनके नियम और उपयोगी सिद्धान्त आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित हैं। गर्भ धारण से लेकर मरणपर्यन्त की विभिन्न स्थितियों का उल्लेख एव वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है। इसीलिए इसे जीवन-विज्ञान कहा जाता है। मानव जीवन के साथ निकटता एव तादात्म्य भाव इस शास्त्र की मौलिक विशेषता है। जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में यह उपयोगी एव महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद की परिधि मे आने वाली ऐसी अनेक बातें हैं जो धर्म की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसी प्रकार जैन धर्म की अनेक ऐसी बाते हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी धार्मिक दृष्टि से हैं।
इस संदर्भ में 'उपवास' को ही लिया जाए । आत्म-कल्याण की दृष्टि से जैनधर्म मे इस प्रक्रिया को अति महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि उपवास के द्वारा जहाँ आहारगत संयम का पालन होता है वहाँ अन्तःकरण मे उत्पन्न भावो एव परिणामों पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उधर आयुर्वेद शास्त्र में भी 'उपवास' की अतिशय महत्ता स्वीकार की गई है। इसका कारण यह है कि उपवास के द्वारा जिह्वा की लम्पटता, रसो की लोलुपता तथा अति-भक्षण आदि अहितकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है और उदर शुद्धि के साथ-साथ उदरगत क्रियाओ को विश्राम मिलता है। रोगो का मूल उदर विकार माना गया है जो आहार की अनियमितता और आहार सबधी नियमों के उल्लघन से होता है। उपवास के द्वारा दूषित, मलिन, विकृत, अहित, परस्पर विरुद्ध तथा