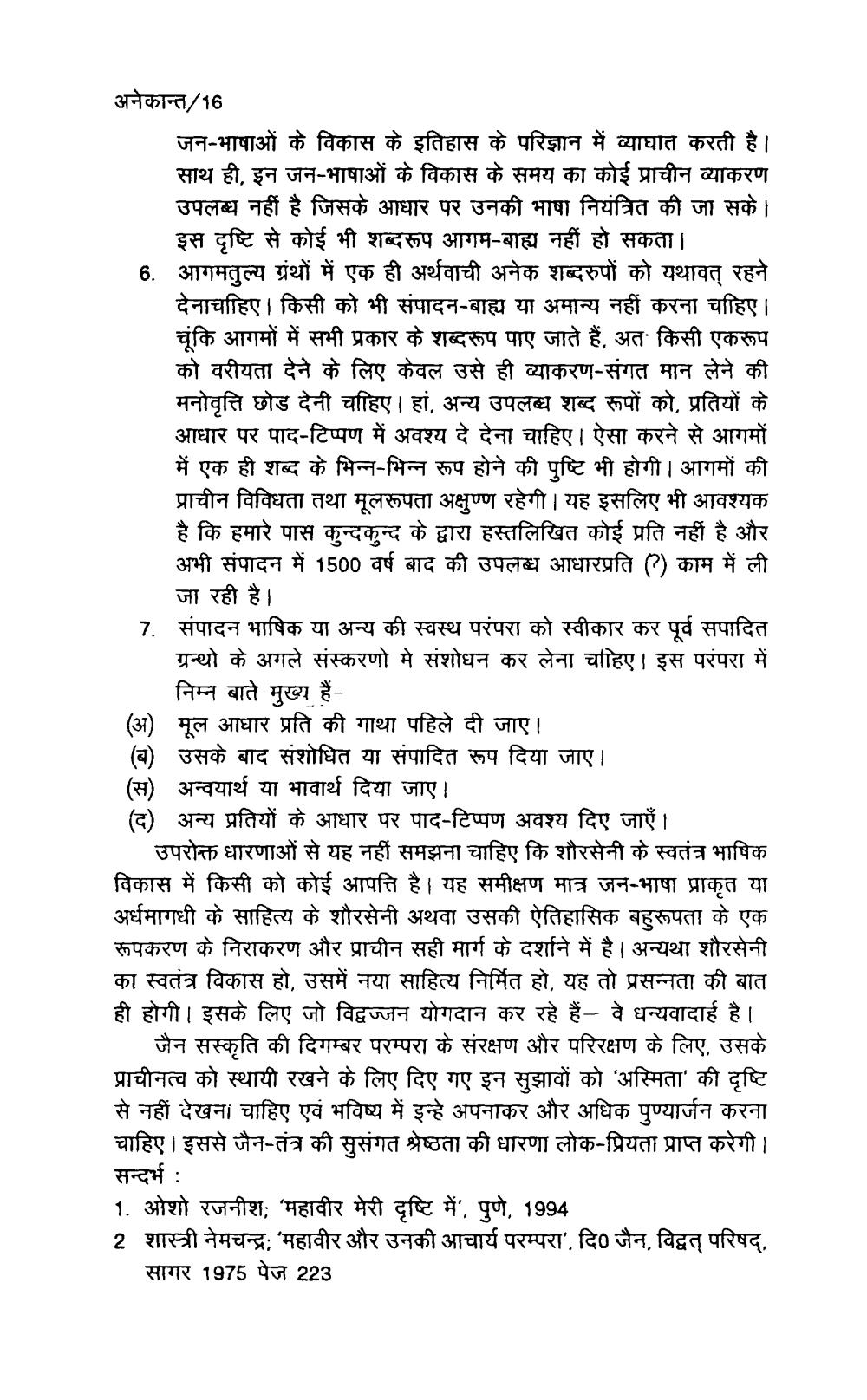________________
अनेकान्त/16
जन-भाषाओं के विकास के इतिहास के परिज्ञान में व्याघात करती है। साथ ही, इन जन-भाषाओं के विकास के समय का कोई प्राचीन व्याकरण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उनकी भाषा नियंत्रित की जा सके।
इस दृष्टि से कोई भी शब्दरूप आगम-बाह्य नहीं हो सकता। 6. आगमतुल्य ग्रंथों में एक ही अर्थवाची अनेक शब्दरुपों को यथावत् रहने
देनाचाहिए। किसी को भी संपादन-बाह्य या अमान्य नहीं करना चाहिए। चूंकि आगमों में सभी प्रकार के शब्दरूप पाए जाते हैं, अत: किसी एकरूप को वरीयता देने के लिए केवल उसे ही व्याकरण-संगत मान लेने की मनोवृत्ति छोड देनी चाहिए। हां, अन्य उपलब्ध शब्द रूपों को, प्रतियों के आधार पर पाद-टिप्पण में अवश्य दे देना चाहिए। ऐसा करने से आगमों में एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न रूप होने की पुष्टि भी होगी। आगमों की प्राचीन विविधता तथा मूलरूपता अक्षुण्ण रहेगी। यह इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे पास कुन्दकुन्द के द्वारा हस्तलिखित कोई प्रति नहीं है और अभी संपादन में 1500 वर्ष बाद की उपलब्ध आधारप्रति (2) काम में ली
जा रही है। 7. संपादन भाषिक या अन्य की स्वस्थ परंपरा को स्वीकार कर पूर्व सपादित
ग्रन्थो के अगले संस्करणो मे संशोधन कर लेना चाहिए। इस परंपरा में
निम्न बाते मुख्य हैं(अ) मूल आधार प्रति की गाथा पहिले दी जाए। (ब) उसके बाद संशोधित या संपादित रूप दिया जाए। (स) अन्वयार्थ या भावार्थ दिया जाए। (द) अन्य प्रतियों के आधार पर पाद-टिप्पण अवश्य दिए जाएँ।
उपरोक्त धारणाओं से यह नहीं समझना चाहिए कि शौरसेनी के स्वतंत्र भाषिक विकास में किसी को कोई आपत्ति है। यह समीक्षण मात्र जन-भाषा प्राकृत या अर्धमागधी के साहित्य के शौरसेनी अथवा उसकी ऐतिहासिक बहुरूपता के एक रूपकरण के निराकरण और प्राचीन सही मार्ग के दर्शाने में है। अन्यथा शौरसेनी का स्वतंत्र विकास हो, उसमें नया साहित्य निर्मित हो, यह तो प्रसन्नता की बात ही होगी। इसके लिए जो विद्वज्जन योगदान कर रहे हैं- वे धन्यवादाह है।
जैन सस्कृति की दिगम्बर परम्परा के संरक्षण और परिरक्षण के लिए, उसके प्राचीनत्व को स्थायी रखने के लिए दिए गए इन सुझावों को 'अस्मिता' की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए एवं भविष्य में इन्हे अपनाकर और अधिक पुण्यार्जन करना चाहिए। इससे जैन-तंत्र की सुसंगत श्रेष्ठता की धारणा लोक-प्रियता प्राप्त करेगी। सन्दर्भ : 1. ओशो रजनीश; 'महावीर मेरी दृष्टि में', पुणे, 1994 2 शास्त्री नेमचन्द्र; 'महावीर और उनकी आचार्य परम्परा', दि० जैन, विद्वत् परिषद्,
सागर 1975 पेज 223