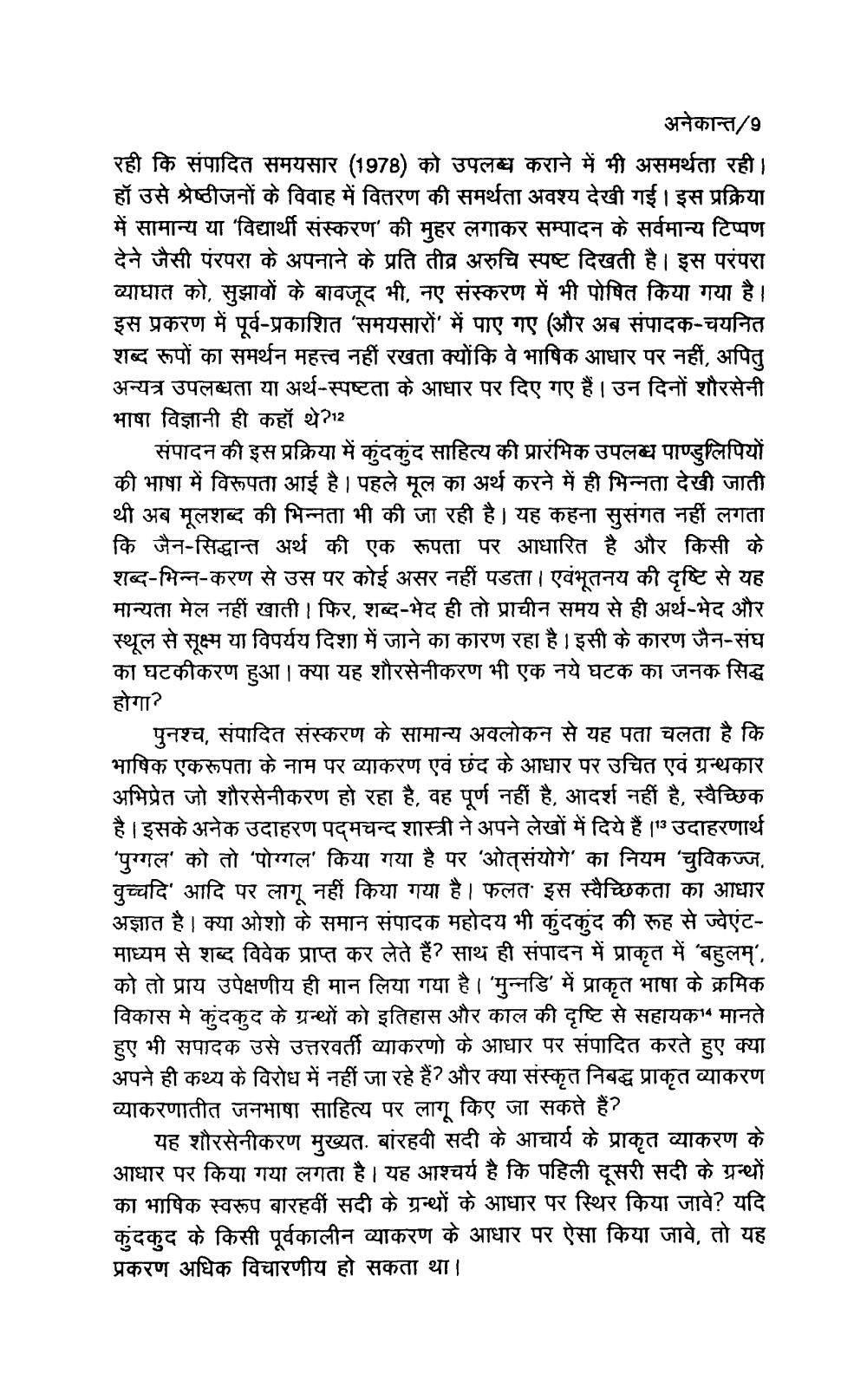________________
अनेकान्त / 9 रही कि संपादित समयसार (1978) को उपलब्ध कराने में भी असमर्थता रही। हॉ उसे श्रेष्ठीजनों के विवाह में वितरण की समर्थता अवश्य देखी गई। इस प्रक्रिया में सामान्य या 'विद्यार्थी संस्करण' की मुहर लगाकर सम्पादन के सर्वमान्य टिप्पण देने जैसी पंरपरा के अपनाने के प्रति तीव्र अरुचि स्पष्ट दिखती है। इस परंपरा व्याघात को, सुझावों के बावजूद भी नए संस्करण में भी पोषित किया गया है। इस प्रकरण में पूर्व - प्रकाशित 'समयसारों' में पाए गए (और अब संपादक- चयनित शब्द रूपों का समर्थन महत्त्व नहीं रखता क्योंकि वे भाषिक आधार पर नहीं, अपितु अन्यत्र उपलब्धता या अर्थ स्पष्टता के आधार पर दिए गए हैं। उन दिनों शौरसेनी भाषा विज्ञानी ही कहाँ थे? 12
संपादन की इस प्रक्रिया में कुंदकुंद साहित्य की प्रारंभिक उपलब्ध पाण्डुलिपियों की भाषा में विरूपता आई है। पहले मूल का अर्थ करने में ही भिन्नता देखी जाती थी अब मूलशब्द की भिन्नता भी की जा रही है। यह कहना सुसंगत नहीं लगता कि जैन- सिद्धान्त अर्थ की एक रूपता पर आधारित है और किसी के शब्द- भिन्न-करण से उस पर कोई असर नहीं पडता । एवंभूतनय की दृष्टि से यह मान्यता मेल नहीं खाती। फिर, शब्द-भेद ही तो प्राचीन समय से ही अर्थ-भेद और स्थूल से सूक्ष्म या विपर्यय दिशा में जाने का कारण रहा है। इसी के कारण जैन संघ का घटकीकरण हुआ। क्या यह शौरसेनीकरण भी एक नये घटक का जनक सिद्ध होगा?
पुनश्च, संपादित संस्करण के सामान्य अवलोकन से यह पता चलता है कि भाषिक एकरूपता के नाम पर व्याकरण एवं छंद के आधार पर उचित एवं ग्रन्थकार अभिप्रेत जो शौरसेनीकरण हो रहा है, वह पूर्ण नहीं है, आदर्श नहीं है, स्वैच्छिक है। इसके अनेक उदाहरण पद्मचन्द शास्त्री ने अपने लेखों में दिये हैं। उदाहरणार्थ 'पुग्गल' को तो 'पोग्गल' किया गया है पर 'ओत्संयोगे' का नियम 'चुविकज्ज. वुच्चदि' आदि पर लागू नहीं किया गया है। फलत इस स्वैच्छिकता का आधार अज्ञात है। क्या ओशो के समान संपादक महोदय भी कुंदकुंद की रूह से ज्वेएंटमाध्यम से शब्द विवेक प्राप्त कर लेते हैं? साथ ही संपादन में प्राकृत में 'बहुलम्', को तो प्राय उपेक्षणीय ही मान लिया गया है। 'मुन्नडि' में प्राकृत भाषा के क्रमिक विकास मे कुंदकुद के ग्रन्थों को इतिहास और काल की दृष्टि से सहायक " मानते हुए भी सपादक उसे उत्तरवर्ती व्याकरणो के आधार पर संपादित करते हुए क्या अपने ही कथ्य के विरोध में नहीं जा रहे हैं? और क्या संस्कृत निबद्ध प्राकृत व्याकरण व्याकरणातीत जनभाषा साहित्य पर लागू किए जा सकते हैं?
यह शौरसेनीकरण मुख्यत. बारहवी सदी के आचार्य के प्राकृत व्याकरण के आधार पर किया गया लगता है। यह आश्चर्य है कि पहिली दूसरी सदी के ग्रन्थों का भाषिक स्वरूप बारहवीं सदी के ग्रन्थों के आधार पर स्थिर किया जावे? यदि कुंदकुद के किसी पूर्वकालीन व्याकरण के आधार पर ऐसा किया जावे, तो यह प्रकरण अधिक विचारणीय हो सकता था ।