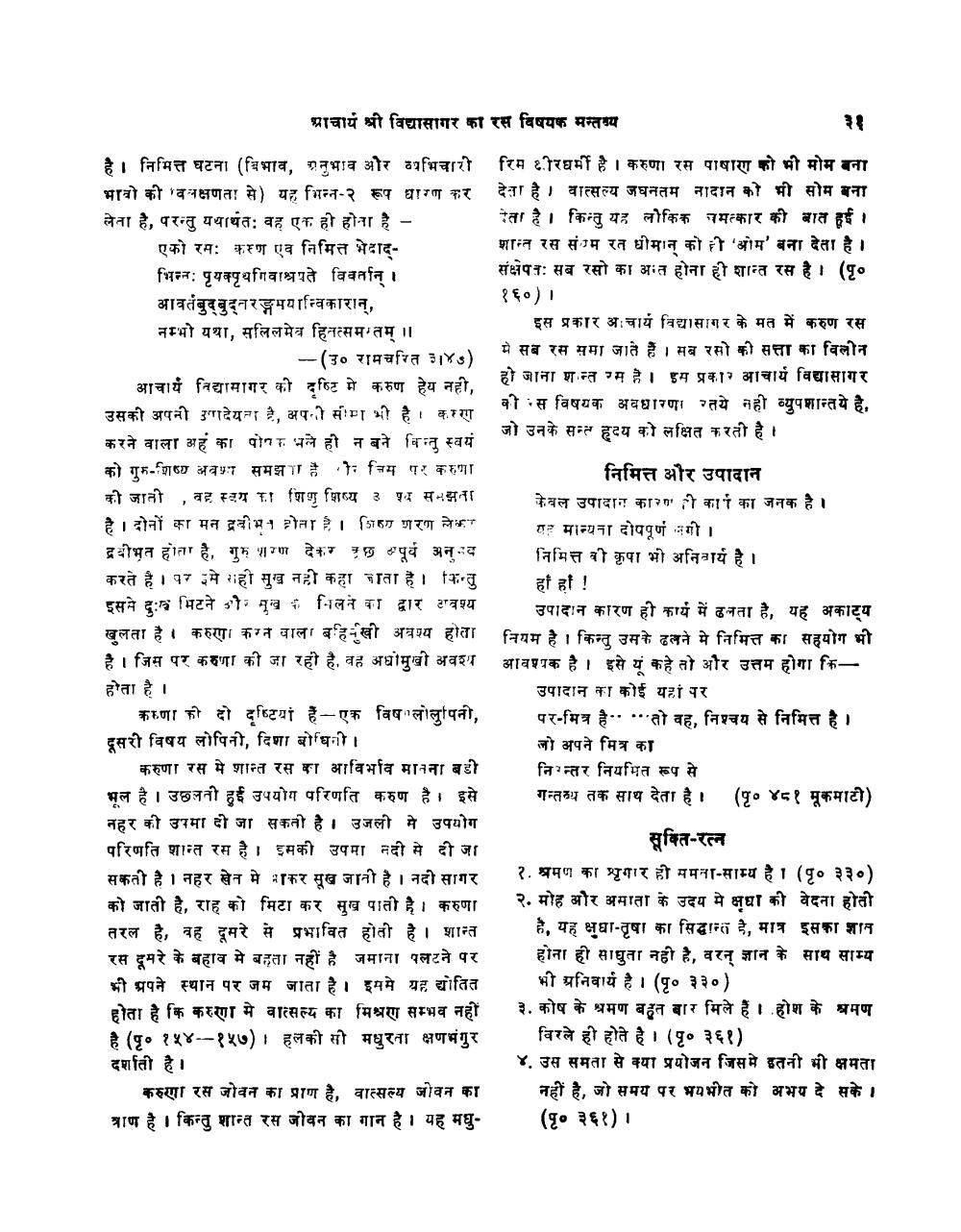________________
प्राचार्य श्री विद्यासागर का रस विषयक मन्तव्य
है। निमित्त घटना (बिभाव, गानुभाव और व्यभिचारी रिम धीरधर्मी है । करुणा रस पाषाण को भी मोम बना भावो की विलक्षणता से) यह भिन्न-२ रूप धारण कर देता है। वात्सल्य जघनतम नादान को भी सोम बना लेता है, परन्तु यथार्थत: वह एक ही होता है -
देता है। किन्तु यह लोकिक चमत्कार की बात हुई। एको रमः करण एव निमित्त भेदाद
शान्त रस संगम रत धीमान कोही 'ओम' बना देता है। भिन्न: पृथक्पृथगिवाश्रपते विवर्तान् ।
संक्षेपत: सब रसो का आत होना ही शान्त रस है। (पृ. आवर्तबुद्बुद्तरङ्गमयान्विकारान्,
१६०)। नम्भो यथा, सलिलमेव हितत्सम तम् ।।
इस प्रकार आचार्य विद्यासागर के मत में करुण रस -(उ० रामचरित ३।४७)
मे सब रस समा जाते हैं । सब रसो की सत्ता का विलीन आचार्य विद्यामागर की दृष्टि मे करुण हेय नही,
हो जाना शन्त म है। इस प्रकार आचार्य विद्यासागर
की स विषयक अवधारणा रतये नही व्युपशान्तये है, उसकी अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा भी है। करण ।
जो उनके सन्त हृदय को लक्षित करती है। करने वाला अहं का पोषक भले ही न बने विन्तु स्वयं को गुरु-शिष्य अवशा समझा है और निम पर करुणा
निमित्त और उपादान की जाती , वह स्वयका शिशु शिष्य ३ च समझता
के बल उपादान कारी का का जनक है। है । दोनों का मन द्रवीभ होता है। जिय शरण लेकर
राः मान्यता दोषपूर्ण जगी। द्रवीभूत होता है, गुरु शरण देकर नछ अपूर्व अनुभव
निमित्त वी कृपा भी अनिवार्य है। करते है । पर इसे सही सुख नही कहा जाता है। किन्तु इसने दु:ख मिटने और मुखक मिलने का द्वार अवश्य
उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य खुलता है। करुणा करने वाला बहिखी अवश्य होता।
नियम है । किन्तु उसके ढलने मे निमित्त का सहयोग भी है। जिस पर करुणा की जा रही है, वह अधोमुखी अवश्य आवश्यक है। इसे यूं कहे तो और उत्तम होगा किहोता है ।
उपादान का कोई यहां पर करुणा को दो दृष्टियां हैं-एक विषालोलुपिनी,
पर-मित्र है.. .."तो वह, निश्चय से निमित्त है। दूसरी विषय लोपिनी, दिशा बोधिनी।
जो अपने मित्र का करुणा रस मे शान्त रस का आविर्भाव मानना बडी निरन्तर नियमित रूप से भल है । उछलती हुई उपयोग परिणति करुण है। इसे गन्तव्य तक साथ देता है। (पृ० ४८१ मूकमाटी) नहर की उपमा दी जा सकती है। उजली मे उपयोग
सूक्ति-रत्न परिणति शान्त रस है। इसकी उपमा नदी से दी जा सकती है। नहर खेत मे भाकर सूख जाती है । नदी सागर
१. श्रमण का शृगार ही ममना-साम्य है । (पृ० ३३०) को जाती है, राह को मिटा कर सुख पाती है। करुणा
२. मोह और अमाता के उदय मे क्षुधा की वेदना होती तरल है, वह दूसरे से प्रभावित होती है। शान्त है, यह क्षुधा-तृषा का सिद्धान्त है, मात्र इसका ज्ञान रस दूसरे के बहाव मे बहता नहीं है जमाना पलटने पर होना ही साधुता नही है, वरन् ज्ञान के साथ साम्य भी अपने स्थान पर जम जाता है। इसमे यह द्योतित भी अनिवार्य है। (पृ० ३३०) होता है कि करुणा मे वात्सल्य का मिश्रण सम्भव नहीं ३. कोष के श्रमण बहुत बार मिले हैं। होश के श्रमण है (पृ. १५४--१५७)। हलकी सी मधुरता क्षणभंगुर विरले ही होते है। (पृ० ३६१) दर्शाती है।
४. उस समता से क्या प्रयोजन जिसमे इतनी भी क्षमता करुणा रस जोवन का प्राण है, वात्सल्य जीवन का नहीं है, जो समय पर भयभीत को अभय दे सके । बाण है । किन्तु शान्त रस जीवन का गान है। यह मधु- (पृ. ३६१)।