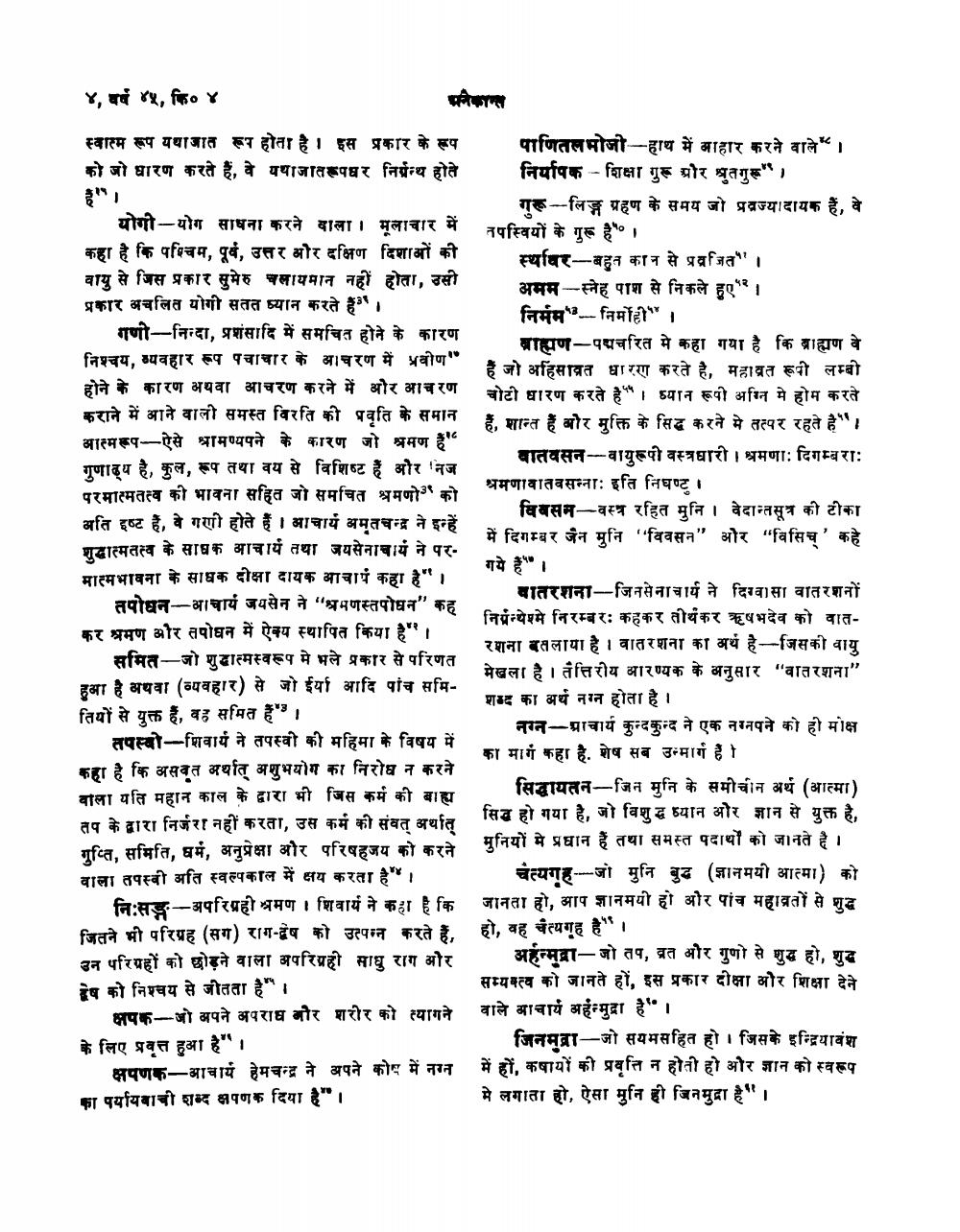________________
४, वर्ष ४५, कि०४
अनेकान्त
स्वात्म रूप यथाजात रूप होता है। इस प्रकार के रूप पाणितलमोजी-हाथ में हार करने वाले" । को जो धारण करते हैं, वे यथाजातरूपधर निर्ग्रन्थ होते निर्यापक-शिक्षा गुरू और श्रुतगुरू",
गरू--लिङ्ग ग्रहण के समय जो प्रव्रज्यादायक हैं, वे योगी-योग साधना करने वाला। मूलाचार में
तपस्वियों के गुरू है। कहा है कि पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की
स्थावर-बहुत कान से प्रवजित'। वायु से जिस प्रकार सुमेरु चलायमान नहीं होता, उसी
अमम-स्नेह पाश से निकले हुए। प्रकार अचलित योगी सतत ध्यान करते हैं।
निर्मम-निर्मोही । गणी-निन्दा, प्रशंसादि में समचित होने के कारण
ब्राह्मण-पपचरित मे कहा गया है कि ब्राह्मण वे निश्चय, व्यवहार रूप पचाचार के आचरण में प्रवीण"
हैं जो अहिंसावत धारण करते है, महाव्रत रूपी लम्बी होने के कारण अथवा आचरण करने में और आचरण
चोटी धारण करते है। ध्यान रूपी अग्नि मे होम करते कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृति के समान
हैं, शान्त हैं और मुक्ति के सिद्ध करने मे तत्पर रहते है। आत्मरूप-ऐसे श्रामण्यपने के कारण जो श्रमण है।" गुणाढ्य है, कुल, रूप तथा वय से विशिष्ट हैं और नज
बातवसन-वायुरूपी वस्त्रधारी। श्रमणा: दिगम्बरा: परमात्मतत्व की भावना सहित जो समचित श्रमणो को श्रमणावातवसन्नाः इति निघण्टु ।
विवसम-वस्त्र रहित मुनि । वेदान्तसूत्र की टीका अति इष्ट हैं, वे गणी होते हैं । आचार्य अमृतचन्द्र ने इन्हें
में दिगम्बर जैन मुनि “विवसन" और "विसिच्' कहे शूद्धात्मतत्व के साधक आचार्य तथा जयसेनाचार्य ने पर. मात्मभावना के साधक दीक्षा दायक आचार्य कहा है।
गये हैं। तपोधन-आचार्य जयसेन ने "श्रमणस्तपोधन" कह
वातरशना-जिनसेनाचार्य ने दिग्वासा वातरशनों
निग्रंन्थेश्मे निरम्बरः कहकर तीर्थंकर ऋषभदेव को वातकर श्रमण और तपोधन में ऐक्य स्थापित किया है।
रशना बसलाया है । वातरशना का अर्थ है-जिसकी वायु समित-जो शुद्धात्मस्वरूप मे भले प्रकार से परिणत
मेखला है । तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार “वात रशना" हुआ है अथवा (व्यवहार) से जो ईर्या आदि पांच समि
शब्द का अर्थ नग्न होता है। तियों से युक्त हैं, वह समित हैं।
नग्न-प्राचार्य कुन्दकुन्द ने एक नग्नपने को ही मोक्ष तपस्वी-शिवार्य ने तपस्वी की महिमा के विषय में
का मार्ग कहा है. शेष सब उन्मार्ग है। कहा है कि असवत अर्थात् अशुभयोग का निरोध न करने वाला यति महान काल के द्वारा भी जिस कर्म की बाह्य
सिद्धायतन-जिन मुनि के समीचीन अर्थ (आत्मा) तप के द्वारा निर्जरा नहीं करता, उस कर्म की संवत् अर्थात्
सिद्ध हो गया है, जो विशुद्ध ध्यान और ज्ञान से युक्त है, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिषहजय को करने मुनियों में प्रधान हैं तथा समस्त पदार्थों को जानते है । वाला तपस्वी अति स्वल्पकाल में क्षय करता है"।
चैत्यगह-जो मुनि बुद्ध (ज्ञानमयी आत्मा) को नि:सङ्कः-अपरिग्रही श्रमण । शिवार्य ने कहा है कि जानता हो, आप ज्ञानमयी हो और पांच महाव्रतों से शुद्ध जितने भी परिग्रह (सग) राग-द्वेष को उत्पन्न करते हैं, हो, वह चैत्यगह है"। उन परिग्रहों को छोड़ने वाला अपरिग्रही साधु राग और अहंन्मुद्रा-जो तप, व्रत और गुणो से शुद्ध हो, शुद्ध देष को निश्चय से जीतता है।
सम्यक्त्व को जानते हों, इस प्रकार दीक्षा और शिक्षा देने क्षपक-जो अपने अपराध और शरीर को त्यागने वाले आचार्य अहन्मुद्रा है। के लिए प्रवृत्त हुआ है"।
जिनमत्रा-जो सयमसहित हो। जिसके इन्द्रियावंश क्षपणक-आचार्य हेमचन्द्र ने अपने कोष में नग्न में हों, कषायों की प्रवृत्ति न होती हो और ज्ञान को स्वरूप का पर्यायवाची शब्द क्षपणक दिया है"।
मे लगाता हो, ऐसा मुनि ही जिनमुद्रा है"।