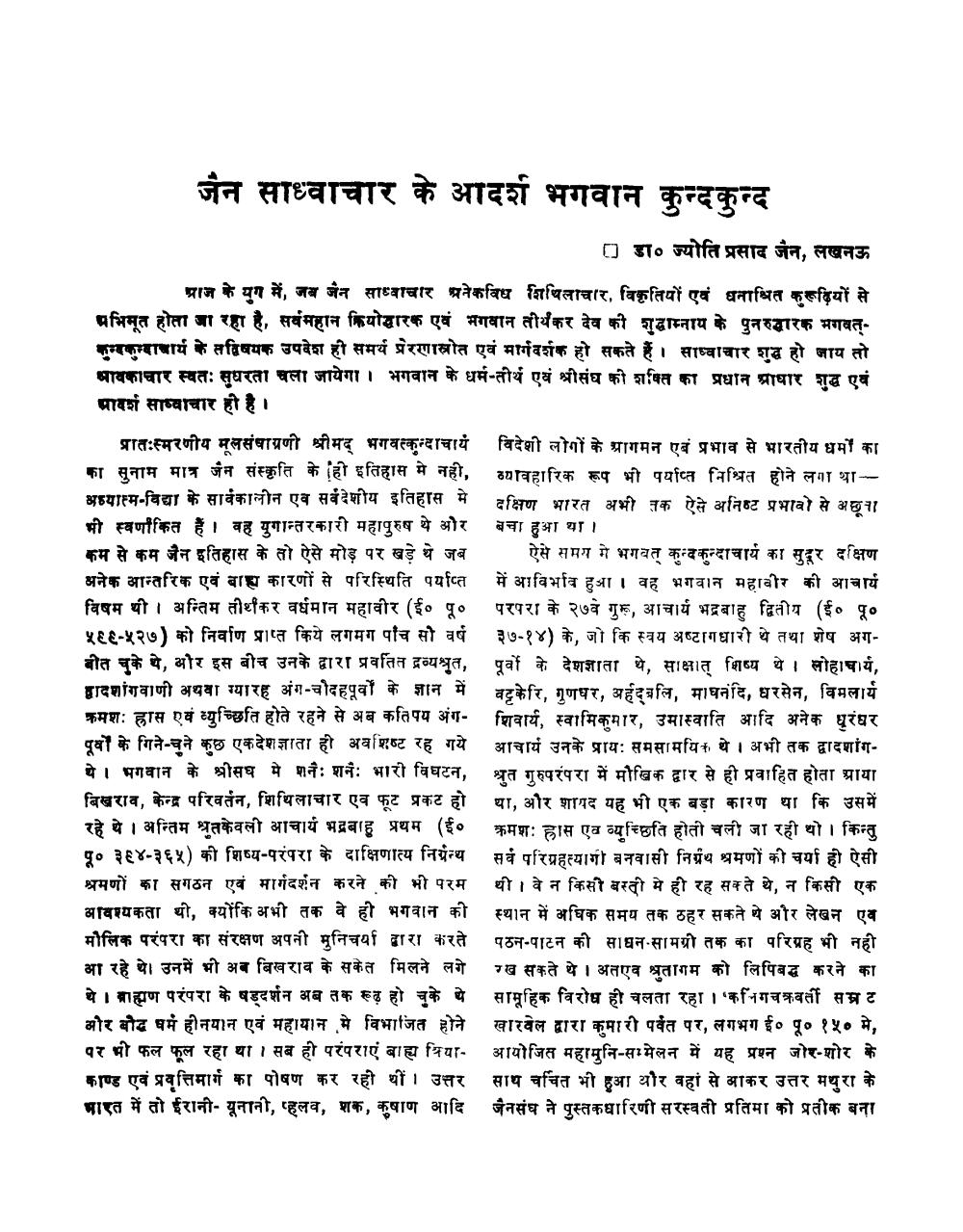________________
जैन साध्वाचार के आदर्श भगवान कुन्दकुन्द
डाज्योति प्रसाद जैन, लखनऊ
प्राज के युग में, जब जैन साध्वाचार अनेकविध शिथिलाचार, विकृतियों एवं धनाधित कुरूढ़ियों से अभिमूत होता जा रहा है, सर्वमहान क्रियोहारक एवं भगवान तीर्थंकर देव की शुद्धाम्नाय के पुनरुवारक भगवत्करकन्दाचार्य के तविषयक उपवेश ही समर्थ प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक हो सकते हैं। साध्वाचार शुद्ध हो जाय तो प्रावकाचार स्वतः संघरता चला जायेगा। भगवान के धर्म-तीर्थ एवं श्रीसंघ की शक्ति का प्रधान प्राधार शद्ध एवं पावर्श साध्वाचार ही है।
प्रातःस्मरणीय मूलसंचाग्रणी श्रीमद् भगवत्कुन्दाचार्य विदेशी लोगों के प्रागमन एवं प्रभाव से भारतीय धर्मों का का सूनाम मात्र जन संस्कृति के ही इतिहास में नहीं, व्यावहारिक रूप भी पर्याप्त निश्रित होने लगा थाअध्यात्म-विद्या के सार्वकालीन एव सर्वदेशीय इतिहास में दक्षिण भारत अभी तक ऐसे अनिष्ट प्रभावो से अछना भी स्वर्णाकित हैं। वह युगान्तरकारी महापुरुष थे और बचा हुआ था। कम से कम जैन इतिहास के तो ऐसे मोड़ पर खड़े थे जब ऐसे समय मे भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य का सुदूर दक्षिण अनेक आन्तरिक एवं बाप कारणों से परिस्थिति पर्याप्त में आविर्भाव हुआ। वह भगवान महावीर की आचार्य विषम थी। अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर (ई० पू० परपरा के २७वे गुरू, आचार्य भद्रबाहु द्वितीय (ई० पू० ५६९-५२७) को निर्वाण प्राप्त किये लगमग पांच सो वर्ष ३७-१४) के, जो कि स्वय अष्टागधारी थे तथा शेष अगबीत चुके थे, और इस बीच उनके द्वारा प्रवर्तित द्रव्यश्रुत, पूर्वो के देशज्ञाता थे, साक्षात् शिष्य थे। लोहाचार्य, द्वादशांगवाणी अथवा ग्यारह अंग-चौदहपूर्वो के ज्ञान में वटुकेरि, गुणधर, अर्हद्वलि, माघनंदि, धरसेन, विमलार्य क्रमशः ह्रास एवं ध्युच्छिति होते रहने से अब कतिपय अंग- शिवार्य, स्वामिकमार, उमास्वाति आदि अनेक घरघर पूर्वो के गिने-चुने कुछ एकदेश ज्ञाता ही अवशिष्ट रह गये आचार्य उनके प्रायः समसामयिक थे । अभी तक द्वादशांगथे। भगवान के श्रीसघ मे शनैः शनैः भारी विघटन, श्रुत गुरुपरंपरा में मौखिक द्वार से ही प्रवाहित होता पाया बिखराव, केन्द्र परिवर्तन, शिथिलाचार एव फूट प्रकट हो था, और शायद यह भी एक बड़ा कारण था कि उसमें रहे थे । अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु प्रथम (ई० क्रमशः ह्रास एक व्यच्छिति होती चली जा रही थो । किन्तु पृ० ३९४-३६५) की शिष्य-परंपरा के दाक्षिणात्य निर्ग्रन्थ सर्व परिग्रहत्यागी बनवासी निग्रंथ श्रमणों की चर्या ही ऐसी श्रमणों का सगठन एवं मार्गदर्शन करने की भी परम थी। वे न किसी बस्ती मे ही रह सकते थे, न किसी एक आवश्यकता थी, क्योंकि अभी तक वे ही भगवान को स्थान में अधिक समय तक ठहर सकते थे और लेखन एव मौलिक परंपरा का संरक्षण अपनी मुनिचर्या द्वारा करते पठन-पाटन की साधन-सामग्री तक का परिग्रह भी नहीं आ रहे थे। उनमें भी अब बिखराव के सकेत मिलने लगे रख सकते थे । अतएव श्रुतागम को लिपिबर थे। ब्राह्मण परंपरा के षड्दर्शन अब तक रूढ़ हो चुके थे सामूहिक विरोध ही चलता रहा। कनिगचक्रवर्ती सम्रट और बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित होने खारवेल द्वारा कुमारी पर्वत पर, लगभग ई० पू० १५० मे, पर भी फल फूल रहा था। सब ही परंपराएं बाह्य पिया- आयोजित महामुनि-सम्मेलन में यह प्रश्न जोर-शोर के काण्ड एवं प्रवृत्तिमार्ग का पोषण कर रही थीं। उत्तर साथ चचित भी हुआ और वहां से आकर उत्तर मथुरा के भारत में तो ईरानी- यूनानी, हलव, शक, कुषाण आदि जैनसंघ ने पुस्तकधारिणी सरस्वती प्रतिमा को प्रतीक बना