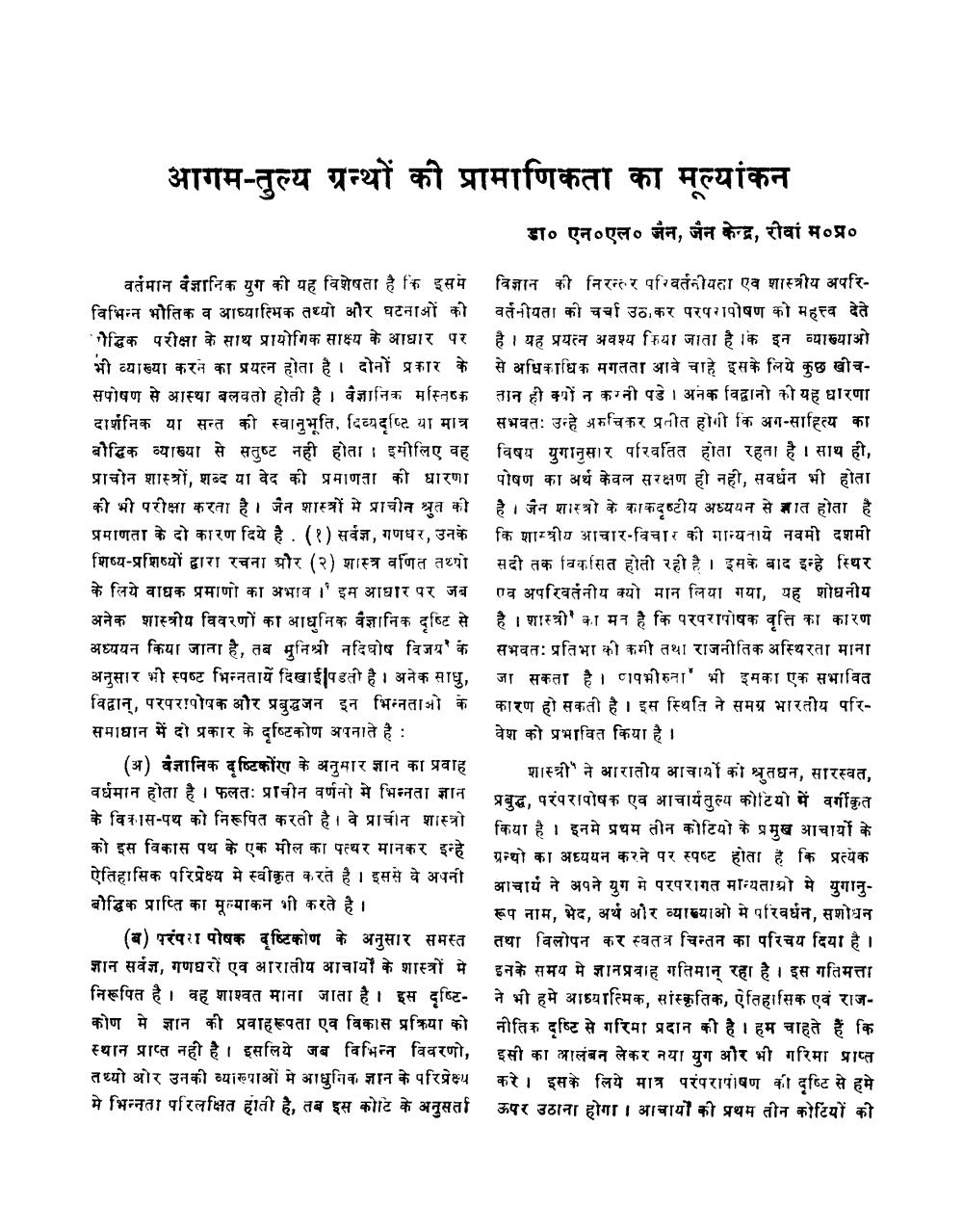________________
आगम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन
वर्तमान वैज्ञानिक युग की यह विशेषता है कि इसमें विभिन्न भौतिक व आध्यात्मिक तथ्यों और घटनाओं को द्धिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक साक्ष्य के आधार पर भी व्याख्या करने का प्रयत्न होता है। दोनों प्रकार के सपोषण से आस्था बलवतो होती है। वैज्ञानिक मस्तिष्क दार्शनिक या सन्त की स्वानुभूति दिव्यदृष्टि या मात्र बौद्धिक व्याख्या से सतुष्ट नहीं होता इसीलिए वह प्राचीन शास्त्रों, शब्द या वेद की प्रमाणता की धारणा की भी परीक्षा करता है। जैन शास्त्रों में प्राचीन श्रुत की प्रमाणता के दो कारण दिये है. (१) सर्वश, गणधर उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा रचना और (२) शास्त्र वर्णित तथ्यो के लिये वाधक प्रमाणो का अभाव। इस आधार पर जब अनेक शास्त्रीय विवरणों का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, तब मुनिश्री नदिघोष विजय के अनुसार भी स्पष्ट भिन्नतायें दिखाई पडती है । अनेक साधु, विद्वान्, परपरपोषक और प्रबुद्धजन इन भिन्नताओ के समाधान में दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाते है
(अ) वैज्ञानिक दृष्टिकों के अनुसार ज्ञान का प्रवाह वर्धमान होता है। फलतः प्राचीन वर्णनो मे भिन्नता ज्ञान के विकास पथ को निरूपित करती है। वे प्राचीन शास्त्रो को इस विकास पथ के एक मील का पत्थर मानकर इन्हे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे स्वीकृत करते है। इससे वे अपनी बौद्धिक प्राप्ति का मूल्याकन भी करते है ।
(ब) परंपरा पोषक दृष्टिकोण के अनुसार समस्त ज्ञान सर्वज्ञ, गणधरों एव आरातीय आचार्यों के शास्त्रों में निरूपित है वह शाश्वत माना जाता है। इस दृष्टि कोण मे ज्ञान की प्रवाहरूपता एवं विकास प्रक्रिया को स्थान प्राप्त नही है । इसलिये जब विभिन्न विवरणो, तथ्यो ओर उनकी व्याख्याओं में आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे भिन्नता परिलक्षित होती है, तब इस कोटि के अनुसर्ता
डा० एन०एल० जैन, जंन केन्द्र, रीवां म०प्र०
विज्ञान की निरन्तर परिवर्तनीया एवं शास्त्रीय अपरिवर्तनीयता की चर्चा उठा कर परपरापोषण को महत्त्व देते है । यह प्रयत्न अवश्य किया जाता है कि इन व्याख्याओ से अधिकाधिक मगतता आये चाहे इसके लिये कुछ बीचछान ही क्यों न करनी पडे अनेक विद्वानो की यह धारणा संभवतः उन्हें अरुचिकर प्रतीत होगी कि अन-साहित्य का विषय युगानुसार परिवर्तित होता रहता है। साथ ही, पोषण का अर्थ केवल सरक्षण ही नहीं, सवर्धन भी होता है। जैन शास्त्री के काकदृष्टीय अध्ययन से ज्ञात होता है कि शास्त्रीय आचार-विचार की मान्यताये नवमी दशमी सदी तक विकसित होती रही है । इसके बाद इन्हे स्थिर एव अपरिवर्तनीय क्यो मान लिया गया, यह शोधनीय है। शास्त्री का मन है कि परपरापोषक वृद्धि का कारण सभवतः प्रतिभा की कमी तथा राजनीतिक अस्थिरता माना जा सकता है। पापभीरुता भी इसका एक सभावित कारण हो सकती है। इस स्थिति ने समग्र भारतीय परिवेश को प्रभावित किया है।
शास्त्री ने आरातीय आवायों को बुतधन, सारस्वत, प्रबुद्ध, परंपरापोषक एव आचार्य तुल्य कोटियो में वर्गीकृत किया है। इनमे प्रथम तीन कोटियों के प्रमुख आचार्यों के ग्रन्थो का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक आचार्य ने अपने युग मे परपरागत मान्यतायो मे युगानु रूप नाम, भेद, अर्थ और व्याख्याओ मे परिवर्धन, सशोधन तथा विलोपन कर स्वतंत्र चिन्तन का परिचय दिया है। इनके समय मे ज्ञानप्रवाह गतिमान् रहा है । इस गतिमत्ता ने भी हमे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से गरिमा प्रदान की है। हम चाहते हैं कि इसी का आलंबन लेकर नया युग और भी गरिमा प्राप्त करे । इसके लिये मात्र परंपरापोषण की दृष्टि से हमे ऊपर उठाना होगा । आचायों की प्रथम तीन कोटियों की