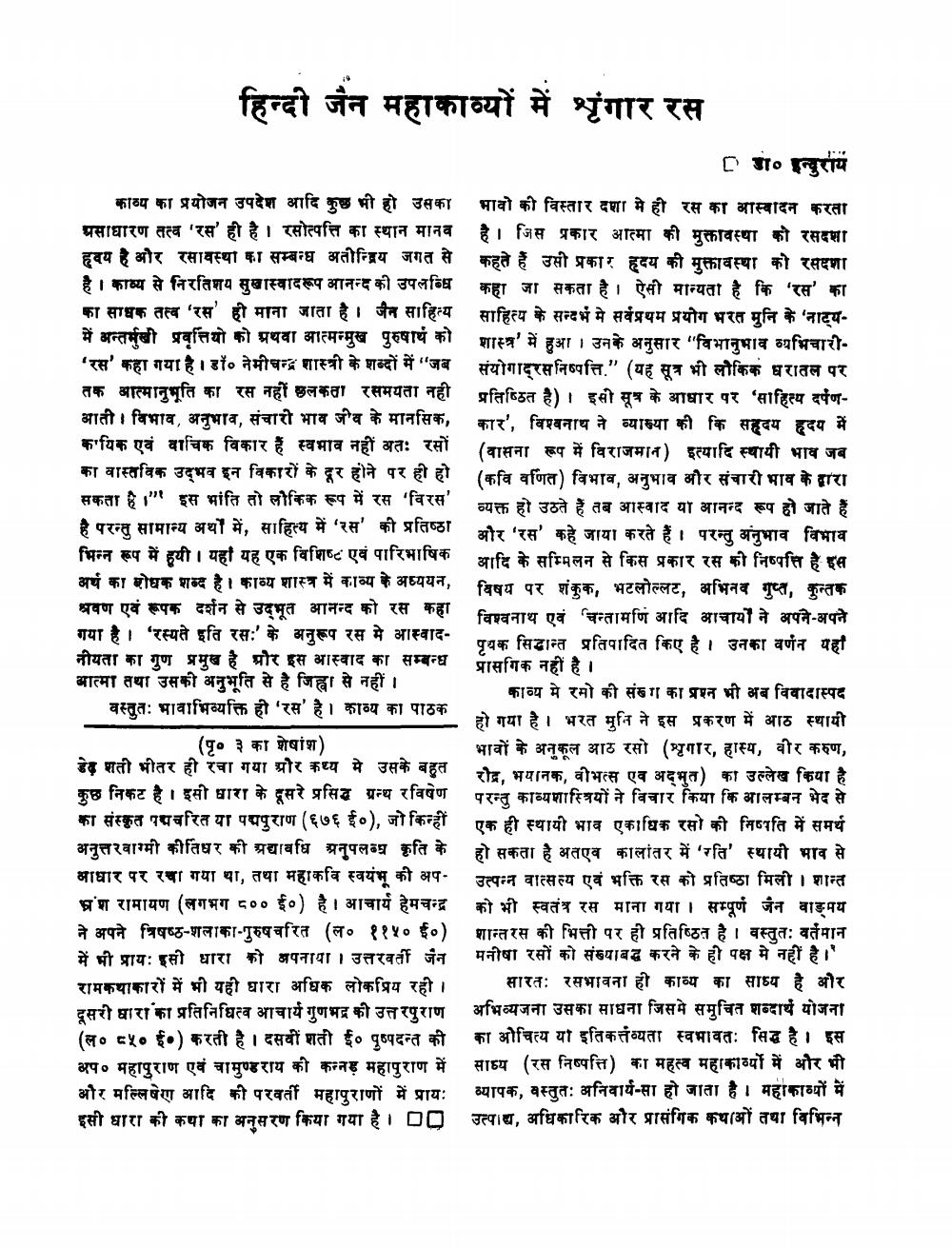________________
हिन्दी जैन महाकाव्यों में शृंगार रस
काव्य का प्रयोजन उपदेश आदि कुछ भी हो उसका असाधारण तत्व 'रस' ही है। रसोत्पत्ति का स्थान मानव हृदय है और रसावस्था का सम्बन्ध अतीन्द्रिय जगत से है। काव्य से निरतिशय सुखास्वादरूप आनन्द की उपलब्धि का साधक तत्व 'रस' ही माना जाता है। जैन साहित्य में अन्तर्मुखी प्रवृत्तियो को अथवा आत्मन्मुख पुरुषार्थ को 'रस' कहा गया है। डॉ० नेमीचन्द्र शास्त्री के शब्दों में "जब तक आत्मानुभूति का रस नहीं छलकता रसमयता नही आती। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जीव के मानसिक, कायिक एवं वार्षिक विकार हैं स्वभाव नहीं अतः रसों का वास्तविक उद्भव इन विकारों के दूर होने पर ही हो सकता है। इस भांति तो लौकिक रूप में रस 'विरस' है परन्तु सामान्य अर्थों में, साहित्य में 'रस' की प्रतिष्ठा भिन्न रूप में हुयी। यहाँ यह एक विशिष्ट एवं पारिभाषिक अर्थ का बोधक शब्द है । काव्य शास्त्र में काव्य के अध्ययन, श्रवण एवं रूपक दर्शन से उद्भूत आनन्द को रस कहा गया है । 'रस्यते इति रसः' के अनुरूप रस मे आस्वादनीयता का गुण प्रमुख है और इस आस्वाद का सम्बन्ध आत्मा तथा उसको अनुभूति से है जिल्ला से नहीं ।
वस्तुतः भावाभिव्यक्ति ही 'रस' है । काव्य का पाठक ( पृ० ३ का शेषांश)
डेढ शती भीतर ही रचा गया और कथ्य मे उसके बहुत कुछ निकट है। इसी धारा के दूसरे प्रसिद्ध ग्रन्थ रविषेण का संस्कृत पद्मचरित या पद्मपुराण (६७६ ई०), जो किन्हीं अनुत्तरवाग्मी कीर्तिधर की अद्यावधि अनुपलब्ध कृति के आधार पर रखा गया था, तथा महाकवि स्वयंभू की अप' रामायण ( लगभग ८०० ई०) है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने त्रिषष्ठ-शलाका-पुरुष चरित (ल० ११५० ई०) में भी प्रायः इसी धारा को अपनाया । उत्तरवर्ती जैन रामकथाकारों में भी यही द्वारा अधिक लोकप्रिय रही। दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व आचार्य गुणभद्र की उत्तरपुराण (ल० ८५० ई०) करती है। दसवीं शती ई० पुष्पदन्त की अप० महापुराण एवं चामुण्डराय की कन्नड़ महापुराण में और मल्मिषेश आदि की परवर्ती महापुराणों में प्रायः इसी धारा की कथा का अनुसरण किया गया है।
[ डा० इन्दुरा
भावो की विस्तार दशा मे ही रस का आस्वादन करता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था को रसदशा कहते हैं उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा कहा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि 'रस' का साहित्य के सन्दर्भ मे सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' में हुआ । उनके अनुसार "विभानुभाव व्यभिचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्ति" (यह सूत्र भी लौकिक धरातल पर प्रतिष्ठित है ) । इसी सूत्र के आधार पर 'साहित्य दर्पणकार, विश्वनाथ ने व्याख्या की कि सहृदय हृदय में ( वासना रूप में विराजमान ) इत्यादि स्थायी भाव जब ( कवि वर्णित ) विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा
व्यक्त हो उठते हैं तब आस्वाद या आनन्द रूप हो जाते हैं। और 'रस' कहे जाया करते हैं। परन्तु अनुभाव विभाव आदि के सम्मिलन से किस प्रकार रस को निष्पत्ति है इस विषय पर शंकुक, भटलोल्लट, अभिनव गुप्त, कुन्तक विश्वनाथ एवं चिन्तामणि आदि आचार्यों ने अपने-अपने पृथक सिद्धान्त प्रतिपादित किए है। उनका वर्णन यहाँ प्रासंगिक नहीं है।
काव्य मे रमों की संख्ग का प्रश्न भी अब विवादास्पद हो गया है। भरत मुनि ने इस प्रकरण में आठ स्थायी भावों के अनुकूल आठ रसो ( श्रृगार, हास्य, वीर करुण, रौद्र, भयानक, वीभत्स एव अद्भुत) का उल्लेख किया है परन्तु काव्यशास्त्रियों ने विचार किया कि आलम्बन भेद से एक ही स्थायी भाव एकाधिक रसो की मिष्यति में समर्थ हो सकता है अतएव कालांतर में 'रति' स्थायी भाव से उत्पन्न वात्सल्य एवं भक्ति रस को प्रतिष्ठा मिली। शान्त को भी स्वतंत्र रस माना गया। सम्पूर्ण जैन वाङ्मय शान्तरस की भिती पर ही प्रतिष्ठित है। वस्तुतः वर्तमान मनीषा रसों को संवाद करने के ही पक्ष में नहीं है।'
सारतः रसभावना ही काव्य का साध्य है और अभिव्यजना उसका साधना जिसमे समुचित शब्दार्थ योजना का औचित्य या इतिकर्तव्यता स्वभावतः सिद्ध है । इस साध्य ( रस निष्पति) का महत्व महाकाव्यों में और भी व्यापक, वस्तुतः अनिवार्य सा हो जाता है । महाकाव्यों में उत्पाद्य, अधिकारिक और प्रासंगिक कथाओं तथा विभिन्न