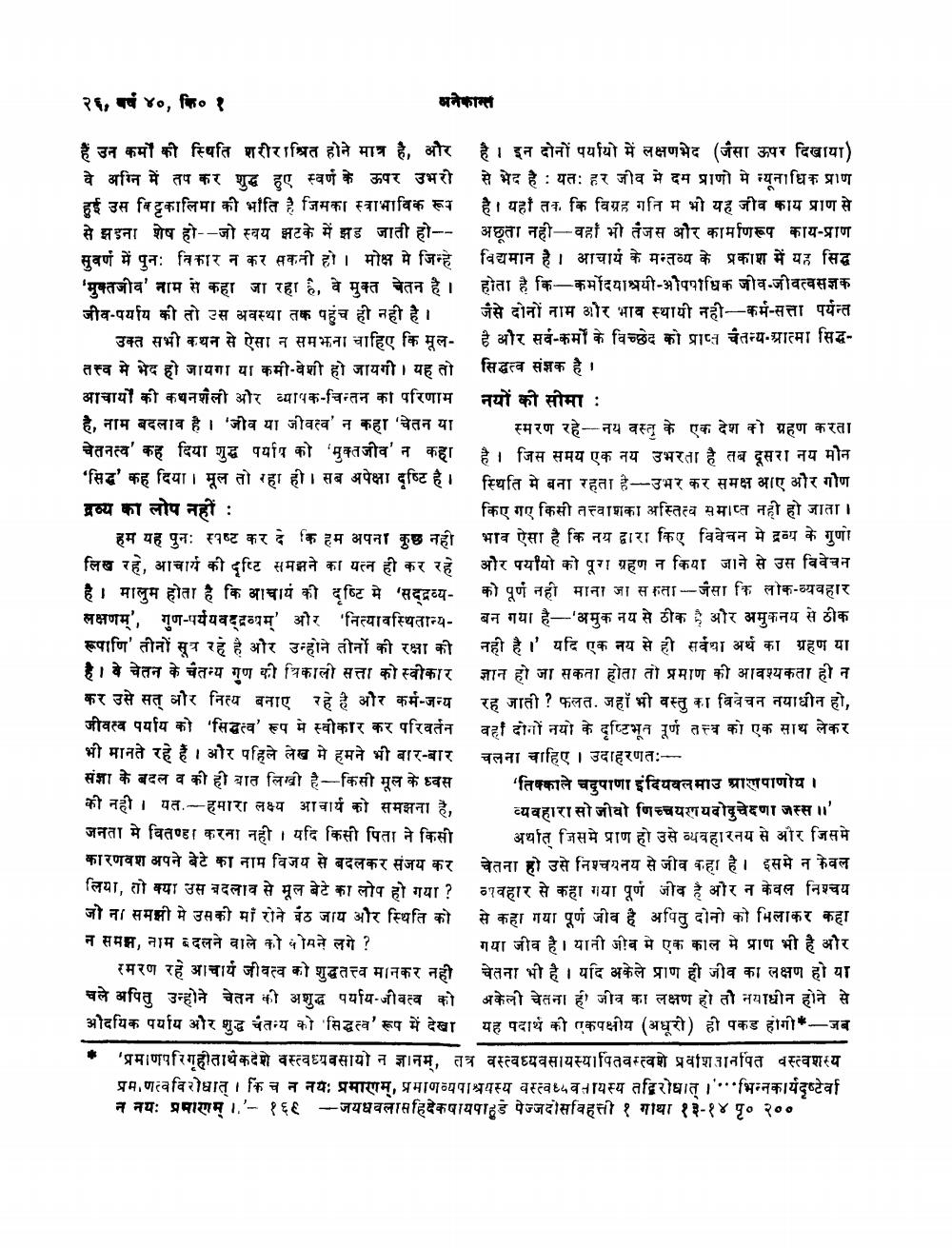________________
२६ बर्ष ४०, कि०१
बनेकान्त
हैं उन कर्मों की स्थिति शरीराश्रित होने मात्र है, और है। इन दोनों पर्यायो में लक्षणभेद (जैसा ऊपर दिखाया) वे अग्नि में तप कर शुद्ध हए स्वर्ण के ऊपर उभरी से भेद है : यतः हर जीव मे दम प्राणो मे न्यूनाधिक प्राण हुई उस विटकालिमा की भांति है जिसका स्वाभाविक रूप है। यहाँ तक कि विग्रह गति में भी यह जीव काय प्राण से से झडना शेष हो--जो स्वय झटके में झड जाती हो-- अछूता नहीं-वहाँ भी तंजस और कार्माणरूप काय-प्राण सुवर्ण में पुन: विकार न कर सकती हो। मोक्ष मे जिन्हे विद्यमान है। आचार्य के मन्तव्य के प्रकाश में यह सिद्ध 'मुक्तजीव' नाम से कहा जा रहा है, वे मुक्त चेतन है। होता है कि-कर्मोदयाश्रयी-औपपाधिक जीव-जीवत्वसज्ञक जीव-पर्याय की तो उस अवस्था तक पहुंच ही नही है। जैसे दोनों नाम और भाव स्थायी नहीं-कर्म-सत्ता पर्यन्त
उक्त सभी कथन से ऐसा न समझना चाहिए कि मूल- है और सर्व-कर्मों के विच्छेद को प्राप्त चतन्य-प्रात्मा सिद्धतत्व मे भेद हो जायगा या कमी-वेशी हो जायगी। यह तो सिद्धत्व संशक है। आचार्यों की कथनशैली और व्यापक-चिन्तन का परिणाम नयों की सीमा : है, नाम बदलाव है। 'जीव या जीवत्व' न कहा 'चेतन या स्मरण रहे-नय वस्तु के एक देश को ग्रहण करता चेतनत्व' कह दिया शुद्ध पर्याप को 'मुक्तजीव' न कहा है। जिस समय एक नय उभरता है तब दूसरा नय मोन 'सिद्ध' कह दिया। मूल तो रहा ही। सब अपेक्षा दृष्टि है। स्थिति मे बना रहता है-उभर कर समक्ष आए और गोण द्रव्य का लोप नहीं:
किए गए किसी तत्त्वाशका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। हम यह पुन: स्पष्ट कर दे कि हम अपना कुछ नही भाव ऐसा है कि नय द्वारा किए विवेचन मे द्रव्य के गुणो लिख रहे, आचार्य की दृष्टि समझने का यत्न ही कर रहे और पर्यायो को पूग ग्रहण न किया जाने से उस विवेचन है। मालुम होता है कि आचार्य की दृष्टि मे 'सदद्रव्य- को पूर्ण नही माना जा सकता-जैसा कि लोक-व्यवहार लक्षणम्', गुण-पर्ययवद्रव्यम्' और 'नित्यावस्थितान्य- बन गया है-'अमुक नय से ठीक है और अमुकनय से ठीक रूपाणि' तीनों सूप रहे है और उन्होंने तीनों की रक्षा की नहीं है।' यदि एक नय से ही सर्वथा अर्थ का ग्रहण या है। वे चेतन के चैतन्य गुण की पिकाली सत्ता को स्वीकार ज्ञान हो जा सकता होता तो प्रमाण की आवश्यकता ही न कर उसे सत् और नित्य बनाए रहे है और कर्म-जन्य रह जाती? फलत. जहाँ भी वस्तु का विवेचन नयाधीन हो, जीवत्व पर्याय को 'सिद्धत्व' रूप में स्वीकार कर परिवर्तन वहां दोनों नयो के दृष्टिभूत पूर्ण तत्त्व को एक साथ लेकर भी मानते रहे हैं। और पहिले लेख में हमने भी बार-बार चलना चाहिए । उदाहरणत:संज्ञा के बदल व की ही बात लिखी है-किसी मूल के ध्वस 'तिक्काले चदुपाणा इंदियवलमाउ प्राणपाणोय। की नहीं। यत.-हमारा लक्ष्य आचार्य को समझना है,
व्यवहारासो जीवो णिच्चयरायदोदुचेदणा जस्स ॥' जनता मे वितण्डा करना नही । यदि किसी पिता ने किसी अर्थात जिसमे प्राण हो उसे व्यवहारनय से और जिसमे कारणवश अपने बेटे का नाम विजय से बदलकर संजय कर चेतना हो उसे निश्चयनय से जीव कहा है। इसमे न केवल लिया, तो क्या उस बदलाव से मूल बेटे का लोप हो गया? पवहार से कहा गया पूर्ण जीव है और न केवल निश्चय जो ना समझी मे उसकी माँ रोने चंठ जाय और स्थिति को से कहा गया पूर्ण जीव है अपितु दोनो को मिलाकर कहा न समझ, नाम बदलने वाले को कोसने लगे ?
गया जीव है। यानी जीव मे एक काल मे प्राण भी है और रमरण रहे आचार्य जीवत्व को शुद्धतत्त्व मानकर नही चेतना भी है। यदि अकेले प्राण ही जीव का लक्षण हो या चले अपितु उन्होने चेतन की अशुद्ध पर्याय-जीवत्व को अकेली चेतना ही जीव का लक्षण हो तो नयाधीन होने से औदयिक पर्याय और शुद्ध चतन्य को 'सिद्धत्व' रूप में देखा यह पदार्थ को एकपक्षीय (अधूरी) ही पकड होगी*-जब
'प्रमाणपरिगृहीतायैकदेशे वस्त्वध्यवसायो न ज्ञानम्, तत्र वस्त्वध्यवसायस्यापितवस्त्वशे प्रशितानपित वस्त्वशस्य प्रमाणत्वविरोधात् । किं च न नयः प्रमारणम्, प्रमाणव्यपाश्रयस्य वस्त्व५वतायस्य तद्विरोधात् । भिन्नकार्यदृष्टेर्वा न नयः प्रमारणम् ।'- १६६ -जयधवलासहिदेकषायपाडे पेज्जदोसविहत्ती १ गाथा १३-१४ पृ० २००