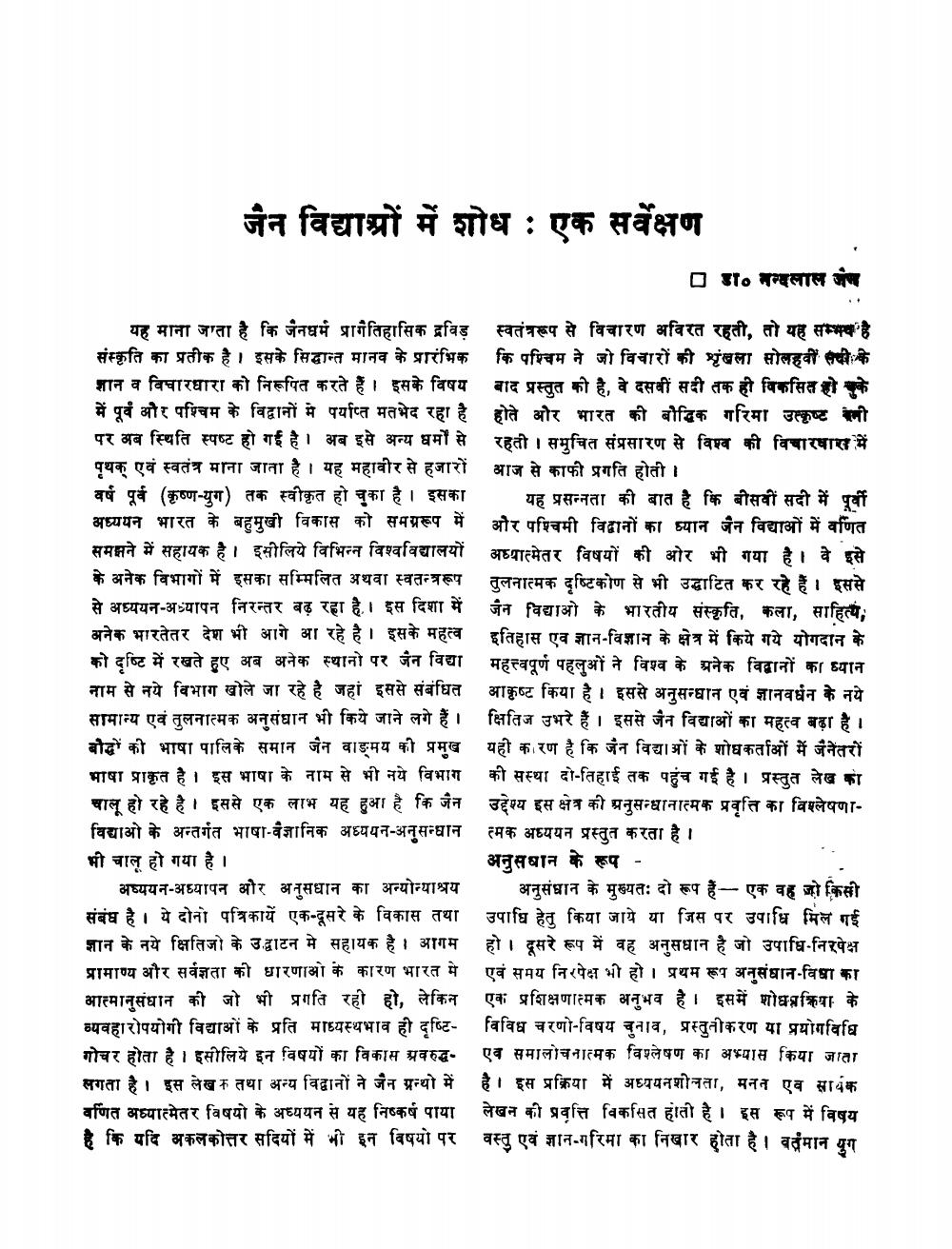________________
जैन विद्याओं में शोध : एक सर्वेक्षण
0डानन्दलाल जंग
यह माना जाता है कि जैनधर्म प्रागैतिहासिक द्रविड़ स्वतंत्ररूप से विचारण अविरत रहती, तो यह सम्भव है संस्कृति का प्रतीक है। इसके सिद्धान्त मानव के प्रारंभिक कि पश्चिम ने जो विचारों की श्रृंखला सोलहवीं सदी के शान व विचारधारा को निरूपित करते हैं। इसके विषय बाद प्रस्तुत की है, वे दसवीं सदी तक ही विकसित हो चुके में पूर्व और पश्चिम के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है होते और भारत की बौद्धिक गरिमा उत्कृष्ट बनी पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब इसे अन्य धर्मों से रहती। समुचित संप्रसारण से विश्व की विचारधारा में पृथक एवं स्वतंत्र माना जाता है। यह महावीर से हजारों आज से काफी प्रगति होती। वर्ष पूर्व (कृष्ण-युग) तक स्वीकृत हो चुका है। इसका यह प्रसन्नता की बात है कि बीसवीं सदी में पूर्वी अध्ययन भारत के बहुमुखी विकास को समग्ररूप में और पश्चिमी विद्वानों का ध्यान जैन विद्याओं में वणित समझने में सहायक है। इसीलिये विभिन्न विश्वविद्यालयों अध्यात्मेतर विषयों की ओर भी गया है। वे इसे के अनेक विभागों में इसका सम्मिलित अथवा स्वतन्त्ररूप तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी उद्घाटित कर रहे हैं। इससे से अध्ययन-अध्यापन निरन्तर बढ़ रहा है। इस दिशा में जैन विद्याओ के भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, अनेक भारतेतर देश भी आगे आ रहे है। इसके महत्व इतिहास एव ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में किये गये योगदान के को दृष्टि में रखते हुए अब अनेक स्थानो पर जैन विद्या महत्त्वपूर्ण पहलुओं ने विश्व के अनेक विद्वानों का ध्यान नाम से नये विभाग खोले जा रहे है जहां इससे संबंधित आकृष्ट किया है। इससे अनुसन्धान एवं ज्ञानवर्धन के नये सामान्य एवं तुलनात्मक अनुसंधान भी किये जाने लगे हैं। क्षितिज उभरे हैं। इससे जैन विद्याओं का महत्व बढ़ा है। बौद्धों की भाषा पालिके समान जैन वाङ्मय की प्रमुख यही क रण है कि जैन विद्याओं के शोधकर्ताओं में जैनेतरों भाषा प्राकृत है। इस भाषा के नाम से भी नये विभाग की सस्था दो-तिहाई तक पहुंच गई है। प्रस्तुत लेख को चालू हो रहे है। इससे एक लाभ यह हुआ है कि जैन उद्देश्य इस क्षेत्र की अनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति का विश्लेषणाविद्याओ के अन्तर्गत भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान त्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। भी चालू हो गया है।
अनुसंधान के रूप - अध्ययन-अध्यापन और अनुसंधान का अन्योन्याश्रय अनुसंधान के मुख्यतः दो रूप हैं- एक वह जो किसी संबंध है। ये दोनो पत्रिकायें एक-दूसरे के विकास तथा उपाधि हेतु किया जाये या जिस पर उपाधि मिल गई ज्ञान के नये क्षितिजो के उद्धाटन में सहायक है। आगम हो। दूसरे रूप में वह अनुसधान है जो उपाधि-निरपेक्ष प्रामाण्य और सर्वज्ञता की धारणाओ के कारण भारत मे एवं समय निरपेक्ष भी हो। प्रथम रूप अनुसंधान-विधा का आत्मानुसंधान की जो भी प्रगति रही हो, लेकिन एक प्रशिक्षणात्मक अनुभव है। इसमें शोधप्रक्रिया के व्यवहारोपयोगी विद्याओं के प्रति माध्यस्थभाव ही दृष्टि- विविध चरणो-विषय चुनाव, प्रस्तुतीकरण या प्रयोगविधि गोचर होता है । इसीलिये इन विषयों का विकास अवरुद्ध- एव समालोचनात्मक विश्लेषण का अभ्यास किया जाता लगता है। इस लेखक तथा अन्य विद्वानों ने जैन ग्रन्थो में है। इस प्रक्रिया में अध्ययनशीलता, मनन एव सार्थक वणित अध्यात्मेतर विषयो के अध्ययन से यह निष्कर्ष पाया लेखन की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस रूप में विषय है कि यदि अकलकोत्तर सदियों में भी इन विषयो पर वस्तु एवं ज्ञान-गरिमा का निखार होता है। वर्तमान यग