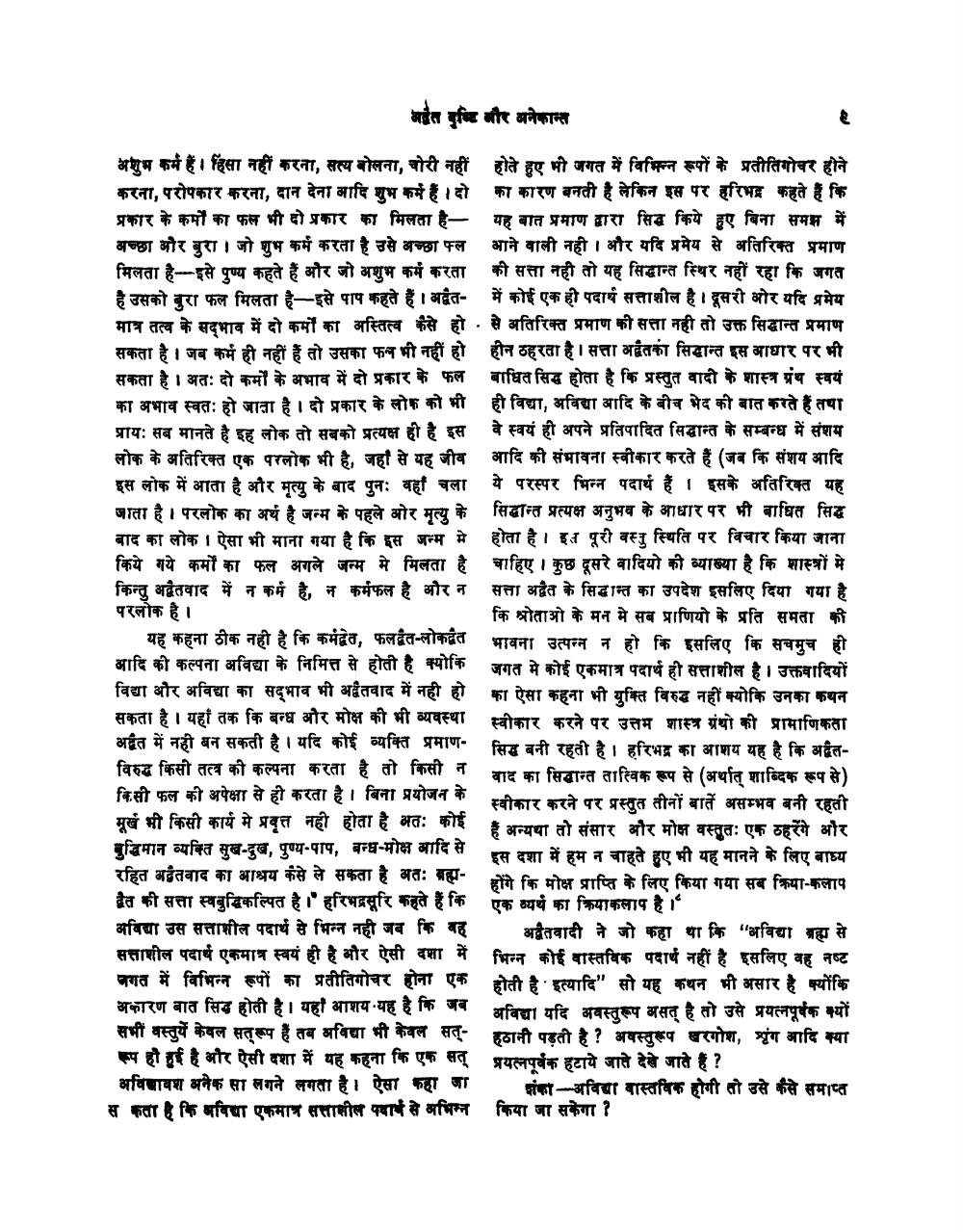________________
बढत दि और अनेकान्त
अशुभ कर्म हैं। हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं होते हुए भी जगत में विभिन्न रूपों के प्रतीतिगोचर होने करना, परोपकार करना, दान देना आदि शुभ कर्म हैं। दो का कारण बनती है लेकिन इस पर हरिभद्र कहते हैं कि प्रकार के कर्मों का फल भी दो प्रकार का मिलता है- यह बात प्रमाण द्वारा सिद्ध किये हुए बिना समझ में अच्छा और बुरा। जो शुभ कर्म करता है उसे अच्छा फल आने वाली नही । और यदि प्रमेय से अतिरिक्त प्रमाण मिलता है-इसे पुण्य कहते हैं और जो अशुभ कर्म करता की सत्ता नही तो यह सिद्धान्त स्थिर नहीं रहा कि जगत है उसको बुरा फल मिलता है-इसे पाप कहते हैं । अद्वैत- में कोई एक ही पदार्थ सत्ताशील है। दूसरी ओर यदि प्रमेय मात्र तत्व के सद्भाव में दो कर्मों का अस्तित्व कैसे हो . से अतिरिक्त प्रमाण की सत्ता नही तो उक्त सिद्धान्त प्रमाण सकता है। जब कर्म ही नहीं हैं तो उसका फल भी नहीं हो हीन ठहरता है । सत्ता अद्वतका सिद्धान्त इस आधार पर भी सकता है। अत: दो कर्मों के अभाव में दो प्रकार के फल बाधित सिद्ध होता है कि प्रस्तुत वादी के शास्त्र ग्रंथ स्वयं का अभाव स्वतः हो जाता है। दो प्रकार के लोक को भी ही विद्या, अविद्या आदि के बीच भेद की बात करते हैं तथा प्रायः सब मानते है इह लोक तो सबको प्रत्यक्ष ही है इस वे स्वयं ही अपने प्रतिपादित सिद्धान्त के सम्बन्ध में संशय लोक के अतिरिक्त एक परलोक भी है, जहां से यह जीव आदि की संभावना स्वीकार करते हैं (जब कि संशय आदि इस लोक में आता है और मृत्यु के बाद पुनः वहाँ चला ये परस्पर भिन्न पदार्थ हैं । इसके अतिरिक्त यह जाता है। परलोक का अर्थ है जन्म के पहले और मृत्यु के सिद्धान्त प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भी बाधित सिद्ध बाद का लोक । ऐसा भी माना गया है कि इस जन्म मे होता है। इस पूरी वस्तु स्थिति पर विचार किया जाना किये गये कर्मों का फल अगले जन्म मे मिलता है चाहिए । कुछ दूसरे वादियो की व्याख्या है कि शास्त्रों में किन्तु अद्वैतवाद में न कर्म है, न कर्मफल है और न सत्ता अद्वैत के सिद्धान्त का उपदेश इसलिए दिया गया है परलोक है।
कि श्रोताओ के मन मे सब प्राणियो के प्रति समता की यह कहना ठीक नही है कि कर्मद्वेत, फलद्वैत-लोकद्वैत भावना उत्पन्न न हो कि मि आदि की कल्पना अविद्या के निमित्त से होती है क्योकि जगत मे कोई एकमात्र पदार्थ ही सत्ताशील है। उक्तवादियों विद्या और अविद्या का सद्भाव भी अद्वैतवाद में नही हो का ऐसा कहना भी युक्ति विरुद्ध नहीं क्योकि उनका कथन सकता है। यहाँ तक कि बन्ध और मोक्ष की भी व्यवस्था स्वीकार करने पर उत्तम शास्त्र ग्रंथो की प्रामाणिकता अद्वैत में नही बन सकती है । यदि कोई व्यक्ति प्रमाण
सिद्ध बनी रहती है। हरिभद्र का आशय यह है कि अद्वैतविरुद्ध किसी तत्व की कल्पना करता है तो किसी न
वाद का सिद्धान्त तात्विक रूप से (अर्थात् शाब्दिक रूप से) किसी फल की अपेक्षा से ही करता है। बिना प्रयोजन के
स्वीकार करने पर प्रस्तुत तीनों बातें असम्भव बनी रहती मूर्ख भी किसी कार्य मे प्रवृत्त नही होता है अतः कोई
हैं अन्यथा तो संसार और मोक्ष वस्तुतः एक ठहरेंगे और बुद्धिमान व्यक्ति सुख-दुख, पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष आदि से
इस दशा में हम न चाहते हुए भी यह मानने के लिए बाध्य रहित अद्वैतवाद का आश्रय कैसे ले सकता है अतः ब्रह्म- योगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया सब क्रिया-कलाप द्वैत की सत्ता स्वबुद्धिकल्पित है। हरिभद्रसूरि कहते हैं कि एक व्यर्थ का क्रियाकलाप है। अविद्या उस सत्ताशील पदार्थ से भिन्न नही जब कि वह अद्वैतवादी ने जो कहा था कि "अविद्या ब्रह्म से सत्ताशील पदार्थ एकमात्र स्वयं ही है और ऐसी दशा में भिन्न कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है इसलिए वह नष्ट जगत में विभिन्न रूपों का प्रतीतिगोचर होना एक होती है इत्यादि" सो यह कथन भी असार है क्योंकि अकारण बात सिद्ध होती है। यहाँ आशय यह है कि जब अविद्या यदि अवस्तुरूप असत् है तो उसे प्रयत्नपूर्वक क्यों सभी वस्तुयें केवल सतरूप हैं तब अविद्या भी केवल सत्
हठानी पड़ती है ? अवस्तुरूप खरगोश, शृंग आदि क्या रूप ही हुई है और ऐसी दशा में यह कहना कि एक सत् प्रयत्नपूर्वक हटाये जाते देखे जाते हैं ?
अविद्यावश अनेक सा लगने लगता है। ऐसा कहा जा शंका-अविद्या वास्तविक होगी तो उसे कैसे समाप्त सकता है कि विधा एकमात्र सत्तासील पहा से अभिन्न किया जा सकेगा।