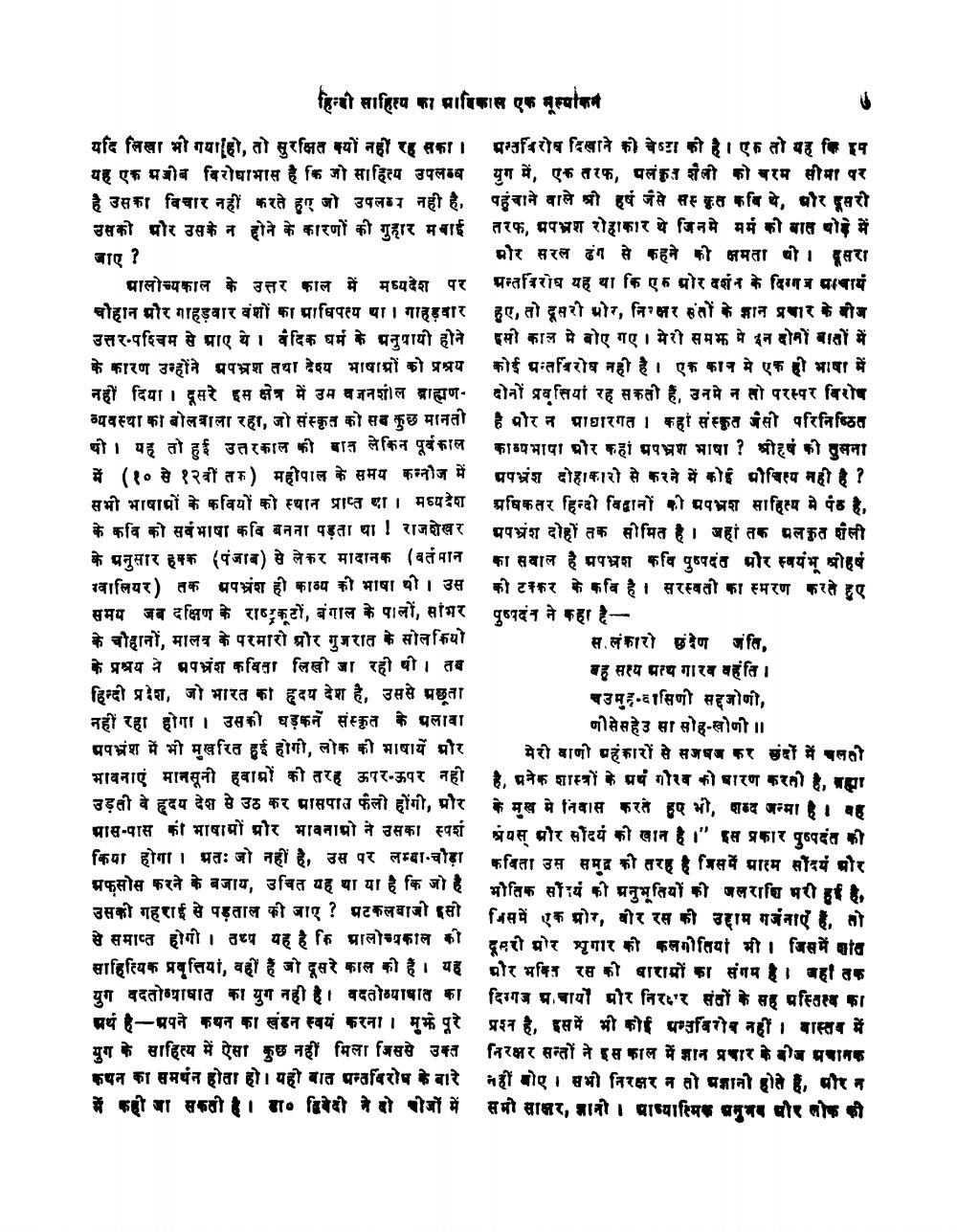________________
हिन्दी साहित्यका यदि लिखा भी गया हो, तो सुरक्षित क्यों नहीं रह सका । यह एक मजीब विरोधाभास है कि जो साहित्य उपलब्ध है उसका विचार नहीं करते हुए जो उपलब्ध नहीं है, उसकी भोर उसके न होने के कारणों की गुहार मबाई जाए ?
प्राविकाल
एक मूल्यांकन
विशेष दिखाने की चेष्टा की है। एक तो यह कि इम युग में, एक तरफ, पलंकृत शैली को चरम सीमा पर पहुंचाने वाले श्री हर्ष जैसे सह कुल कवि थे, और दूसरी तरफ, अपभ्रंश शहाकार थे जिनमे मर्म की बात थोड़े में मोर सरल ढंग से कहने की क्षमता थी। दूसरा प्रतविरोध यह था कि एक ओर दर्शन के दिग्गज प्राचार्य हुए, तो दूसरी ओर, निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार के बीज इसी काल मे बोए गए। मेरी समझ मे इन दोनों बातों में कोई विरोध नही है। एक कान में एक ही भाषा में दोनों प्रवृत्तियां रह सकती हैं, उनमे न तो परस्पर विशेष है पोरन प्राधारगत । कहां संस्कृत जैसी परिनिष्ठित काव्यभाषा और कहां प्रपश भाषा ? श्रीहर्ष की तुलना अपभ्रंश दोहाकारी से करने में कोई भौचित्य नहीं है ? अधिकतर हिन्दी विद्वानों को अपभ्रश साहित्य में पंठ है, अपभ्रंश दोहों तक सीमित है। जहां तक मलकृत शैली का सवाल है प्रपभ्रंश कवि पुष्पदंत भोर स्वयंभू श्रीहर्ष की टक्कर के कवि है। सरस्वती का स्मरण करते हुए पुष्पदंन ने कहा है
स. लंकारो छंदेण जंति, बहु सत्य प्रत्थ गारव वहति ।
मुह-वासिणी सद्दजोणी, णीसेस हेउ सा सोह-खोणी ॥
प्रालोच्यकाल के उत्तर काल में मध्यदेश पर चौहान मोर गाड़वार वंशों का प्राधिपत्य था। गाड़वार उतर-पश्चिम से प्राए थे । वैदिक धर्म के अनुयायी होने के कारण उन्होंने प्रपभ्रंश तथा देश्य भाषाओं को प्रश्रय नहीं दिया। दूसरे इस क्षेत्र में उस वजनशील ब्राह्मणव्यवस्था का बोलबाला रहा, जो संस्कृत को सब कुछ मानती थी । यह तो हुई उत्तरकाल की बात लेकिन पूर्वकाल में ( १० से १२वीं तक ) महीपाल के समय कन्नौज में सभी भाषाओं के कवियों को स्थान प्राप्त था। मध्यदेश के कवि को सर्वभाषा कवि बनना पड़ता था ! राजशेखर के अनुसार हक्क (पंजाब) से लेकर मादानक ( वर्तमान ग्वालियर) तक अपभ्रंश ही काव्य की भाषा थी । उस समय जब दक्षिण के राष्ट्रकूटों, बंगाल के पालों, सांभर के चौहानों, मालव के परमारो और गुजरात के सोलकियो के प्रश्रय ने पभ्रंश कविता लिखी जा रही थी। तब हिन्दी प्रदेश, जो भारत का हृदय देश है, उससे अछूता नहीं रहा होगा । उसकी घड़कनें संस्कृत के बलावा अपभ्रंश में भी मुखरित हुई होगी, लोक की भाषायें मौर भावनाएं मानसूनी हवाओं की तरह ऊपर-ऊपर नहीं उड़ती वे हृदय देश से उठ कर घासपात फैली होंगी, प्रौर प्रास-पास की भाषाम्रों और भावनाओ ने उसका स्पर्श किया होगा । भ्रतः जो नहीं है, उस पर लम्बा-चौड़ा अफ़सोस करने के बजाय, उचित यह था या है कि जो है उसकी गहराई से पड़ताल की जाए ? घटकलबाजी इसी से समाप्त होगी। तथ्य यह है कि प्रालीच्यकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, वहीं हैं जो दूसरे काल की हैं। यह युग वदतोव्याघात का युग नही है। वदतोव्याघात का अर्थ है - प्रपने कथन का खंडन स्वयं करना । मुझे पूरे युग के साहित्य में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उक्त कथन का समर्थन होता हो । यही बात प्रतविरोध के बारे में कही जा सकती है। डा० द्विवेदी ने दो चीजों में
मेरी वाणी प्रहंकारों से सजधज कर छंदों में चलती है, अनेक शास्त्रों के प्रयं गौरव को धारण करती है, ब्रह्मा के मुख में निवास करते हुए भी, शब्द जन्मा है। वह श्रेयस् और सौंदर्य की खान है ।" इस प्रकार पुष्पदंत की कविता उस समुद्र की तरह है जिसमें प्रारम सौंदर्य और भौतिक सौंदर्य की अनुभूतियों की जलराशि मरी हुई है, जिसमें एक ओर, वीर रस की उद्दाम गर्जनाएँ हैं, तो दूसरी भोर शृगार की कलगीतियां भी । जिसमें शांत और भक्ति रस की धाराम्रों का संगम है। जहाँ तक दिग्गज मचायो मोर निरक्षर संतों के सह प्रस्तिस्व का प्रश्न है, इसमें भी कोई विशेष नहीं । वास्तव में निरक्षर सन्तों ने इस काल में ज्ञान प्रचार के बीज अचानक नहीं बोए। सभी निरक्षर न तो अज्ञानी होते हैं, पीर न सभी साक्षर, ज्ञानी । प्राध्यात्मिक अनुभव पोर लोक की