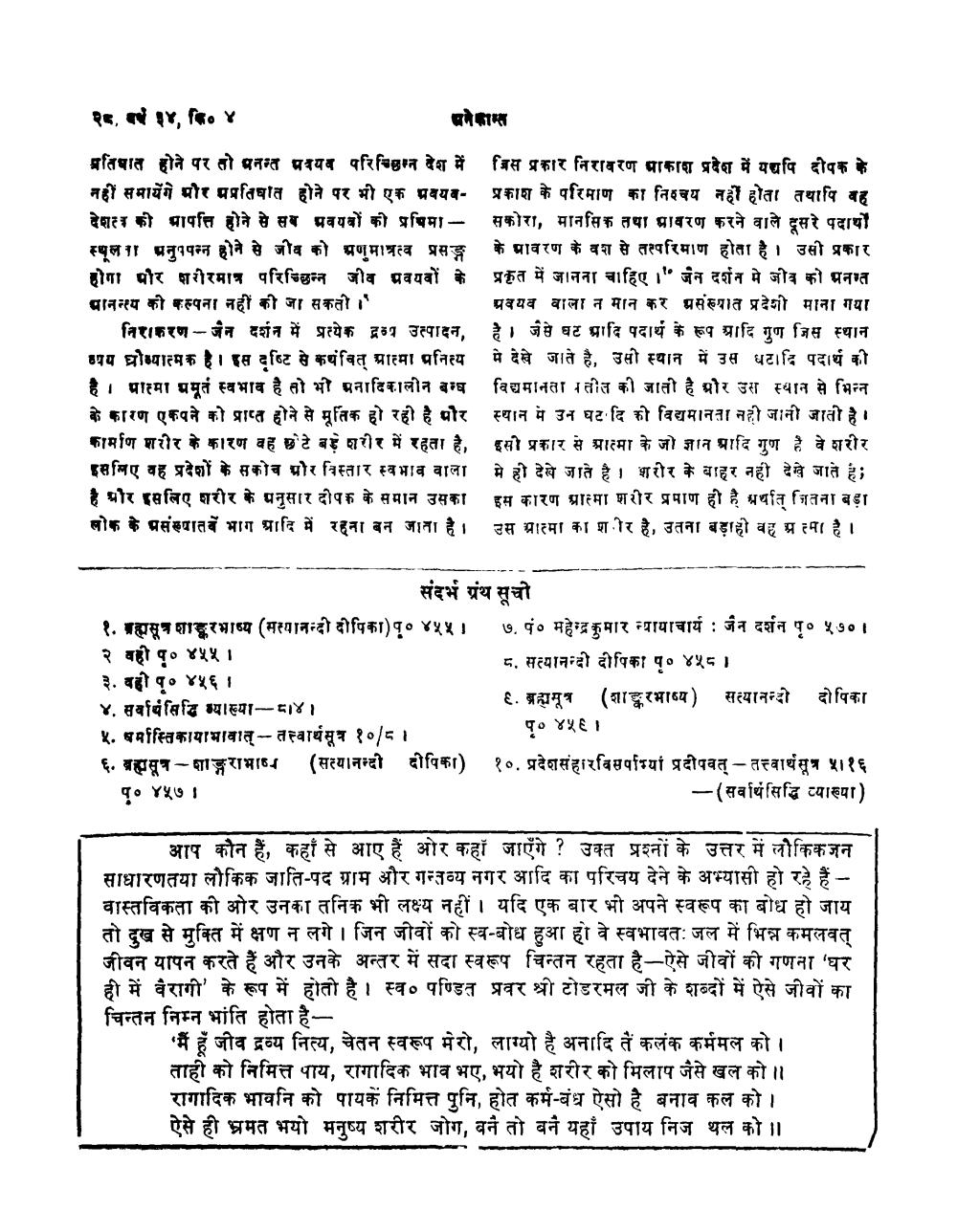________________
प्रतिपात होने पर तो अनन्त अवयव परिच्छिम्न देश में जिस प्रकार निरावरण पाकाश प्रदेश में यद्यपि दीपक के नहीं समायेंगे और प्रतिघात होने पर भी एक प्रबयब- प्रकाश के परिमाण का निश्चय नहीं होता तथापि वह देशतकी भापत्ति होने से सब प्रवयवों को प्रषिमा- सकोरा, मानसिक तथा प्रावरण करने वाले दूसरे पदार्थों स्थूल ना अनुपपन्न होने से जीव को अणुमात्रत्व प्रसङ्ग के प्रावरण के वश से तत्परिमाण होता है। उसी प्रकार होगा पौर शरीरमात्र परिच्छिन्न जीव अवयवों के प्रकृत में जानना चाहिए।" जैन दर्शन मे जीव को मनात माननस्य को कल्पना नहीं की जा सकती।'
प्रवयव वाला न मान कर प्रसंख्यात प्रदेशी माना गया निराकरण-जैन दर्शन में प्रत्येक द्रव्य उत्पादन, है। जैसे घट प्रादि पदार्थ के रूप प्रादि गुण जिस स्थान व्यय प्रौव्यात्मक है। इस दष्टि से कवित् प्रात्मा पनित्य मे देखे जाते है, उसी स्थान में उस घटादि पदार्थ की है। पास्मा ममूर्त स्वभाव है तो भी मनादिकालीन बन्ध विद्यमानता प्रतीत की जाती है और उस स्थान से भिन्न के कारण एकपने को प्राप्त होने से मूर्तिक हो रही है और स्थान में उन घट दि को विद्यमानता नही जानी जाती है। कार्माण शरीर के कारण वह छोटे बड़े शरीर में रहता है, इसी प्रकार से प्रात्मा के जो ज्ञान प्रादि गुण है वे शरीर इसलिए वह प्रदेशों के सकोच पोर विस्तार स्वभाव वाला मे ही देखे जाते है। शरीर के बाहर नही देखे जाते है। है और इसलिए शरीर के अनुसार दीपक के समान उसका इस कारण प्रात्मा शरीर प्रमाण ही है अर्थात् जितना बड़ा लोक के प्रसंस्पातवें भाग आदि में रहना बन जाता है। उस प्रात्मा का शीर है, उतना बड़ाही वह प्रत्मा है।
संदर्भ ग्रंथ सूची १. ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य (मस्यानन्दी दीपिका)पृ० ४५५। ७. पं० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य : जैन दर्शन पृ० ५७० । २ वही १०४५५।
८. सत्यानन्दी दीपिका १० ४५८ । ३. वही १० ४५६ । ४. सर्वार्थ सिदि व्याख्या-।४
६. ब्रह्मसूत्र (शाङ्करभाष्य) सत्यानन्दो दीपिका ५. धर्मास्तिकायाभावात् - तत्त्वार्थसूत्र १०/८ ।
पृ०४५६। ६. ब्रह्मसूत्र-शाङ्गराभाष्य (सत्यानन्दी दीपिका) १०. प्रदेशसंहारविसम्यां प्रदीपवत् - तत्त्वार्थसूत्र ५।१६ पु. ४५७ ।
-(सर्वार्थ सिद्धि व्याख्या)
आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं ओर कहाँ जाएँगे ? उक्त प्रश्नों के उत्तर में लौकिकजन साधारणतया लौकिक जाति-पद ग्राम और गन्तव्य नगर आदि का परिचय देने के अभ्यासी हो रहे हैं - वास्तविकता की ओर उनका तनिक भी लक्ष्य नहीं। यदि एक बार भी अपने स्वरूप का बोध हो जाय तो दुख से मुक्ति में क्षण न लगे। जिन जीवों को स्व-बोध हुआ हो वे स्वभावतः जल में भिन्न कमलवत् जीवन यापन करते हैं और उनके अन्तर में सदा स्वरूप चिन्तन रहता है-ऐसे जीवों की गणना घर ही में वैरागी' के रूप में होतो है। स्व० पण्डित प्रवर श्री टोडरमल जी के शब्दों में ऐसे जीवों का चिन्तन निम्न भांति होता है
'मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य, चेतन स्वरूप मेरो, लाग्यो है अनादि तै कलंक कर्ममल को। ताही को निमित्त पाय, रागादिक भाव भए, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को॥ रागादिक भावनि को पायके निमित्त पुनि, होत कर्म-बंध ऐसो है बनाव कल को। ऐसे ही भ्रमत भयो मनुष्य शरीर जोग, वन तो बनै यहाँ उपाय निज थल को॥