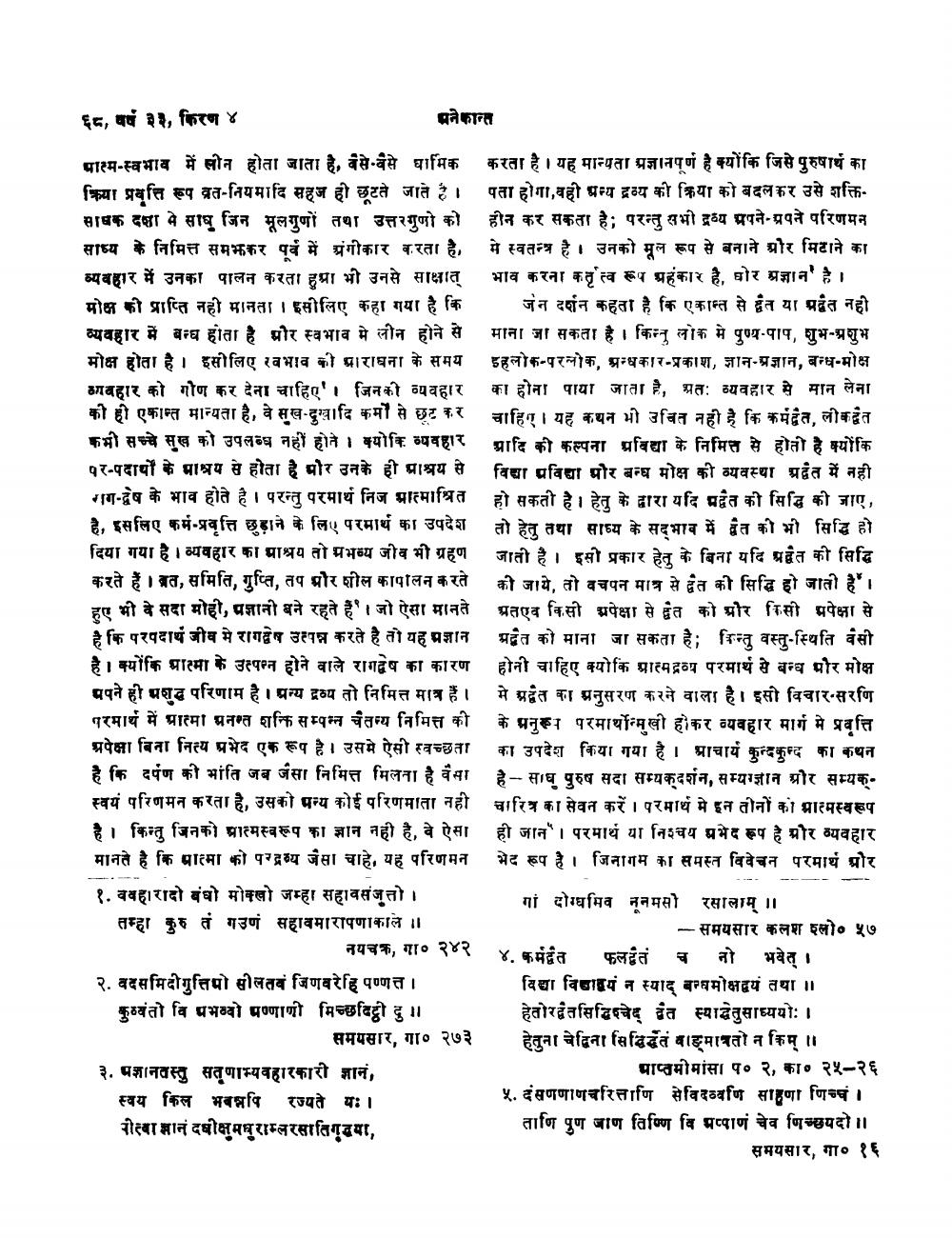________________
६८, वर्ष ३३, किरण ४
अनेकान्त
पास्म-स्वभाव में लीन होता जाता है, वैसे-वैसे घामिक करता है। यह मान्यता प्रज्ञानपूर्ण है क्योंकि जिसे पुरुषार्थ का क्रिया प्रवृत्ति रूप व्रत-नियमादि सहज ही छूटते जाते है। पता होगा,वही अन्य द्रव्य की क्रिया को बदलकर उसे शक्तिसापक दशा मे साप जिन मुलगणों तथा उत्तरगणो को हीन कर सकता है। परन्तु सभी द्रव्य अपने-अपने परिणमन साध्य के निमित्त समझकर पूर्व में अंगीकार करता है, मे स्वतन्त्र है । उनको मूल रूप से बनाने और मिटाने का व्यवहार में उनका पालन करता हुमा भी उनसे साक्षात् भाव करना कर्तृत्व रूप अहंकार है, घोर अज्ञान' है। मोक्ष की प्राप्ति नही मानता । इसीलिए कहा गया है कि जैन दर्शन कहता है कि एकान्त से द्वत या प्रत नही व्यवहार में बन्ध होता है और स्वभाव मे लीन होने से माना जा सकता है। किन्तु लोक मे पुण्य-पाप, शुभ-अशुभ मोक्ष होता है। इसीलिए स्वभाव की प्राराधना के समय इहलोक-परलोक, अन्धकार-प्रकाश, ज्ञान-प्रज्ञान, बन्ध-मोक्ष गवहार को गौण कर देना चाहिए। जिनकी व्यवहार का होना पाया जाता है, अत: व्यवहार से मान लेना की ही एकान्त मान्यता है, वे सुख-दुखादि कमो से छुट कर चाहिए। यह कथन भी उचित नही है कि कर्मद्वैत, लीकद्वैत कभी सच्चे सुख को उपलब्ध नहीं होते। क्योकि व्यवहार प्रादि की कल्पना प्रविद्या के निमित्त से होती है क्योंकि पर-पदार्थों के माश्रय से होता है और उनके ही पाश्रय से विद्या प्रविद्या और बन्ध मोक्ष की व्यवस्था अद्वैत में नही गग-द्वेष के भाव होते है। परन्तु परमार्थ निज प्रात्माश्रित हो सकती है। हेत के द्वारा यदि अद्वैत की सिद्धि की जाए, है, इसलिए कर्म-प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए परमार्थ का उपदेश तो हेतु तथा साध्य के सदभाव में वैत की भी सिद्धि हो दिया गया है। व्यवहार का माश्रय तो मभव्य जीव भी ग्रहण जाती है। इसी प्रकार हेतू के बिना यदि प्रत की सिद्धि करते हैं। व्रत, समिति, गुप्ति, तप और शील कापालन करते की जाये, तो वचपन मात्र से दंत की सिद्धि हो जाती है। हए भी वे सदा मोही, प्रज्ञानी बने रहते हैं। जो ऐसा मानते प्रतएव किसी अपेक्षा से दूत को और किसी अपेक्षा से है कि परपदार्थ जीव मे रागद्वेष उत्पन्न करते है तो यह प्रज्ञान अद्वैत को माना जा सकता है। किन्तु वस्तु-स्थिति वसी है। क्योंकि प्रात्मा के उत्पन्न होने वाले रागद्वेष का कारण होनी चाहिए क्योकि प्रात्मद्रव्य परमार्थ से बन्ध पौर मोक्ष अपने ही प्रशुद्ध परिणाम है। अन्य द्रव्य तो निमित्त मात्र हैं। मे अद्वत का अनुसरण करने वाला है। इसी विचार-सरणि परमार्थ में प्रात्मा अनन्त शक्ति सम्पन्न चैतन्य निमित्त की के अनुरूप परमार्थोन्मुखी होकर व्यवहार मार्ग मे प्रवृत्ति अपेक्षा बिना नित्य प्रभेद एक रूप है। उसमे ऐसी स्वच्छता का उपदेश किया गया है । प्राचार्य कुन्दकुन्द का कथन है कि दर्पण की भांति जब जैसा निमित्त मिलता है वैसा है- साध पुरुष सदा सम्यकदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्. स्वयं परिणमन करता है, उसको पन्य कोई परिणमाता नहीं चारित्र का सेवन करें। परमार्थ मे इन तीनों को प्रात्मस्वरूप है। किन्तु जिनको प्रात्मस्वरूप का ज्ञान नही है, वे ऐसा ही जान । परमार्थ या निश्चय प्रभेद रूप है और व्यवहार मानते है कि पात्मा को परद्रव्य जैसा चाहे, यह परिणमन भेद रूप है। जिनागम का समस्त विवेचन परमार्थ और १. ववहारादो बंधो मोक्खो जम्हा सहावसंजत्तो।
गां दोग्धमिव ननमसो रसालाम् ।। तम्हा कुरु तं गउणं सहावमारापणाकाले ॥
- समयसार कलश श्लो० ५७ __ नयचक्र, गा० २४२ ४. कर्मवंत फलद्वतं च नो भवेत् । २. बदसमिदीगुत्तिमो सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्त ।
विद्या विषादयं न स्याद् बन्धमोक्षद्वयं तथा ॥ कुम्वंतो वि प्रभव्यो अण्णाणी मिच्छदिट्टी दु॥
हेतोरवैतसिद्धिश्चेद् दंत स्याद्धेतुसाध्ययोः ।
समयसार, गा० २७३ हेतुना चेदिना सिविद्धतं वाङ्मावतो न किम् ॥ ३. पज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं,
माप्तमीमांसा प० २, का० २५-२६ स्वय किल भवन्नपि रज्यते यः।
५. दंसणणाणचरित्ताणि सेविदर्वाण साहणा णिच् । सीत्वासानं दधीक्षमधुराम्लरसातिगत्या,
ताणि पूण जाण तिण्णि वि प्रप्पाणं चेव णिच्छयदो।
समयसार, गा० १६