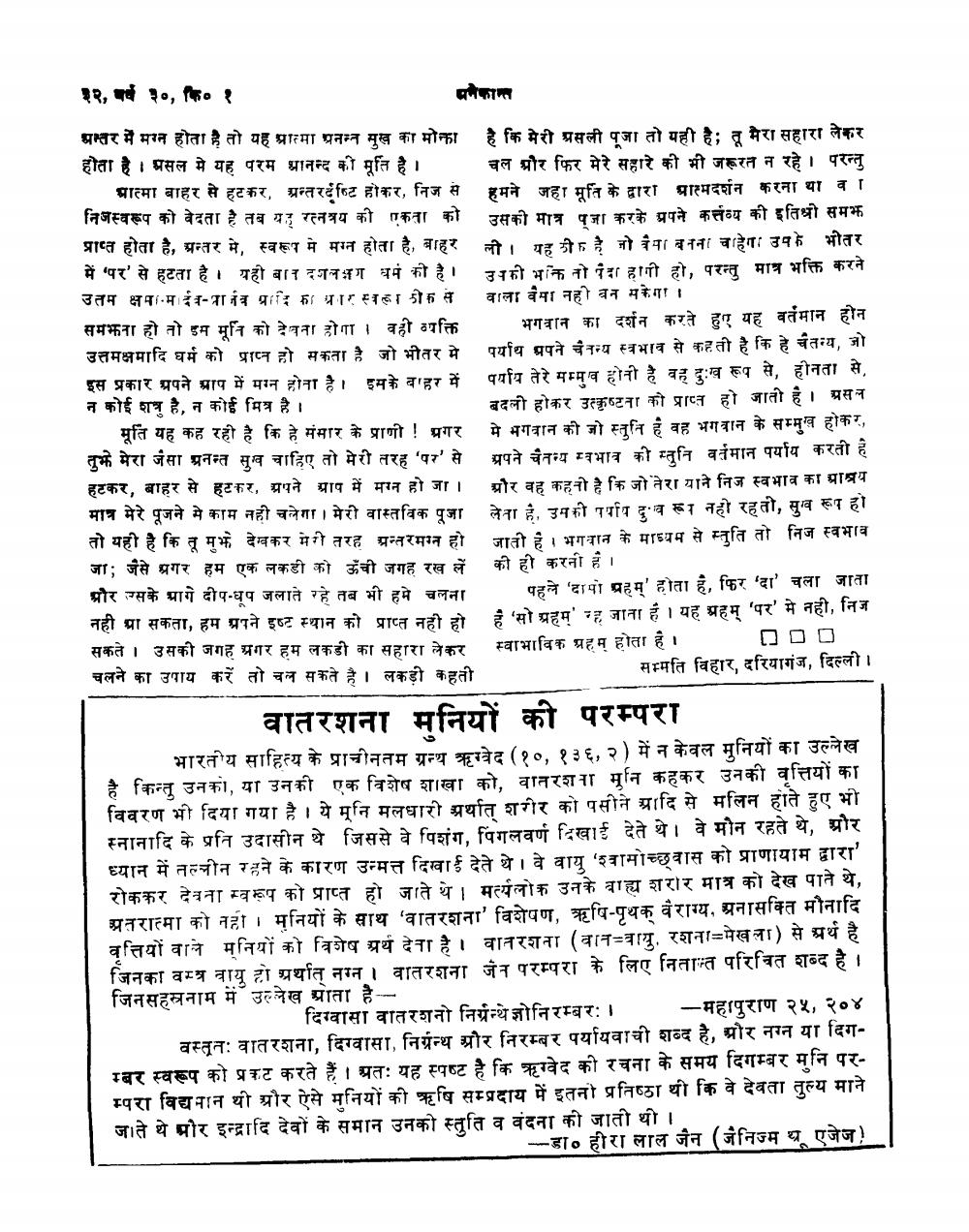________________
१२, पर्व ३०, कि० १
अन्तर में मग्न होता है तो यह प्रारमा प्रनम्न मुख का मोका है कि मेरी असली पूजा तो यही है; तू मेरा सहारा लेकर होता है। असल में यह परम प्रानन्द की मूर्ति है। चल और फिर मेरे सहारे की भी जरूरत न रहे। परन्तु
प्रात्मा बाहर से हटकर, अन्तरर्दष्टि होकर, निज से हमने जहा मूर्ति के द्वारा प्रात्मदर्शन करना था व । निजस्वरूप को वेदता है तब यह रत्नत्रय की एकता को उसकी मात्र जा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ प्राप्त होता है, अन्तर मे, स्वरूप में मग्न होता है, बाहर ली। यही है जो वैमा बनना चाहेगा उपके भीतर में 'पर' से हटता है। यही बात दशलक्षग धर्म की है। उसकी भकि नो पैदा होगी हो, परन्तु मात्र भक्ति करने उतम क्षमा म र्दव-पानव प्रादि का मारवाडी कसे वाला वैमा नहीं बन सकेगा। समझना हो तो इम मूनि को देखना होगा। वही व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए यह वर्तमान होन उत्तमक्षमादि धर्म को प्राप्त हो सकता है जो भीतर मे पर्याथ अपने चैतन्य स्वभाव से कहती है कि हे चैतन्य, जो इस प्रकार अपने प्राप में मग्न होता है। इसके बाहर में पर्याय तेरे मम्म व होनी है वह दुःख रूप से, हीनता से, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है।
बदली होकर उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है। असल मूर्ति यह कह रही है कि हे संसार के प्राणी! अगर मे भगवान की जो स्तुति है वह भगवान के सम्मुख होकर, तुझे मेरा जैसा अनन्त सूख चाहिए तो मेरी तरह 'पर' से अपने चैतन्य स्वभाव की स्तुनि वर्तमान पर्याय करता है हटकर, बाहर से हटकर, अपने आप में मग्न हो जा। और वह कहती है कि जो तेरा याने निज स्वभाव का पात्रय मात्र मेरे पूजने में काम नही चलेगा। मेरी वास्तविक पूजा लेता है, उसकी पर्याप दू व रूप नहीं रहता, सुख रूप है। तो यही है कि तु मझे देखकर मेरी तरह अन्तरमग्न हो जाती है। भगवान के माध्यम से स्तुति तो निज स्वभाव जा; जैसे अगर हम एक लकडी को ऊँची जगह रख लें की ही करनी है। और उसके आगे दीप-धूप जलाते रहे तब भी हमे चलना पहले 'दामो प्रहम्' होता है, फिर 'दा' चला जाता नही पा सकता, हम अपने इष्ट स्थान को प्राप्त नही हो है 'सो अहम्' नह जाता है । यह अहम् 'पर' मे नही, निज सकते। उसकी जगह अगर हम लकडी का सहारा लेकर स्वाभाविक अहम होता है।
. . . चलने का उपाय करें तो चल सकते है। लकड़ी कहती
सम्मति विहार, दरियागंज, दिल्ली।
वातरशना मनियों को परम्परा भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद (१०, १३६, २) में न केवल मुनियों का उल्लेख है किन्तु उनको, या उनकी एक विशेष शाखा को, वातरशता मुनि कहकर उनकी वृत्तियों का विवरण भी दिया गया है। ये मूनि मलधारी अर्थात शरीर को पसीने ग्रादि से मलिन होते हुए भी स्नानादि के प्रति उदासीन थे जिससे वे पिशंग, पिंगलवर्ण दिखाई देते थे। वे मौन रहते थे, और ध्यान में तल्लीन रहने के कारण उन्मत्त दिखाई देते थे। वे वाय 'श्वासोच्छवास को प्राणायाम द्वारा' रोककर देवता स्वरूप को प्राप्त हो जाते थे। मर्त्यलोक उनके बाह्य शरीर मात्र को देख पाते थे, अतरात्मा को नहीं । मनियों के साथ 'वातरशना' विशेषण, ऋषि-पृथक वैराग्य, अनासक्ति मौनादि वत्तियों वाले मनियों को विशेष अर्थ देता है। वातरशना (वात-वायु. रशनामेखला) से अर्थ है जिनका वस्त्र वायू हो अर्थात नग्न । वातरशना जैन परम्परा के लिए नितान्त परिचित शब्द है। जिनसहस्रनाम में उल्लेख प्रोता है
दिग्वासा वातरशनो निर्ग्रन्थे ज्ञोनिरम्बरः। -महापुराण २५, २०४ वस्तुतः वातरशना, दिग्वासा, निर्ग्रन्थ और निरम्बर पर्यायवाची शब्द है, और नग्न या दिगम्बर स्वरूप को प्रकट करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद की रचना के समय दिगम्बर मनि परम्परा विद्यमान थी और ऐसे मनियों की ऋषि सम्प्रदाय में इतनी प्रतिष्ठा थी कि वे देवता तुल्य माने जाते थे और इन्द्रादि देवों के समान उनको स्तुति व वंदना की जाती थी।
--डा. हीरा लाल जैन (जैनिज्म थ्र एजेज)